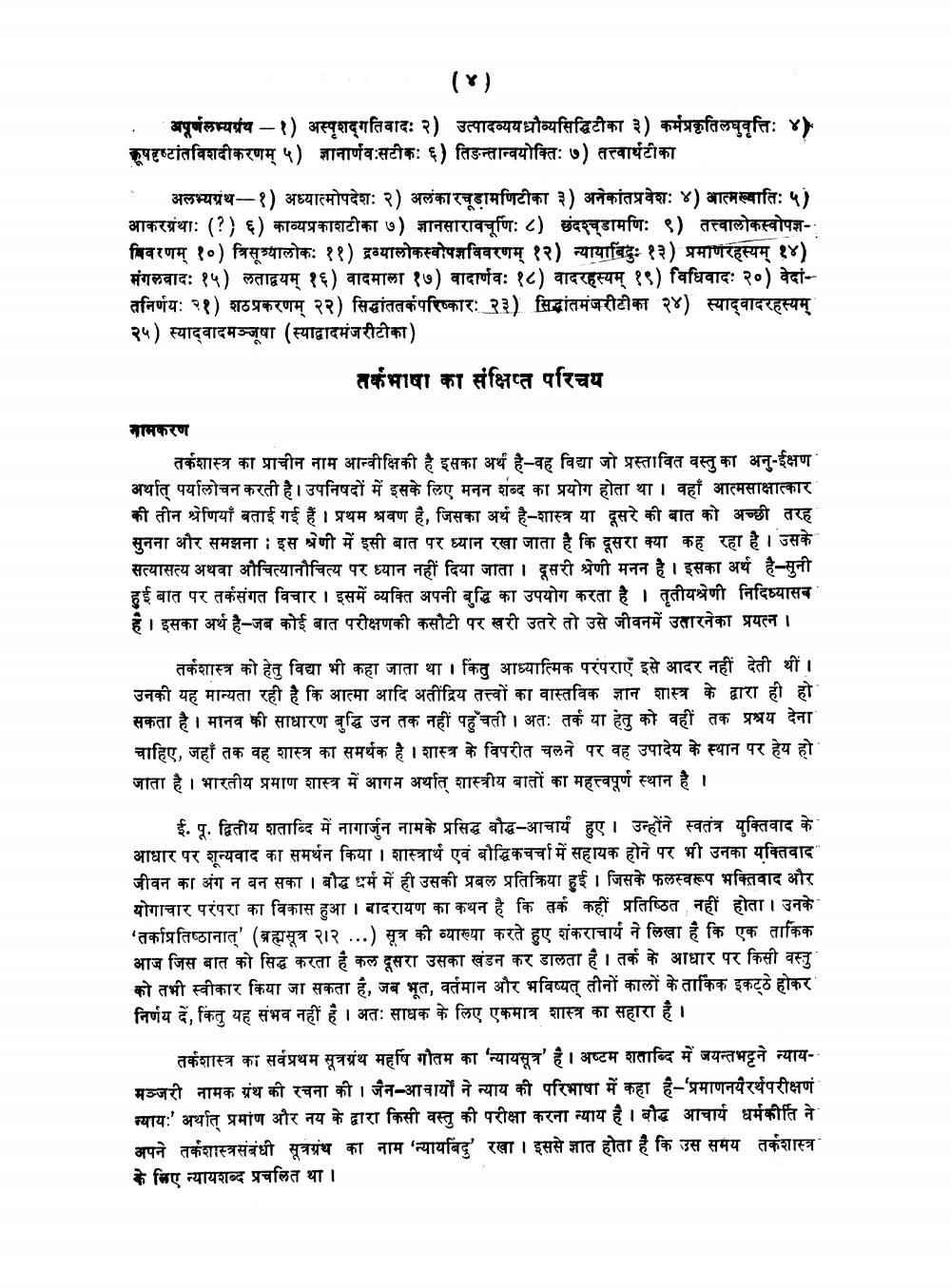Book Title: Jain Tark Bhasha Author(s): Shobhachandra Bharilla Publisher: Tiloakratna Sthanakvasi Jain Dharmik Pariksha Board View full book textPage 9
________________ ___ अपूर्णलभ्यग्रंथ -१) अस्पृशद्गतिवादः २) उत्पादव्ययध्रौव्यसिद्धिटीका ३) कर्मप्रकृतिलघुवृत्तिः ४) कूषदृष्टांतविशदीकरणम् ५) ज्ञानार्णवःसटीकः ६) तिङन्तान्वयोक्तिः ७) तत्त्वार्थटीका - अलभ्यग्रंथ-१) अध्यात्मोपदेशः २) अलंकारचूडामणिटीका ३) अनेकांतप्रवेशः ४) आत्मख्वाति: ५) आकरग्रंथाः (?) ६) काव्यप्रकाशटीका ७) ज्ञानसारावणिः ८) छंदश्च्डामणिः ९) तत्त्वालोकस्वोपज्ञविवरणम् १०) त्रिसूश्यालोकः ११) द्रव्यालोकस्वोपज्ञविवरणम् १२) न्यायाबिंदुः१३) प्रमाणरहस्यम् १४) मंगलवादः १५) लताद्वयम् १६) वादमाला १७) वादार्णवः १८) वादरहस्यम् १९) विधिवादः २०) वेदां-- तनिर्णयः २१) शठप्रकरणम् २२) सिद्धांततर्कपरिष्कारः २३) सिद्धांतमंजरीटीका २४) स्याद्वादरहस्यम् २५) स्याद्वादमञ्जूषा (स्याद्वादमंजरीटीका) तर्कभाषा का संक्षिप्त परिचय नामकरण तर्कशास्त्र का प्राचीन नाम आन्वीक्षिकी है इसका अर्थ है-वह विद्या जो प्रस्तावित वस्तु का अनु-ईक्षण अर्थात् पर्यालोचन करती है। उपनिषदों में इसके लिए मनन शब्द का प्रयोग होता था। वहाँ आत्मसाक्षात्कार की तीन श्रेणियाँ बताई गई हैं। प्रथम श्रवण है, जिसका अर्थ है-शास्त्र या दूसरे की बात को अच्छी तरह सुनना और समझना : इस श्रेणी में इसी बात पर ध्यान रखा जाता है कि दूसरा क्या कह रहा है । उसके सत्यासत्य अथवा औचित्यानौचित्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी श्रेणी मनन है । इसका अर्थ है-सुनी हुई बात पर तर्कसंगत विचार । इसमें व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है । तृतीयश्रेणी निदिध्यासन है। इसका अर्थ है-जब कोई बात परीक्षणकी कसौटी पर खरी उतरे तो उसे जीवनमें उतारनेका प्रयत्न । तर्कशास्त्र को हेतु विद्या भी कहा जाता था। किंतु आध्यात्मिक परंपराएँ इसे आदर नहीं देती थीं। उनकी यह मान्यता रही है कि आत्मा आदि अतींद्रिय तत्त्वों का वास्तविक ज्ञान शास्त्र के द्वारा ही हो सकता है। मानव की साधारण बुद्धि उन तक नहीं पहुँचती। अत: तर्क या हेतु को वहीं तक प्रश्रय देना चाहिए, जहाँ तक वह शास्त्र का समर्थक है । शास्त्र के विपरीत चलने पर वह उपादेय के स्थान पर हेय हो जाता है। भारतीय प्रमाण शास्त्र में आगम अर्थात शास्त्रीय बातों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । ई. पू. द्वितीय शताब्दि में नागार्जुन नामके प्रसिद्ध बौद्ध-आचार्य हुए। उन्होंने स्वतंत्र युक्तिवाद के आधार पर शून्यवाद का समर्थन किया। शास्त्रार्थ एवं बौद्धिकचर्चा में सहायक होने पर भी उनका यक्तिवाद जीवन का अंग न बन सका । बौद्ध धर्म में ही उसकी प्रबल प्रतिक्रिया हुई। जिसके फलस्वरूप भक्तिवाद और योगाचार परंपरा का विकास हुआ। बादरायण का कथन है कि तर्क कहीं प्रतिष्ठित नहीं होता। उनके 'तर्काप्रतिष्ठानात्' (ब्रह्मसूत्र २।२ ...) सूत्र की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने लिखा है कि एक तार्किक आज जिस बात को सिद्ध करता है कल दूसरा उसका खंडन कर डालता है। तर्क के आधार पर किसी वस्तु को तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब भूत, वर्तमान और भविष्यत् तीनों कालों के तार्किक इकट्ठे होकर निर्णय दें, किंतु यह संभव नहीं है । अतः साधक के लिए एकमात्र शास्त्र का सहारा है। तर्कशास्त्र का सर्वप्रथम सूत्रग्रंथ महर्षि गौतम का 'न्यायसूत्र' है । अष्टम शताब्दि में जयन्तभट्टने न्यायमञ्जरी नामक ग्रंथ की रचना की। जैन-आचार्यों ने न्याय की परिभाषा में कहा है-'प्रमाणनयरर्थपरीक्षणं न्यायः' अर्थात प्रमाण और नय के द्वारा किसी वस्तु की परीक्षा करना न्याय है। बौद्ध आचार्य धर्मकीर्ति ने अपने तर्कशास्त्रसंबंधी सूत्रग्रंथ का नाम 'न्यायबिंदु' रखा । इससे ज्ञात होता है कि उस समय तर्कशास्त्र के लिए न्यायशब्द प्रचलित था।Page Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 110