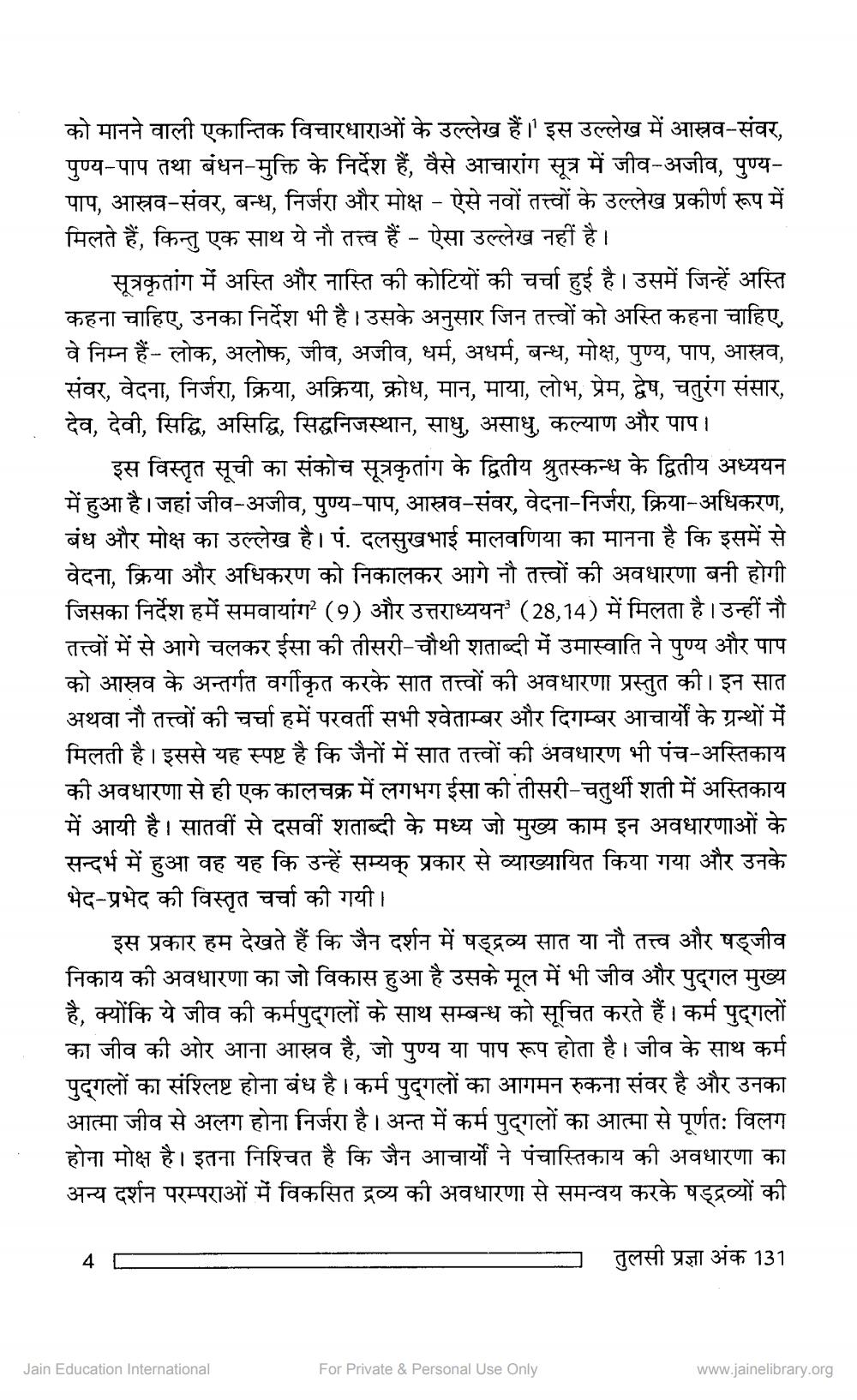Book Title: Tulsi Prajna 2006 04 Author(s): Shanta Jain, Jagatram Bhattacharya Publisher: Jain Vishva Bharati View full book textPage 9
________________ को मानने वाली एकान्तिक विचारधाराओं के उल्लेख हैं।' इस उल्लेख में आस्रव-संवर, पुण्य-पाप तथा बंधन-मुक्ति के निर्देश हैं, वैसे आचारांग सूत्र में जीव - अजीव, पुण्यपाप, आस्रव-संवर, बन्ध, निर्जरा और मोक्ष ऐसे नवों तत्त्वों के उल्लेख प्रकीर्ण रूप में मिलते हैं, किन्तु एक साथ ये नौ तत्त्व हैं - ऐसा उल्लेख नहीं है । सूत्रकृतांग में अस्ति और नास्ति की कोटियों की चर्चा हुई है । उसमें जिन्हें अस्ति कहना चाहिए, उनका निर्देश भी है। उसके अनुसार जिन तत्त्वों को अस्ति कहना चाहिए, वे निम्न हैं- लोक, अलोक, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, वेदना, निर्जरा, क्रिया, अक्रिया, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, चतुरंग संसार, देव, देवी, सिद्धि, असिद्धि, सिद्धनिजस्थान, साधु, असाधु, कल्याण और पाप । इस विस्तृत सूची का संकोच सूत्रकृतांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के द्वितीय अध्ययन हुआ है। जहां जीव- अजीव, पुण्य-पाप, आस्रव - संवर, वेदना - निर्जरा, क्रिया- अधिकरण, बंध और मोक्ष का उल्लेख है। पं. दलसुखभाई मालवणिया का मानना है कि इसमें से वेदना, क्रिया और अधिकरण को निकालकर आगे नौ तत्त्वों की अवधारणा बनी होगी जिसका निर्देश हमें समवायांग (9) और उत्तराध्ययन' (28,14) में मिलता है। उन्हीं नौ तत्त्वों में से आगे चलकर ईसा की तीसरी - चौथी शताब्दी में उमास्वाति ने पुण्य और पाप को आस्रव के अन्तर्गत वर्गीकृत करके सात तत्त्वों की अवधारणा प्रस्तुत की। इन सात अथवा नौ तत्त्वों की चर्चा हमें परवर्ती सभी श्वेताम्बर और दिगम्बर आचार्यों के ग्रन्थों में मिलती है। इससे यह स्पष्ट है कि जैनों में सात तत्त्वों की अवधारण भी पंच - अस्तिकाय की अवधारणा से ही एक कालचक्र में लगभग ईसा की तीसरी चतुर्थी शती में अस्तिकाय में आयी है। सातवीं से दसवीं शताब्दी के मध्य जो मुख्य काम इन अवधारणाओं के सन्दर्भ में हुआ वह यह कि उन्हें सम्यक् प्रकार से व्याख्यायित किया गया और उनके भेद-प्रभेद की विस्तृत चर्चा की गयी । 1 इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में षड्द्रव्य सात या नौ तत्त्व और षड्जीव निकाय की अवधारणा का जो विकास हुआ है उसके मूल में भी जीव और पुद्गल मुख्य है, क्योंकि ये जीव की कर्मपुद्गलों के साथ सम्बन्ध को सूचित करते हैं । कर्म पुद्गलों का जीव की ओर आना आस्रव है, जो पुण्य या पाप रूप होता है । जीव के साथ कर्म पुद्गलों का संश्लिष्ट होना बंध है । कर्म पुद्गलों का आगमन रुकना संवर है और उनका आत्मा जीव से अलग होना निर्जरा है । अन्त में कर्म पुद्गलों का आत्मा से पूर्णत: विलग होना मोक्ष है । इतना निश्चित है कि जैन आचार्यों ने पंचास्तिकाय की अवधारणा का अन्य दर्शन परम्पराओं में विकसित द्रव्य की अवधारणा से समन्वय करके षड्द्रव्यों की तुलसी प्रज्ञा अंक 131 4 Jain Education International - For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 122