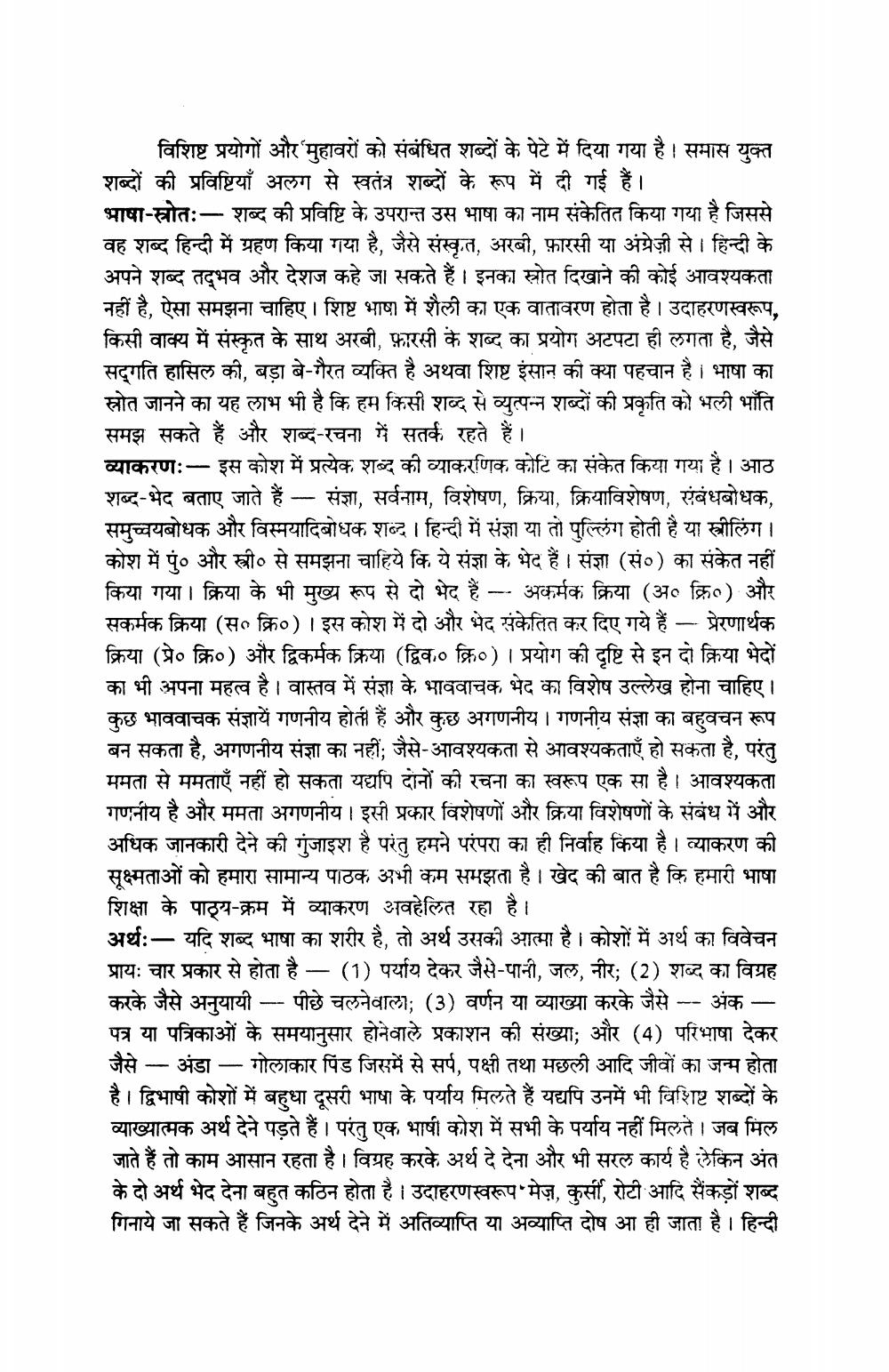Book Title: Shiksharthi Hindi Shabdakosh Author(s): Hardev Bahri Publisher: Rajpal and Sons View full book textPage 9
________________ विशिष्ट प्रयोगों और मुहावरों को संबंधित शब्दों के पेटे में दिया गया है। समास युक्त शब्दों की प्रविष्टियाँ अलग से स्वतंत्र शब्दों के रूप में दी गई हैं। भाषा-स्रोतः- शब्द की प्रविष्टि के उपरान्त उस भाषा का नाम संकेतित किया गया है जिससे वह शब्द हिन्दी में ग्रहण किया गया है, जैसे संस्कृत, अरबी, फ़ारसी या अंग्रेज़ी से। हिन्दी के अपने शब्द तद्भव और देशज कहे जा सकते हैं। इनका स्रोत दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। शिष्ट भाषा में शैली का एक वातावरण होता है। उदाहरणस्वरूप, किसी वाक्य में संस्कृत के साथ अरबी, फारसी के शब्द का प्रयोग अटपटा ही लगता है, जैसे सद्गति हासिल की, बड़ा बे-गैरत व्यक्ति है अथवा शिष्ट इंसान की क्या पहचान है। भाषा का स्रोत जानने का यह लाभ भी है कि हम किसी शब्द से व्युत्पन्न शब्दों की प्रकृति को भली भाँति समझ सकते हैं और शब्द-रचना में सतर्क रहते हैं। व्याकरणः- इस कोश में प्रत्येक शब्द की व्याकरणिक कोटि का संकेत किया गया है । आठ शब्द-भेद बताए जाते हैं - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक शब्द । हिन्दी में संज्ञा या तो पुल्लिंग होती है या स्त्रीलिंग। कोश में पुं० और स्त्री० से समझना चाहिये कि ये संज्ञा के भेद हैं । संज्ञा (सं०) का संकेत नहीं किया गया। क्रिया के भी मुख्य रूप से दो भेद हैं --- अकर्मक क्रिया (अ० क्रि०) और सकर्मक क्रिया (स० क्रि०) । इस कोश में दो और भेद संकेतित कर दिए गये हैं - प्रेरणार्थक क्रिया (प्रे० क्रि०) और द्विकर्मक क्रिया (द्विक० क्रि०) । प्रयोग की दृष्टि से इन दो क्रिया भेदों का भी अपना महत्व है। वास्तव में संज्ञा के भाववाचक भेद का विशेष उल्लेख होना चाहिए। कछ भाववाचक संज्ञायें गणनीय होती हैं और कछ अगणनीय। गणनीय संज्ञा का बहवचन रूप बन सकता है, अगणनीय संज्ञा का नहीं; जैसे-आवश्यकता से आवश्यकताएँ हो सकता है, परंतु ममता से ममताएँ नहीं हो सकता यद्यपि दोनों की रचना का स्वरूप एक सा है। आवश्यकता गणनीय है और ममता अगणनीय । इसी प्रकार विशेषणों और क्रिया विशेषणों के संबंध में और अधिक जानकारी देने की गुंजाइश है परंतु हमने परंपरा का ही निर्वाह किया है। व्याकरण की सूक्ष्मताओं को हमारा सामान्य पाठक अभी कम समझता है। खेद की बात है कि हमारी भाषा शिक्षा के पाठ्य-क्रम में व्याकरण अवहेलित रहा है। अर्थः- यदि शब्द भाषा का शरीर है, तो अर्थ उसकी आत्मा है। कोशों में अर्थ का विवेचन प्रायः चार प्रकार से होता है - (1) पर्याय देकर जैसे-पानी, जल, नीर; (2) शब्द का विग्रह करके जैसे अनुयायी -- पीछे चलनेवाला; (3) वर्णन या व्याख्या करके जैसे --- अंक - पत्र या पत्रिकाओं के समयानुसार होनेवाले प्रकाशन की संख्या; और (4) परिभाषा देकर जैसे - अंडा - गोलाकार पिंड जिसमें से सर्प, पक्षी तथा मछली आदि जीवों का जन्म होता है। द्विभाषी कोशों में बहुधा दूसरी भाषा के पर्याय मिलते हैं यद्यपि उनमें भी विशिष्ट शब्दों के व्याख्यात्मक अर्थ देने पड़ते हैं। परंतु एक भाषी कोश में सभी के पर्याय नहीं मिलते। जब मिल जाते हैं तो काम आसान रहता है। विग्रह करके अर्थ दे देना और भी सरल कार्य है लेकिन अंत के दो अर्थ भेद देना बहुत कठिन होता है। उदाहरणस्वरूप मेज़, कुर्सी, रोटी आदि सैंकड़ों शब्द गिनाये जा सकते हैं जिनके अर्थ देने में अतिव्याप्ति या अव्याप्ति दोष आ ही जाता है। हिन्दीPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 954