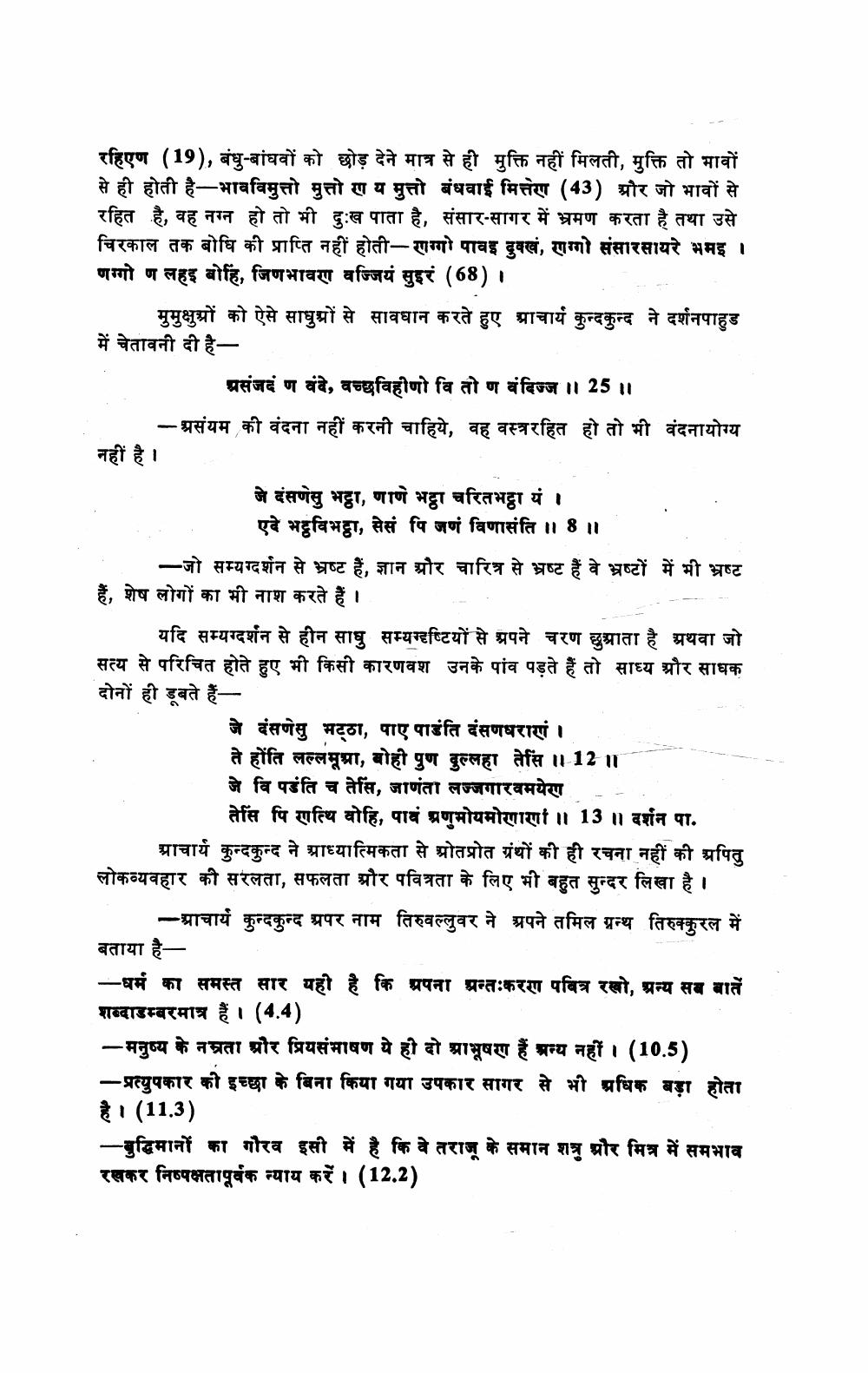Book Title: Jain Vidya 10 11 Author(s): Pravinchandra Jain & Others Publisher: Jain Vidya Samsthan View full book textPage 9
________________ रहिएण (19), बंधु-बांधवों को छोड़ देने मात्र से ही मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो भावों से ही होती है-भावविमुत्तो मुत्तो ण य मुत्तो बंधवाई मित्तरण (43) और जो भावों से रहित है, वह नग्न हो तो भी दुःख पाता है, संसार-सागर में भ्रमण करता है तथा उसे चिरकाल तक बोधि की प्राप्ति नहीं होती-णग्गो पावइ दुवखं, रणग्गो संसारसायरे भमइ । णग्गो ग लहइ बोहि, जिणभावरण वज्जियं सुइरं (68)। मुमुक्षुत्रों को ऐसे साधुनों से सावधान करते हुए प्राचार्य कुन्दकुन्द ने दर्शनपाहुड में चेतावनी दी है प्रसंजदं ण वंदे, वच्छविहीणो वि तो ण बंदिज्ज ॥25॥ - असंयम की वंदना नहीं करनी चाहिये, वह वस्त्ररहित हो तो भी वंदनायोग्य नहीं है। जे दंसणेसु भट्टा, णाणे भट्टा चरितभट्ठा यं । एवे भट्ठविभट्ठा, सेसं पि जणं विणासंति ॥8॥ -जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट हैं, ज्ञान और चारित्र से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्टों में भी भ्रष्ट हैं, शेष लोगों का भी नाश करते हैं । यदि सम्यग्दर्शन से हीन साधु सम्यग्दृष्टियों से अपने चरण छुप्राता है अथवा जो सत्य से परिचित होते हुए भी किसी कारणवश उनके पांव पड़ते हैं तो साध्य और साधक दोनों ही डूबते हैं जे दंसणेसु भट्ठा, पाए पाउंति दसणघराणं। . ते होंति लल्लमूना, बोही पुण दुल्लहा तेसि ॥ 12 ॥ जे वि पडंति च तेसि, जाणंता लज्जगारवमयेण . . . तेसि पि रणत्थि वोहि, पावं अणुभोयमोणाण ॥ 13 ॥ दर्शन पा. प्राचार्य कुन्दकुन्द ने आध्यात्मिकता से ओतप्रोत ग्रंथों की ही रचना नहीं की अपितु लोकव्यवहार की सरलता, सफलता और पवित्रता के लिए भी बहुत सुन्दर लिखा है । -आचार्य कुन्दकुन्द अपर नाम तिरुवल्लुवर ने अपने तमिल ग्रन्थ तिरुक्कुरल में बताया है-धर्म का समस्त सार यही है कि अपना अन्तःकरण पवित्र रखो, अन्य सब बातें शब्दाडम्बरमात्र हैं। (4.4) -मनुष्य के नम्रता और प्रियसंभाषण ये ही दो प्राभूषण हैं अन्य नहीं । (10.5) -प्रत्युपकार की इच्छा के बिना किया गया उपकार सागर से भी अधिक बड़ा होता है। (11.3) -बुद्धिमानों का गौरव इसी में है कि वे तराजू के समान शत्रु और मित्र में समभाव रखकर निष्पक्षतापूर्वक न्याय करें। (12.2)Page Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 180