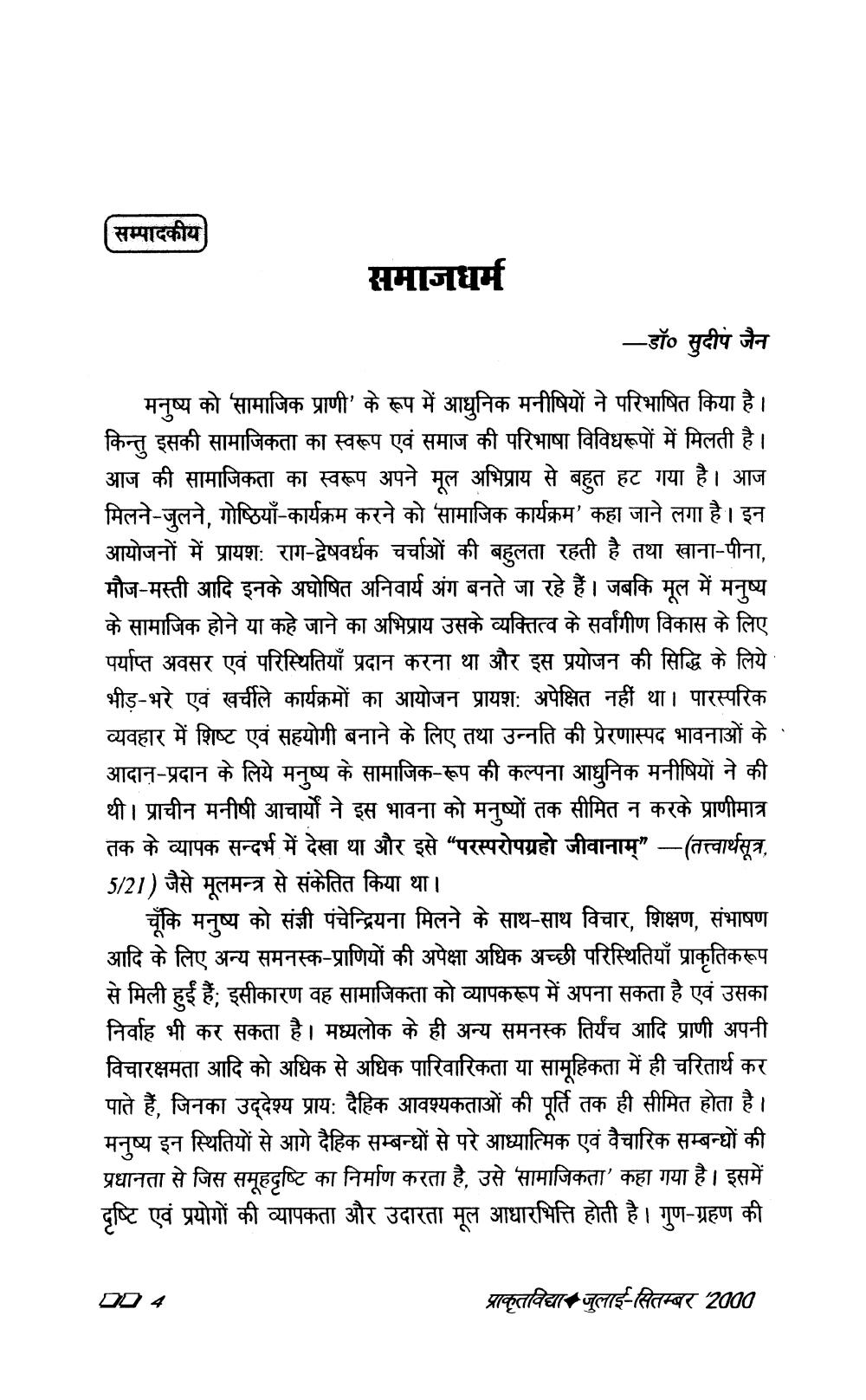Book Title: Prakrit Vidya 2000 07 Author(s): Rajaram Jain, Sudip Jain Publisher: Kundkund Bharti Trust View full book textPage 6
________________ [सम्पादकीय समाजधर्म -डॉ० सुदीप जैन मनुष्य को 'सामाजिक प्राणी' के रूप में आधुनिक मनीषियों ने परिभाषित किया है। किन्तु इसकी सामाजिकता का स्वरूप एवं समाज की परिभाषा विविधरूपों में मिलती है। आज की सामाजिकता का स्वरूप अपने मूल अभिप्राय से बहुत हट गया है। आज मिलने-जुलने, गोष्ठियाँ कार्यक्रम करने को सामाजिक कार्यक्रम' कहा जाने लगा है। इन आयोजनों में प्रायश: राग-द्वेषवर्धक चर्चाओं की बहुलता रहती है तथा खाना-पीना, मौज-मस्ती आदि इनके अघोषित अनिवार्य अंग बनते जा रहे हैं। जबकि मूल में मनुष्य के सामाजिक होने या कहे जाने का अभिप्राय उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर एवं परिस्थितियाँ प्रदान करना था और इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये भीड़-भरे एवं खर्चीले कार्यक्रमों का आयोजन प्रायश: अपेक्षित नहीं था। पारस्परिक व्यवहार में शिष्ट एवं सहयोगी बनाने के लिए तथा उन्नति की प्रेरणास्पद भावनाओं के आदान-प्रदान के लिये मनुष्य के सामाजिक-रूप की कल्पना आधुनिक मनीषियों ने की थी। प्राचीन मनीषी आचार्यों ने इस भावना को मनुष्यों तक सीमित न करके प्राणीमात्र तक के व्यापक सन्दर्भ में देखा था और इसे “परस्परोपग्रहो जीवानाम्” – (तत्त्वार्थसूत्र, 5/21) जैसे मूलमन्त्र से संकेतित किया था। ___ चूँकि मनुष्य को संज्ञी पंचेन्द्रियना मिलने के साथ-साथ विचार, शिक्षण, संभाषण आदि के लिए अन्य समनस्क-प्राणियों की अपेक्षा अधिक अच्छी परिस्थितियाँ प्राकृतिकरूप से मिली हुई हैं; इसीकारण वह सामाजिकता को व्यापकरूप में अपना सकता है एवं उसका निर्वाह भी कर सकता है। मध्यलोक के ही अन्य समनस्क तिर्यंच आदि प्राणी अपनी विचारक्षमता आदि को अधिक से अधिक पारिवारिकता या सामूहिकता में ही चरितार्थ कर पाते हैं, जिनका उद्देश्य प्राय: दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित होता है। मनुष्य इन स्थितियों से आगे दैहिक सम्बन्धों से परे आध्यात्मिक एवं वैचारिक सम्बन्धों की प्रधानता से जिस समूहदृष्टि का निर्माण करता है, उसे 'सामाजिकता' कहा गया है। इसमें दृष्टि एवं प्रयोगों की व्यापकता और उदारता मूल आधारभित्ति होती है। गुण-ग्रहण की DD4 प्राकृतविद्या जुलाई-सितम्बर 2000Page Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 116