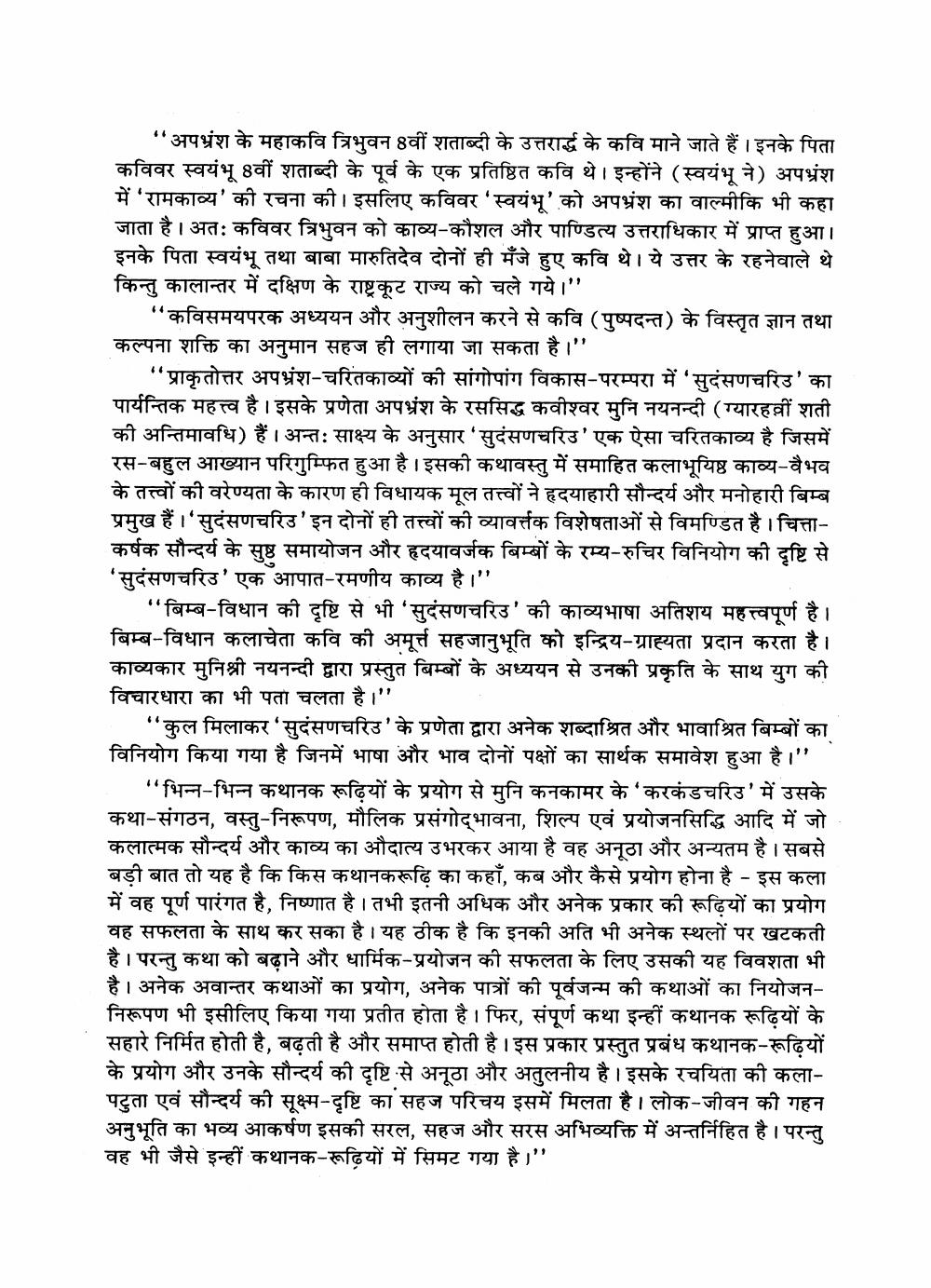Book Title: Apbhramsa Bharti 1997 09 10 Author(s): Kamalchand Sogani, Gyanchandra Khinduka, Gopichand Patni Publisher: Apbhramsa Sahitya Academy View full book textPage 9
________________ 'अपभ्रंश के महाकवि त्रिभुवन 8वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के कवि माने जाते हैं। इनके पिता कविवर स्वयंभू 8वीं शताब्दी के पूर्व के एक प्रतिष्ठित कवि थे । इन्होंने (स्वयंभू ने) अपभ्रंश में 'रामकाव्य' की रचना की। इसलिए कविवर 'स्वयंभू' को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है । अत: कविवर त्रिभुवन को काव्य- कौशल और पाण्डित्य उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ । इनके पिता स्वयंभू तथा बाबा मारुतिदेव दोनों ही मँजे हुए कवि थे। ये उत्तर के रहनेवाले थे किन्तु कालान्तर में दक्षिण के राष्ट्रकूट राज्य को चले गये।" 44 “कविसमयपरक अध्ययन और अनुशीलन करने से कवि (पुष्पदन्त) के विस्तृत ज्ञान तथा कल्पना शक्ति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।" "प्राकृतोत्तर अपभ्रंश चरितकाव्यों की सांगोपांग विकास - परम्परा में 'सुदंसणचरिउ' का पार्यन्ति महत्त्व है। इसके प्रणेता अपभ्रंश के रससिद्ध कवीश्वर मुनि नयनन्दी (ग्यारहवीं शती की अन्तिमावधि ) हैं । अन्तः साक्ष्य के अनुसार 'सुदंसणचरिउ' एक ऐसा चरितकाव्य है जिसमें रस-बहुल आख्यान परिगुम्फित हुआ है। इसकी कथावस्तु में समाहित कलाभूयिष्ठ काव्य-वैभव के तत्त्वों की वरेण्यता के कारण ही विधायक मूल तत्त्वों ने हृदयाहारी सौन्दर्य और मनोहारी बिम्ब प्रमुख हैं। 'सुदंसणचरिउ ' इन दोनों ही तत्त्वों की व्यावर्त्तक विशेषताओं से विमण्डित है। चित्ताकर्षक सौन्दर्य के सुष्ठु समायोजन और हृदयावर्जक बिम्बों के रम्य रुचिर विनियोग की दृष्टि से 'सुदंसणचरिउ' एक आपात रमणीय काव्य है ।" " बिम्ब-विधान की दृष्टि से भी 'सुदंसणचरिउ' की काव्यभाषा अतिशय महत्त्वपूर्ण है। बिम्ब-विधान कलाचेता कवि की अमूर्त सहजानुभूति को इन्द्रिय-ग्राह्यता प्रदान करता है । काव्यकार मुनिश्री नयनन्दी द्वारा प्रस्तुत बिम्बों के अध्ययन से उनकी प्रकृति के साथ युग की विचारधारा का भी पता चलता है।" "कुल मिलाकर 'सुदंसणचरिउ' के प्रणेता द्वारा अनेक शब्दाश्रित और भावाश्रित बिम्बों का विनियोग किया गया है जिनमें भाषा और भाव दोनों पक्षों का सार्थक समावेश हुआ है । " " भिन्न-भिन्न कथानक रूढ़ियों के प्रयोग से मुनि कनकामर के 'करकंडचरिउ' में उसके कथा-संगठन, वस्तु-निरूपण, मौलिक प्रसंगोद्भावना, शिल्प एवं प्रयोजनसिद्धि आदि में जो कलात्मक सौन्दर्य और काव्य का औदात्य उभरकर आया है वह अनूठा और अन्यतम है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किस कथानकरूढ़ि का कहाँ, कब और कैसे प्रयोग होना है - इस कला में वह पूर्ण पारंगत है, निष्णात है। तभी इतनी अधिक और अनेक प्रकार की रूढ़ियों का प्रयोग वह सफलता के साथ कर सका है। यह ठीक है कि इनकी अति भी अनेक स्थलों पर खटकती है । परन्तु कथा को बढ़ाने और धार्मिक प्रयोजन की सफलता के लिए उसकी यह विवशता भी है । अनेक अवान्तर कथाओं का प्रयोग, अनेक पात्रों की पूर्वजन्म की कथाओं का नियोजननिरूपण भी इसीलिए किया गया प्रतीत होता है। फिर, संपूर्ण कथा इन्हीं कथानक रूढ़ियों के सहारे निर्मित होती है, बढ़ती है और समाप्त होती है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रबंध कथानक - रूढ़ियों के प्रयोग और उनके सौन्दर्य की दृष्टि से अनूठा और अतुलनीय है। इसके रचयिता की कलापटुता एवं सौन्दर्य की सूक्ष्म दृष्टि का सहज परिचय इसमें मिलता है। लोक-जीवन की गहन अनुभूति का भव्य आकर्षण इसकी सरल, सहज और सरस अभिव्यक्ति में अन्तर्निहित है । परन्तु वह भी जैसे इन्हीं कथानक रूढ़ियों में सिमट गया है।"Page Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 142