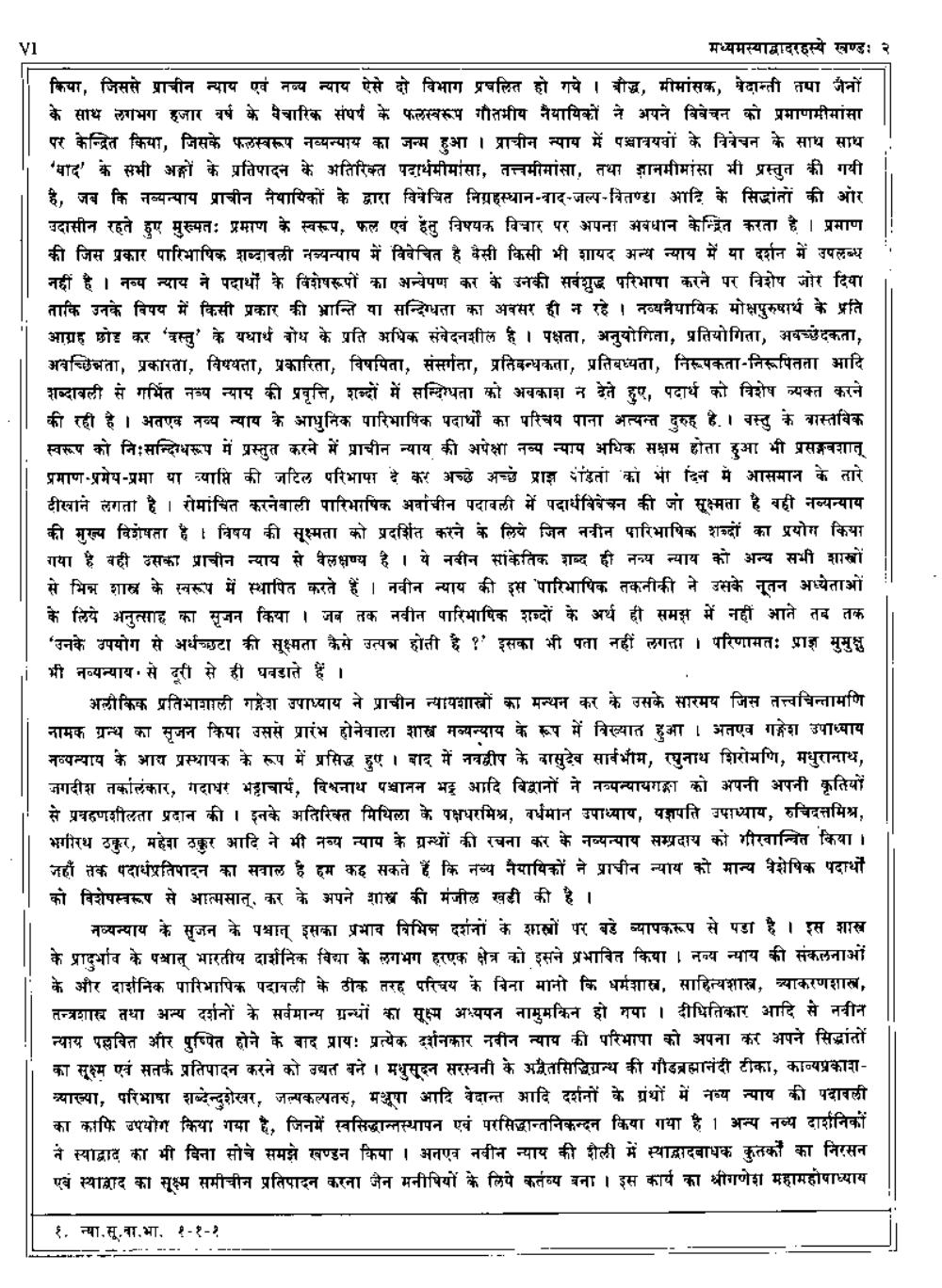Book Title: Syadvadarahasya Part 2 Author(s): Yashovijay Upadhyay, Publisher: Divya Darshan Trust View full book textPage 6
________________ vi मध्यमस्याद्वादरहस्ये खण्डः २ किया, जिससे प्राचीन न्याय एवं नव्य न्याय ऐसे दो विभाग प्रचलित हो गये । बौद्ध, मीमांसक, वेदान्ती तपा जैनों के साथ लगभग हजार वर्ष के वैचारिक संघर्ष के फलस्वरूप गौतमीय नैयायिकों ने अपने विवेचन को प्रमाणमीमांसा पर केन्द्रित किया, जिसके फलस्वरूप नव्यन्याय का जन्म हुआ। प्राचीन न्याय में पश्चावयवों के विवेचन के साथ साथ 'बाद' के सभी अङ्गों के प्रतिपादन के अतिरिक्त पदार्थमीमांसा, तत्वमीमांसा, तथा शानमीमांसा भी प्रस्तुत की गयी है, जब कि नव्यन्याय प्राचीन नैयायिकों के द्वारा विवेचित निग्रहस्थान-बाद-जल्प-वितण्डा आदि के सिद्धांतों की ओर उदासीन रहते हुए मुरूपतः प्रमाण के स्वरूप, फल एवं हेतु विषयक विचार पर अपना अवधान केन्द्रित करता है । प्रमाण की जिस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली नव्यन्याप में विवेचित है वैसी किसी भी शायद अन्य न्याय में या दर्शन में उपलब्ध नहीं है । नव्य न्याय ने पदार्थों के विशेषरूपों का अन्वेपण कर के उनकी सर्वशृद्ध परिभाषा करने पर विशेष जोर दिया ताकि उनके विषय में किसी प्रकार की भ्रान्ति या सन्दिग्धता का अवसर ही न रहे । नव्यनैयायिक मोक्षपुरुषार्थ के प्रति आग्रह छोड़ कर 'वस्तु' के यथार्थ बोध के प्रति अधिक संवेदनशील है । पक्षता, अनुयोगिता, प्रतियोगिता, अवच्छेदकता, अवच्छिनता, प्रकारता, विषयता, प्रकारिता, विषपिता, संसर्गता, प्रतिबन्धकता, प्रतिबध्यता, निरूपकता-निरूपितता आदि शब्दावली से गर्मित नव्य न्याय की प्रवृत्ति, शब्दों में सन्दिग्धता को अवकाश न देते हुए, पदार्थ को विशेष व्यक्त करने की रही है। अतएव नव्य न्याय के आधुनिक पारिभाषिक पदार्थों का परिचय पाना अत्यन्त दुरुह है.। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को निःसन्दिग्धरूप में प्रस्तुत करने में प्राचीन न्याय की अपेक्षा नव्य न्याप अधिक सक्षम होता हुआ भी प्रसङ्गवशात् प्रमाण-प्रमेय-प्रमा या न्याप्ति की जटिल परिभाषा दे कर अच्छे अच्छे प्राज्ञ पांडता को भा दिन में आसमान के तारे दीखाने लगता है । रोमांचित करनेवाली पारिभाषिक अर्वाचीन पदावली में पदार्थविवेचन की जो सूक्ष्मता है वही नव्यन्याय की मुख्य विशेषता है । विषय की सूक्ष्मता को प्रदर्शित करने के लिये जिन नवीन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है वही उसका प्राचीन न्याय से वैलक्षण्य है । ये नवीन सांकेतिक शब्द ही नन्य न्याय को अन्य सभी शास्त्रों से भिन्न शास्त्र के स्वरूप में स्थापित करते हैं। नवीन न्याय की इस पारिभाषिक तकनीकी ने उसके नूतन अध्येताओं के लिये अनुत्साह का सृजन किया । जब तक नवीन पारिभाषिक शब्दों के अर्थ ही समझ में नहीं आते तब तक 'उनके उपयोग से अर्धच्छटा की सूक्ष्मता कैसे उत्पन्न होती है? इसका भी पता नहीं लगता । परिणामतः प्राज्ञ मुमुक्षु भी नव्यन्याय · से दूरी से ही घबड़ाते हैं। अलौकिक प्रतिभाशाली गनेश उपाध्याय ने प्राचीन न्यायशास्त्रों का मन्थन कर के उसके सारमय जिस तत्त्वचिन्तामणि नामक ग्रन्थ का सृजन किया उससे प्रारंभ होनेवाला शास्त्र मन्यन्याय के रूप में विख्यात हुआ । अतएव गङ्गेश उपाध्याय नव्यन्याय के आच प्रस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाद में नवद्वीप के वासुदेव सार्वभौम, रघुनाथ शिरोमणि, मधुरानाथ, जगदीश तालंकार, गदाधर भट्टाचार्य, विक्षनाथ पश्चानन भट्ट आदि विद्वानों ने नव्यन्यायगङ्गा को अपनी अपनी कृतियों से प्रवहणशीलता प्रदान की। इनके अतिरिक्त मिथिला के पक्षधरमिश्र, वर्धमान उपाध्याय, यज्ञपति उपाध्याय, रुचिदसमिश्र, भगीरथ ठकुर, महेवा ठक्कर आदि ने भी नव्य न्याय के ग्रन्थों की रचना कर के नव्यन्याय सम्प्रदाय को गीरवान्वित किया। जहाँ तक पदाधप्रतिपादन का सवाल है हम कह सकते हैं कि नव्य नैयायिकों ने प्राचीन न्याय को मान्य वैशेषिक पदार्थों को विशेपस्नरूप से आत्मसात् कर के अपने शास्त्र की मंजील खटी की है। नव्यन्याय के सृजन के पश्चात् इसका प्रभाव विभिम दर्शनों के शास्त्रों पर बड़े व्यापकरूप से पड़ा है । इस शास्त्र के प्रादुर्भाव के पश्चात् भारतीय दार्शनिक विद्या के लगभग हरएक क्षेत्र को इसने प्रभावित किया । नन्य न्याय की संकलनाओं के और दार्शनिक पारिभापिक पदावली के ठीक तरह परिचय के बिना मानो कि धर्मशास्त्र, साहित्यशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, तन्त्रशास्त्र तथा अन्य दर्शनों के सर्वमान्य ग्रन्थों का सूक्ष्म अध्यपन नामुमकिन हो गया । दीधितिकार आदि से नवीन न्याय पल्लवित और पुष्पित होने के बाद प्रायः प्रत्येक दर्शनकार नवीन न्याय की परिभाषा को अपना कर अपने सिद्धांतों का सूक्ष्म एवं सतर्क प्रतिपादन करने को उद्यत बने । मधुसूदन सरस्वती के अवैतसिद्धिग्रन्थ की गौडब्रह्मानंदी टीका, काव्यप्रकाशव्याख्या, परिभाषा शब्देन्दुशेखर, जल्पकल्पतरु, मञ्जूषा आदि वेदान्त आदि दर्शनों के ग्रंथों में नव्य न्याय की पदावली का काफि उपयोग किया गया है, जिनमें स्वसिद्धान्तस्थापन एवं परसिद्धान्तनिकन्दन किया गया है। अन्य नन्य दार्शनिकों ने स्याद्वाद का भी विना सोचे समझे खण्डन किया । अनएव नवीन न्याय की शैली में स्याद्वादबाधक कुतको का निरसन एवं स्थाबाद का सूक्ष्म समीचीन प्रतिपादन करना जैन मनीषियों के लिये कर्तव्य बना। इस कार्य का श्रीगणेश महामहोपाध्याय १. न्या.सू.वा.भा. १-१-१Page Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 370