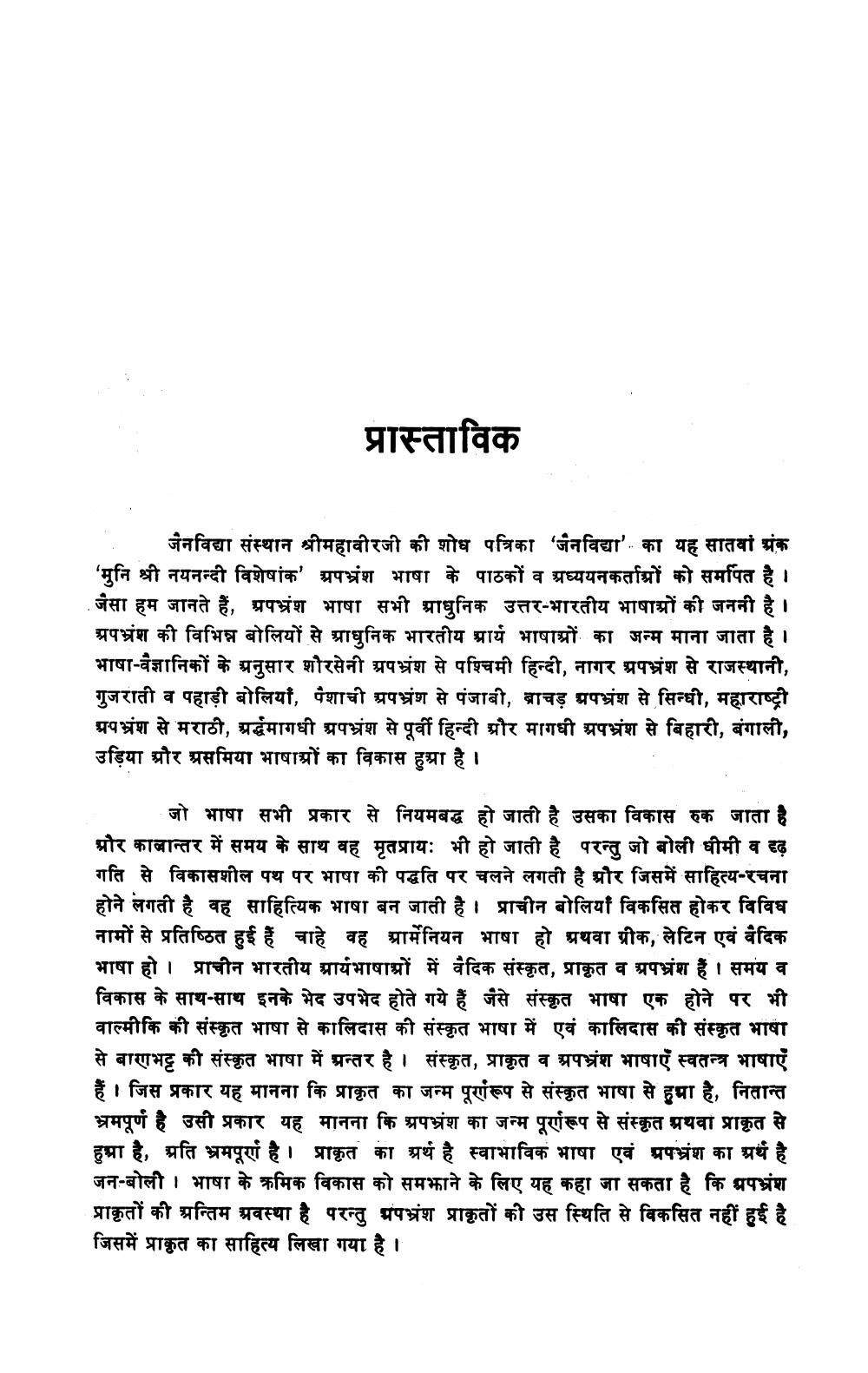Book Title: Jain Vidya 07 Author(s): Pravinchandra Jain & Others Publisher: Jain Vidya Samsthan View full book textPage 7
________________ प्रास्ताविक ___ जैनविद्या संस्थान श्रीमहावीरजी की शोध पत्रिका 'जनविद्या' का यह सातवां अंक 'मुनि श्री नयनन्दी विशेषांक' अपभ्रंश भाषा के पाठकों व अध्ययनकर्ताओं को समर्पित है। जैसा हम जानते हैं, अपभ्रंश भाषा सभी आधुनिक उत्तर-भारतीय भाषाओं की जननी है । अपभ्रंश की विभिन्न बोलियों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म माना जाता है । भाषा-वैज्ञानिकों के अनुसार शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिन्दी, नागर अपभ्रंश से राजस्थानी, गुजराती व पहाड़ी बोलियां, पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिन्धी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, अर्द्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिन्दी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास हुआ है । जो भाषा सभी प्रकार से नियमबद्ध हो जाती है उसका विकास रुक जाता है और कालान्तर में समय के साथ वह मृतप्रायः भी हो जाती है परन्तु जो बोली धीमी व दृढ़ गति से विकासशील पथ पर भाषा की पद्धति पर चलने लगती है और जिसमें साहित्य-रचना होने लगती है वह साहित्यिक भाषा बन जाती है। प्राचीन बोलियां विकसित होकर विविध नामों से प्रतिष्ठित हुई हैं चाहे वह आर्मेनियन भाषा हो अथवा ग्रीक, लेटिन एवं वैदिक भाषा हो । प्राचीन भारतीय आर्यभाषाओं में वैदिक संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश हैं । समय व विकास के साथ-साथ इनके भेद उपभेद होते गये हैं जैसे संस्कृत भाषा एक होने पर भी वाल्मीकि की संस्कृत भाषा से कालिदास की संस्कृत भाषा में एवं कालिदास की संस्कृत भाषा से बाणभट्ट की संस्कृत भाषा में अन्तर है। संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश भाषाएं स्वतन्त्र भाषाएं हैं । जिस प्रकार यह मानना कि प्राकृत का जन्म पूर्णरूप से संस्कृत भाषा से हुमा है, नितान्त भ्रमपूर्ण है उसी प्रकार यह मानना कि अपभ्रंश का जन्म पूर्णरूप से संस्कृत अथवा प्राकृत से हुमा है, अति भ्रमपूर्ण है। प्राकृत का अर्थ है स्वाभाविक भाषा एवं अपभ्रंश का अर्थ है जन-बोली । भाषा के क्रमिक विकास को समझाने के लिए यह कहा जा सकता है कि अपभ्रंश प्राकृतों की अन्तिम अवस्था है परन्तु अपभ्रंश प्राकृतों की उस स्थिति से विकसित नहीं हुई है जिसमें प्राकृत का साहित्य लिखा गया है।Page Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 116