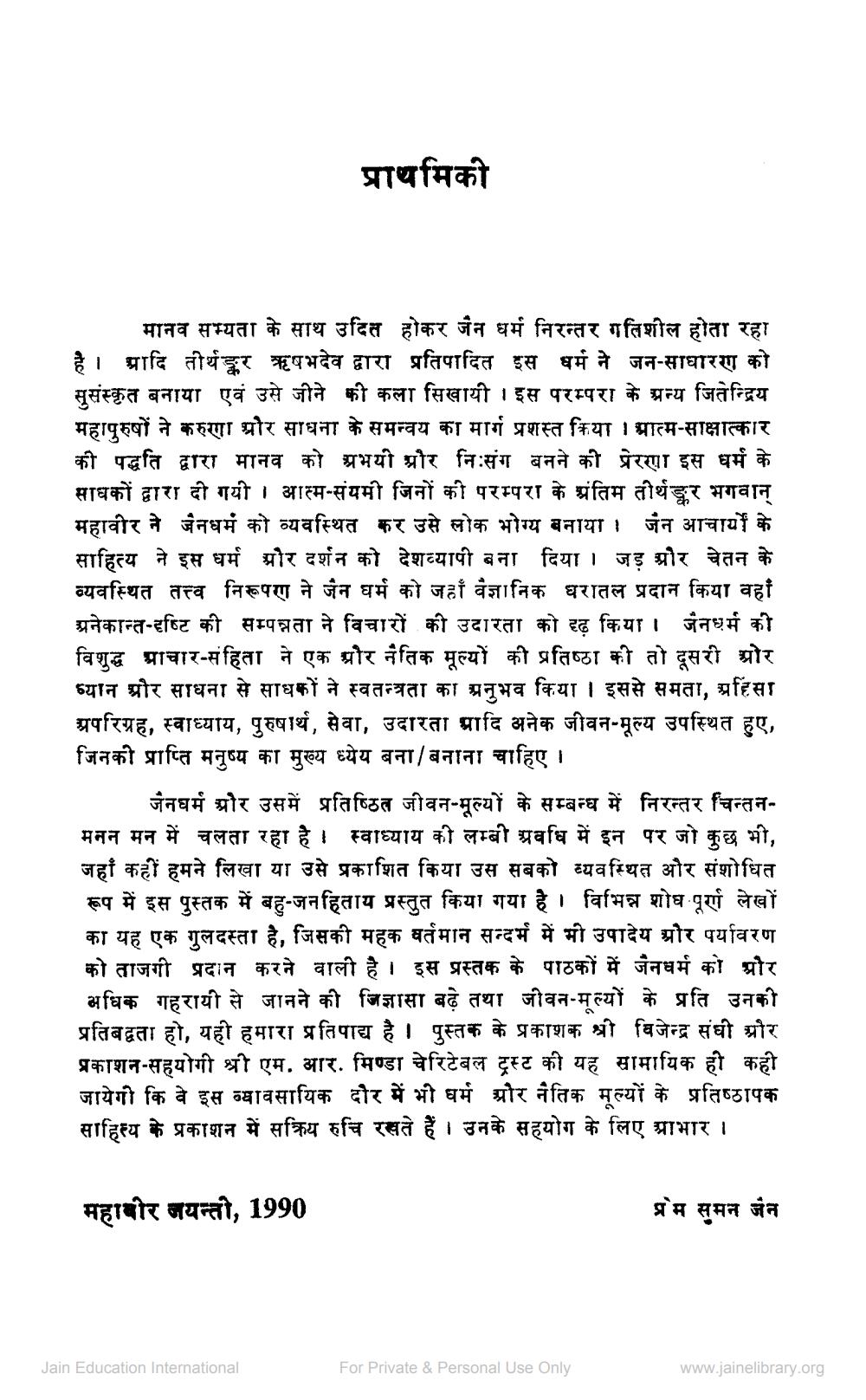Book Title: Jain Dharm aur Jivan Mulya Author(s): Prem Suman Jain Publisher: Sanghi Prakashan Jaipur View full book textPage 7
________________ प्राथमिकी मानव सभ्यता के साथ उदित होकर जैन धर्म निरन्तर गतिशील होता रहा है। प्रादि तीर्थङ्कर ऋषभदेव द्वारा प्रतिपादित इस धर्म ने जन-साधारण को सुसंस्कृत बनाया एवं उसे जीने की कला सिखायी । इस परम्परा के अन्य जितेन्द्रिय महापुरुषों ने करुणा और साधना के समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया । प्रात्म-साक्षात्कार की पद्धति द्वारा मानव को अभयी और निःसंग बनने की प्रेरणा इस धर्म के साधकों द्वारा दी गयी । आत्म-संयमी जिनों की परम्परा के अंतिम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर ने जैनधर्म को व्यवस्थित कर उसे लोक भोग्य बनाया। जैन आचार्यों के साहित्य ने इस धर्म और दर्शन को देशव्यापी बना दिया। जड़ और चेतन के व्यवस्थित तत्त्व निरूपण ने जैन धर्म को जहाँ वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया वहां अनेकान्त-दृष्टि की सम्पन्नता ने विचारों की उदारता को दृढ़ किया। जैनधर्म की विशुद्ध प्राचार-संहिता ने एक और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की तो दूसरी ओर ध्यान और साधना से साधकों ने स्वतन्त्रता का अनुभव किया। इससे समता, अहिंसा अपरिग्रह, स्वाध्याय, पुरुषार्थ, सेवा, उदारता मादि अनेक जीवन-मूल्य उपस्थित हुए, जिनकी प्राप्ति मनुष्य का मुख्य ध्येय बना/ बनाना चाहिए । जैनधर्म और उसमें प्रतिष्ठित जीवन-मूल्यों के सम्बन्ध में निरन्तर चिन्तनमनन मन में चलता रहा है। स्वाध्याय की लम्बी अवधि में इन पर जो कुछ भी, जहाँ कहीं हमने लिखा या उसे प्रकाशित किया उस सबको व्यवस्थित और संशोधित रूप में इस पुस्तक में बहु-जन हिताय प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न शोध पूर्ण लेखों का यह एक गुलदस्ता है, जिसकी महक वर्तमान सन्दर्म में भी उपादेय और पर्यावरण को ताजगी प्रदान करने वाली है। इस प्रस्तक के पाठकों में जैनधर्म को और भधिक गहरायी से जानने की जिज्ञासा बढ़े तथा जीवन-मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्वता हो, यही हमारा प्रतिपाद्य है । पुस्तक के प्रकाशक श्री विजेन्द्र संघी और प्रकाशन-सहयोगी श्री एम. आर. मिण्डा चेरिटेबल ट्रस्ट की यह सामायिक ही कही जायेगी कि वे इस व्यावसायिक दौर में भी धर्म और नैतिक मूल्यों के प्रतिष्ठापक साहित्य के प्रकाशन में सक्रिय रुचि रखते हैं। उनके सहयोग के लिए प्राभार । महाबीर जयन्ती, 1990 प्रेम समन जैन Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 140