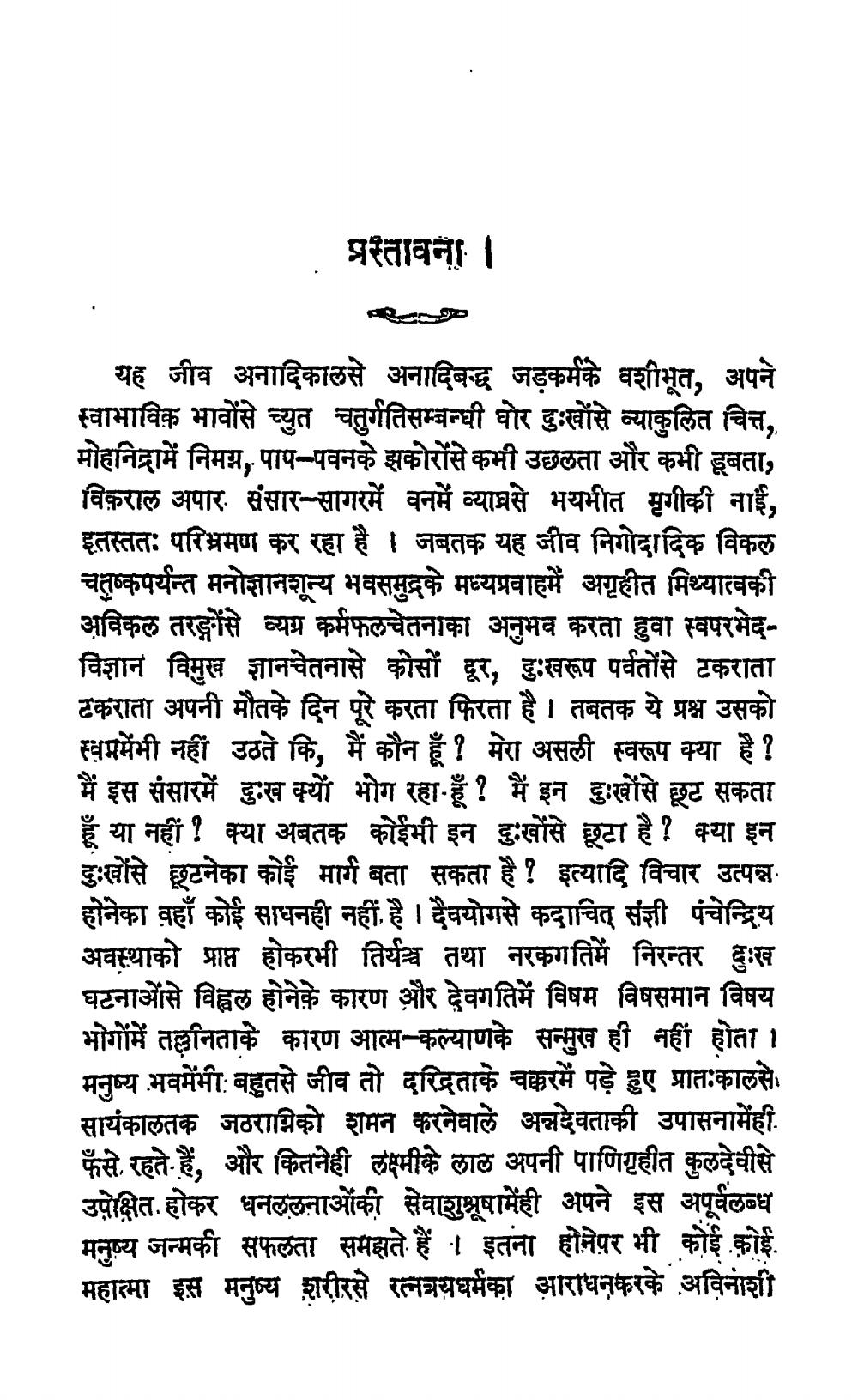Book Title: Jain Siddhant Darpan Author(s): Gopaldas Baraiya Publisher: Anantkirti Digambar Jain Granthmala Samiti View full book textPage 9
________________ प्रस्तावना । यह जीव अनादिकाल से अनादिबद्ध जड़कर्मके वशीभूत, अपने स्वाभाविक भावोंसे च्युत चतुर्गतिसम्बन्धी घोर दुःखोंसे व्याकुलित चित्त, मोहनिद्रामें निमग्न, पाप-पवनके झकोरोंसे कभी उछलता और कभी डूबता, विकराल अपार संसार - सागरमें वनमें व्याघ्र से भयभीत मृगीकी नाई, इतस्ततः परिभ्रमण कर रहा है । जबतक यह जीव निगोदादिक विकल चतुष्कपर्यन्त मनोज्ञानशून्य भवसमुद्रके मध्यप्रवाहमें अगृहीत मिथ्यात्वकी अविकल तरड्रोंसे व्यग्र कर्मफलचेतनाका अनुभव करता हुवा स्वपरभेदविज्ञान विमुख ज्ञानचेतनासे कोसों दूर दुःखरूप पर्वतोंसे टकराता टकराता अपनी मौत के दिन पूरे करता फिरता है । तबतक ये प्रश्न उसको स्वमभी नहीं उठते कि, मैं कौन हूँ? मेरा असली स्वरूप क्या है ? मैं इस संसार में दुःख क्यों भोग रहा हूँ ? मैं इन दुःखोंसे छूट सकता हूँ या नहीं ? क्या अबतक कोईमी इन दुःखोंसे छूटा है ? क्या इन दुःखोंसे छूटनेका कोई मार्ग बता सकता है ? इत्यादि विचार उत्पन्न होनेका वहाँ कोई साधनही नहीं है । दैवयोगसे कदाचित् संज्ञी पंचेन्द्रिय अवस्थाको प्राप्त होकरभी तिर्यञ्च तथा नरकगतिमें निरन्तर दुःख घटनाओंसे विह्वल होनेके कारण और देवगतिमें विषम विषसमान विषय भोगों में तल्लीनता के कारण आत्म-कल्याणके सन्मुख ही नहीं होता । मनुष्य भवभी: बहुतसे जीव तो दरिद्रताके चक्कर में पड़े हुए प्रातः काल से सायंकालतक जठराग्निको शमन करनेवाले अन्नदेवताकी उपासनामेंही. फँसे रहते हैं, और कितनेही लक्ष्मीके लाल अपनी पाणिगृहीत कुलदेवीसे उपेक्षित होकर धनललनाओं की सेवाशुश्रूषामें ही अपने इस अपूर्वलब्ध मनुष्य जन्मकी सफलता समझते हैं । इतना होनेपर भी कोई कोई. महात्मा इस मनुष्य शरीरसे रत्नत्रयधर्मका आराधनकरके अविनाशीPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 169