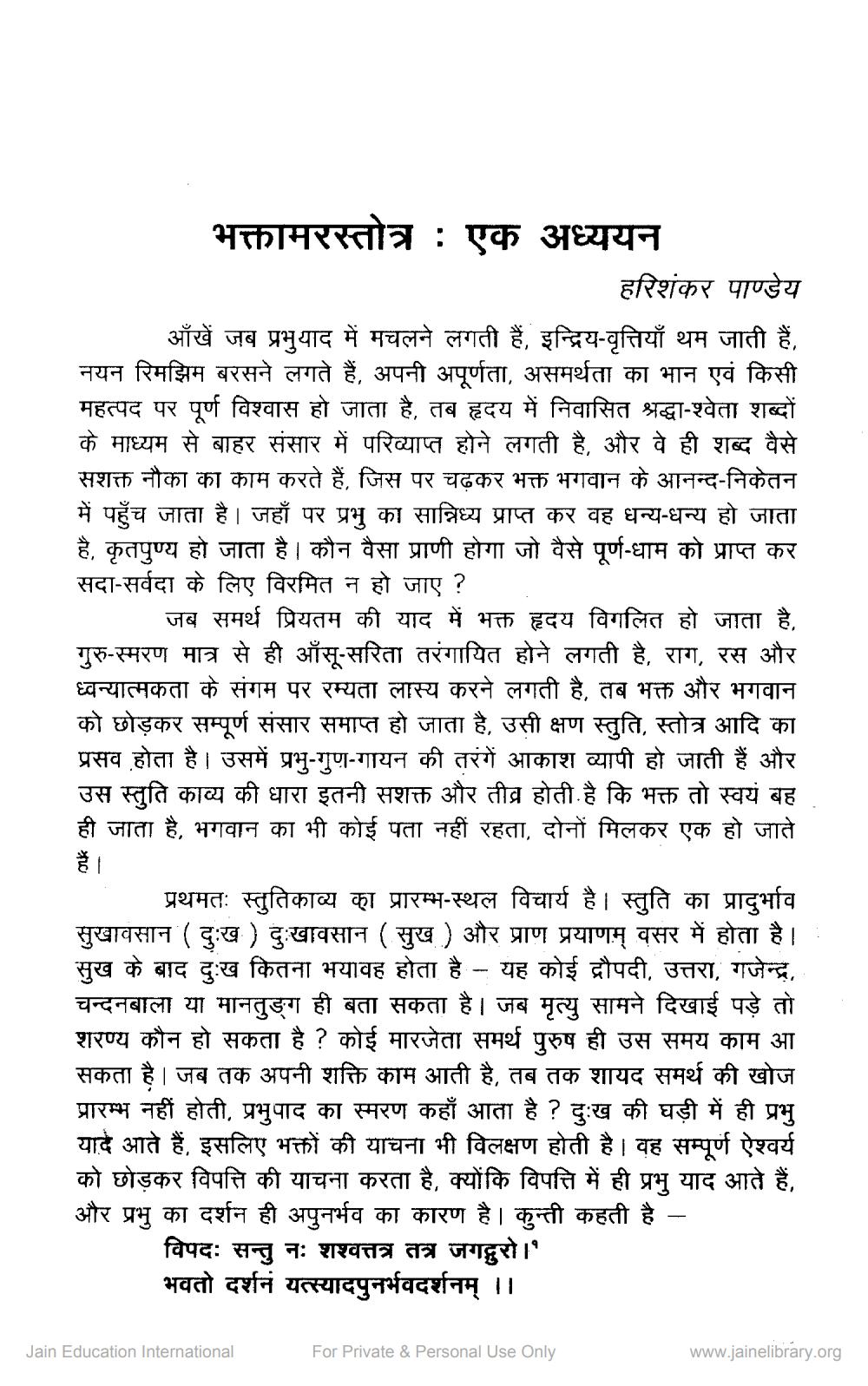Book Title: Sramana 1995 07 Author(s): Ashok Kumar Singh Publisher: Parshvanath Vidhyashram Varanasi View full book textPage 9
________________ भक्तामरस्तोत्र : एक अध्ययन हरिशंकर पाण्डेय आँखें जब प्रभुयाद में मचलने लगती हैं, इन्द्रिय-वृत्तियाँ थम जाती हैं, नयन रिमझिम बरसने लगते हैं, अपनी अपूर्णता, असमर्थता का भान एवं किसी महत्पद पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, तब हृदय में निवासित श्रद्धा-श्वेता शब्दों के माध्यम से बाहर संसार में परिव्याप्त होने लगती है, और वे ही शब्द वैसे सशक्त नौका का काम करते हैं, जिस पर चढ़कर भक्त भगवान के आनन्द-निकेतन में पहुँच जाता है। जहाँ पर प्रभु का सान्निध्य प्राप्त कर वह धन्य-धन्य हो जाता है, कृतपुण्य हो जाता है। कौन वैसा प्राणी होगा जो वैसे पूर्ण-धाम को प्राप्त कर सदा-सर्वदा के लिए विरमित न हो जाए ? जब समर्थ प्रियतम की याद में भक्त हृदय विगलित हो जाता है, गुरु-स्मरण मात्र से ही आँसू-सरिता तरंगायित होने लगती है, राग, रस और ध्वन्यात्मकता के संगम पर रम्यता लास्य करने लगती है, तब भक्त और भगवान को छोड़कर सम्पूर्ण संसार समाप्त हो जाता है, उसी क्षण स्तुति, स्तोत्र आदि का प्रसव होता है। उसमें प्रभु-गुण-गायन की तरंगें आकाश व्यापी हो जाती हैं और उस स्तुति काव्य की धारा इतनी सशक्त और तीव्र होती है कि भक्त तो स्वयं बह ही जाता है, भगवान का भी कोई पता नहीं रहता, दोनों मिलकर एक हो जाते प्रथमतः स्तुतिकाव्य का प्रारम्भ-स्थल विचार्य है। स्तुति का प्रादुर्भाव सुखावसान ( दुःख) दुःखावसान ( सुख ) और प्राण प्रयाणम् वसर में होता है। सुख के बाद दुःख कितना भयावह होता है - यह कोई द्रौपदी, उत्तरा, गजेन्द्र, चन्दनबाला या मानतुङ्ग ही बता सकता है। जब मृत्यु सामने दिखाई पड़े तो शरण्य कौन हो सकता है ? कोई मारजेता समर्थ पुरुष ही उस समय काम आ सकता है। जब तक अपनी शक्ति काम आती है, तब तक शायद समर्थ की खोज प्रारम्भ नहीं होती, प्रभुपाद का स्मरण कहाँ आता है ? दुःख की घड़ी में ही प्रभु याद आते हैं, इसलिए भक्तों की याचना भी विलक्षण होती है। वह सम्पूर्ण ऐश्वर्य को छोड़कर विपत्ति की याचना करता है, क्योंकि विपत्ति में ही प्रभु याद आते हैं, और प्रभु का दर्शन ही अपुनर्भव का कारण है। कुन्ती कहती है - विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो।' भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ।। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 104