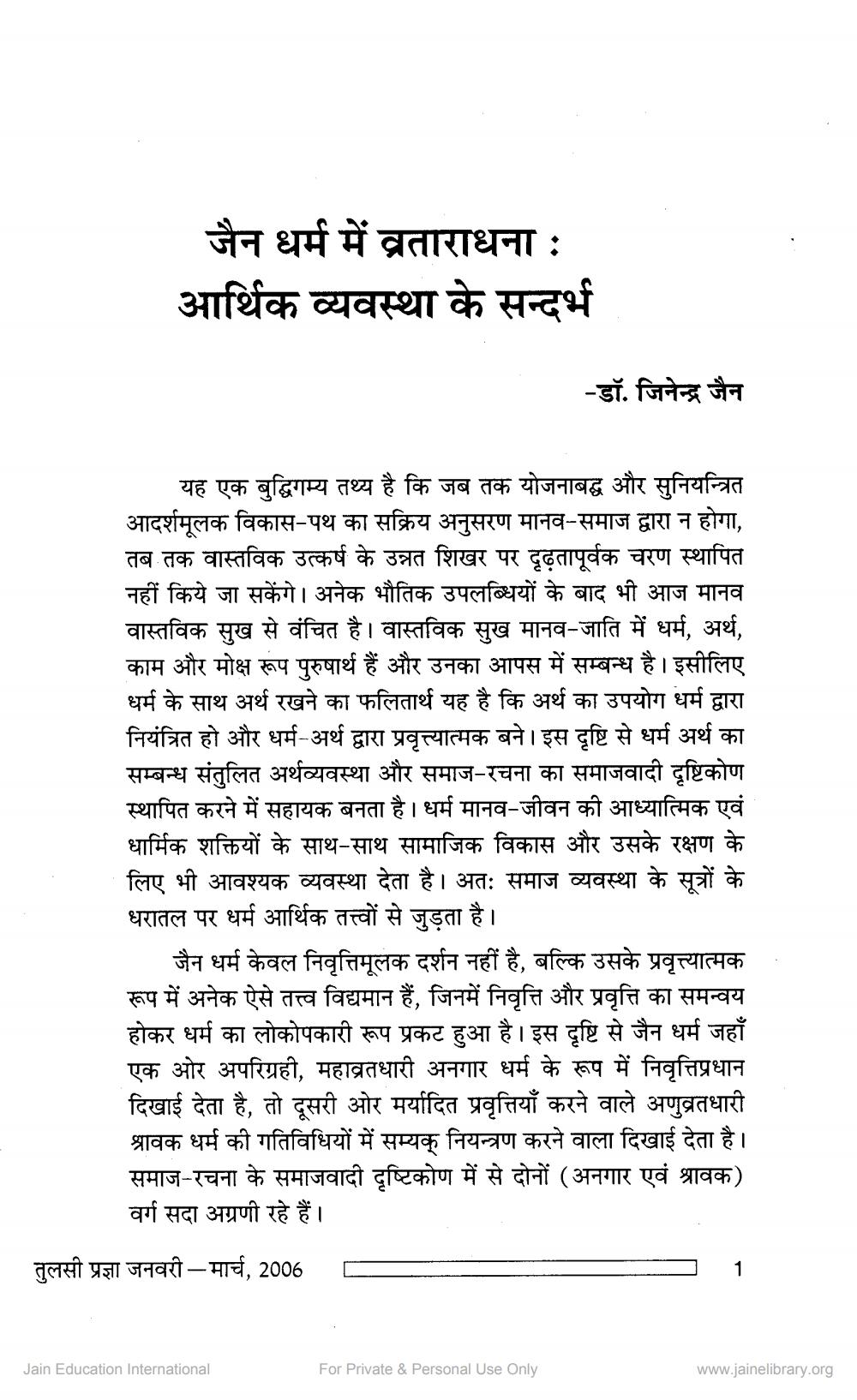Book Title: Tulsi Prajna 2006 01 Author(s): Shanta Jain, Jagatram Bhattacharya Publisher: Jain Vishva Bharati View full book textPage 6
________________ जैन धर्म में व्रताराधना : आर्थिक व्यवस्था के सन्दर्भ यह एक बुद्धिगम्य तथ्य है कि जब तक योजनाबद्ध और सुनियन्त्रित आदर्शमूलक विकास-पथ का सक्रिय अनुसरण मानव-समाज द्वारा न होगा, तब तक वास्तविक उत्कर्ष के उन्नत शिखर पर दृढ़तापूर्वक चरण स्थापित नहीं किये जा सकेंगे । अनेक भौतिक उपलब्धियों के बाद भी आज मानव वास्तविक सुख से वंचित है । वास्तविक सुख मानव-जाति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ हैं और उनका आपस में सम्बन्ध है । इसीलिए धर्म के साथ अर्थ रखने का फलितार्थ यह है कि अर्थ का उपयोग धर्म द्वारा नियंत्रित हो और धर्म - अर्थ द्वारा प्रवृत्त्यात्मक बने। इस दृष्टि से धर्म अर्थ का सम्बन्ध संतुलित अर्थव्यवस्था और समाज - रचना का समाजवादी दृष्टिकोण स्थापित करने में सहायक बनता है । धर्म मानव-जीवन की आध्यात्मिक एवं धार्मिक शक्तियों के साथ-साथ सामाजिक विकास और उसके रक्षण के लिए भी आवश्यक व्यवस्था देता है । अतः समाज व्यवस्था के सूत्रों के धरातल पर धर्म आर्थिक तत्त्वों से जुड़ता है। जैन धर्म केवल निवृत्तिमूलक दर्शन नहीं है, बल्कि उसके प्रवृत्त्यात्मक रूप में अनेक ऐसे तत्त्व विद्यमान हैं, जिनमें निवृत्ति और प्रवृत्ति का समन्वय होकर धर्म का लोकोपकारी रूप प्रकट हुआ है । इस दृष्टि से जैन धर्म जहाँ एक ओर अपरिग्रही, महाव्रतधारी अनगार धर्म के रूप में निवृत्तिप्रधान दिखाई देता है, तो दूसरी ओर मर्यादित प्रवृत्तियाँ करने वाले अणुव्रतधारी श्रावक धर्म की गतिविधियों में सम्यक् नियन्त्रण करने वाला दिखाई देता है । समाज-रचना के समाजवादी दृष्टिकोण में से दोनों (अनगार एवं श्रावक) वर्ग सदा अग्रणी रहे हैं । तुलसी प्रज्ञा जनवरी-मार्च, 2006 - डॉ. जिनेन्द्र जैन Jain Education International For Private & Personal Use Only 1 www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 122