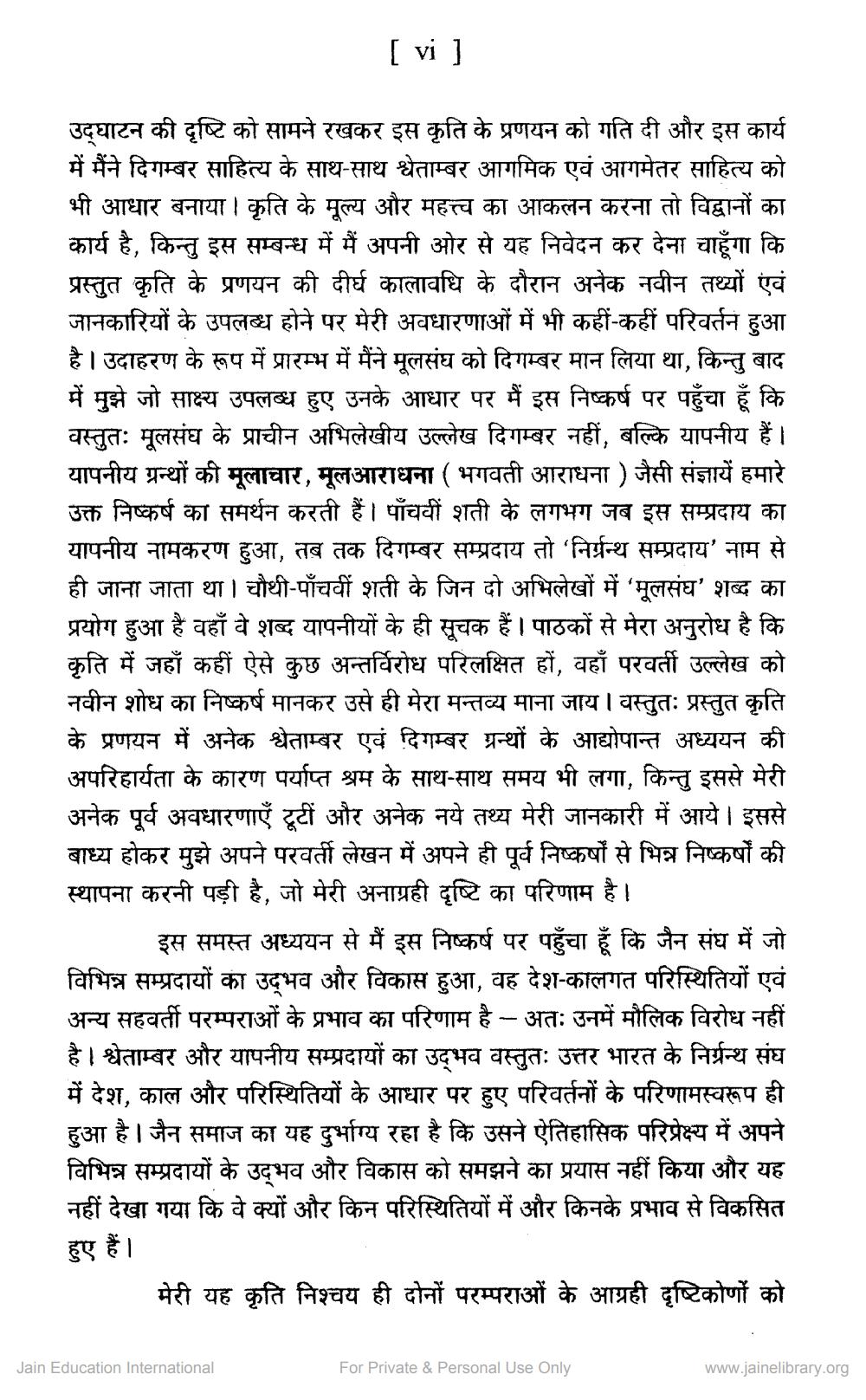Book Title: Jain Dharma ka Yapniya Sampraday Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Parshwanath Shodhpith Varanasi View full book textPage 8
________________ [ vi ] उद्घाटन की दृष्टि को सामने रखकर इस कृति के प्रणयन को गति दी और इस कार्य मैंने दिगम्बर साहित्य के साथ-साथ श्वेताम्बर आगमिक एवं आगमेतर साहित्य को भी आधार बनाया । कृति के मूल्य और महत्त्व का आकलन करना तो विद्वानों का कार्य है, किन्तु इस सम्बन्ध में मैं अपनी ओर से यह निवेदन कर देना चाहूँगा कि प्रस्तुत कृति के प्रणयन की दीर्घ कालावधि के दौरान अनेक नवीन तथ्यों एवं जानकारियों के उपलब्ध होने पर मेरी अवधारणाओं में भी कहीं-कहीं परिवर्तन हुआ है । उदाहरण के रूप में प्रारम्भ में मैंने मूलसंघ को दिगम्बर मान लिया था, किन्तु बाद में मुझे जो साक्ष्य उपलब्ध हुए उनके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वस्तुतः मूलसंघ के प्राचीन अभिलेखीय उल्लेख दिगम्बर नहीं, बल्कि यापनीय हैं । यापनीय ग्रन्थों की मूलाचार, मूल आराधना ( भगवती आराधना ) जैसी संज्ञायें हमारे उक्त निष्कर्ष का समर्थन करती हैं। पाँचवीं शती के लगभग जब इस सम्प्रदाय का यापनीय नामकरण हुआ, तब तक दिगम्बर सम्प्रदाय तो 'निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय' नाम से जाना जाता था। चौथी पाँचवीं शती के जिन दो अभिलेखों में 'मूलसंघ' शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ वे शब्द यापनीयों के ही सूचक हैं। पाठकों से मेरा अनुरोध है कि कृति में जहाँ कहीं ऐसे कुछ अन्तर्विरोध परिलक्षित हों, वहाँ परवर्ती उल्लेख को नवीन शोध का निष्कर्ष मानकर उसे ही मेरा मन्तव्य माना जाय । वस्तुतः प्रस्तुत कृति के प्रणयन में अनेक श्वेताम्बर एवं दिगम्बर ग्रन्थों के आद्योपान्त अध्ययन की अपरिहार्यता के कारण पर्याप्त श्रम के साथ-साथ समय भी लगा, किन्तु इससे मेरी अनेक पूर्व अवधारणाएँ टूटीं और अनेक नये तथ्य मेरी जानकारी में आये । इससे बाध्य होकर मुझे अपने परवर्ती लेखन में अपने ही पूर्व निष्कर्षों से भिन्न निष्कर्षों की स्थापना करनी पड़ी है, जो मेरी अनाग्रही दृष्टि का परिणाम है । इस समस्त अध्ययन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जैन संघ में जो विभिन्न सम्प्रदायों का उद्भव और विकास हुआ, वह देश - कालगत परिस्थितियों एवं अन्य सहवर्ती परम्पराओं के प्रभाव का परिणाम है। अतः उनमें मौलिक विरोध नहीं है । श्वेताम्बर और यापनीय सम्प्रदायों का उद्भव वस्तुतः उत्तर भारत के निर्ग्रन्थ संघ में देश, काल और परिस्थितियों के आधार पर हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ही हुआ है। जैन समाज का यह दुर्भाग्य रहा है कि उसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपने विभिन्न सम्प्रदायों के उद्भव और विकास को समझने का प्रयास नहीं किया और यह नहीं देखा गया कि वे क्यों और किन परिस्थितियों में और किनके प्रभाव से विकसित हुए हैं। मेरी यह कृति निश्चय ही दोनों परम्पराओं के आग्रही दृष्टिकोणों को Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 550