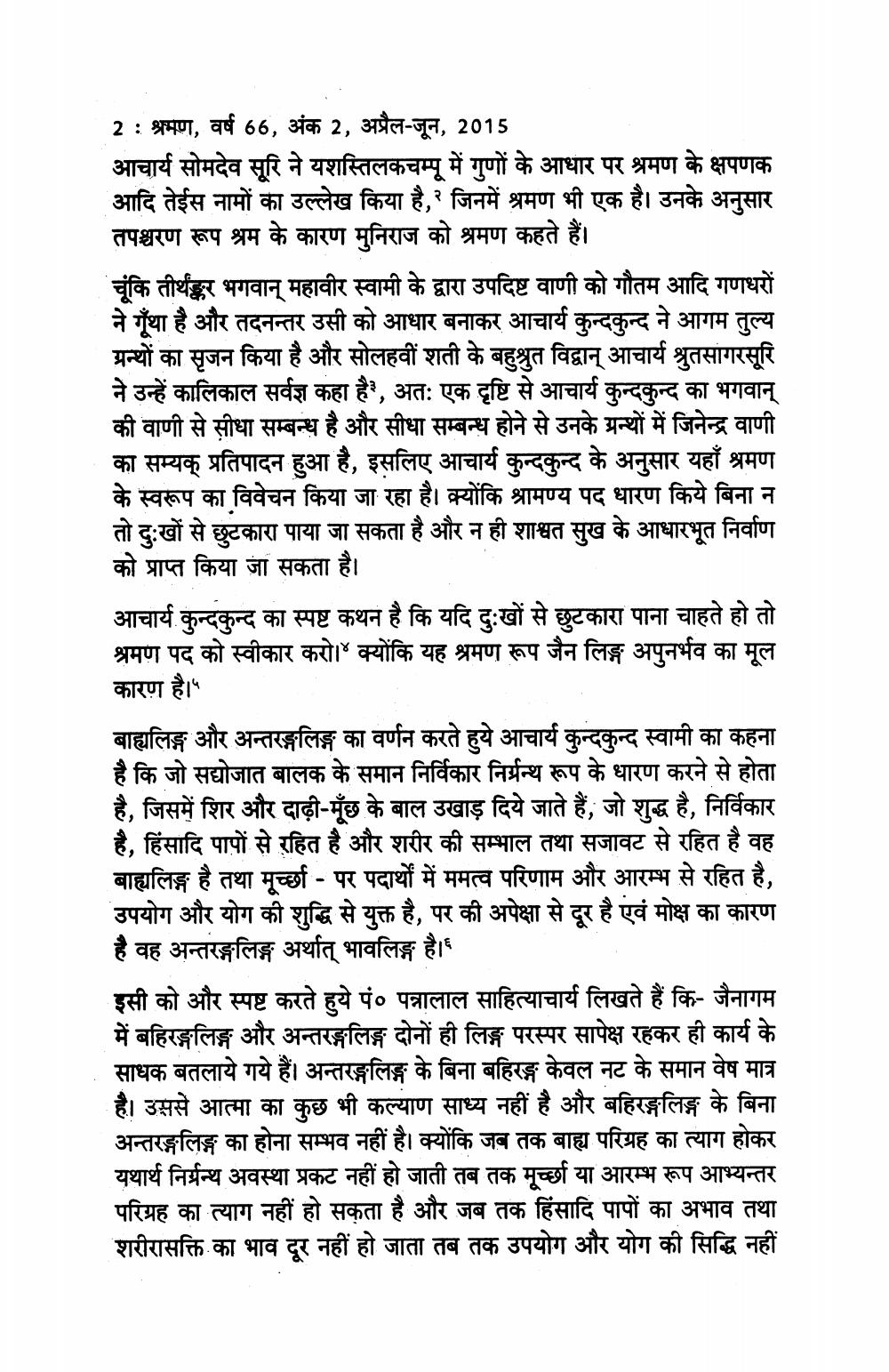Book Title: Sramana 2015 04 Author(s): Sundarshanlal Jain, Ashokkumar Singh Publisher: Parshvanath Vidhyashram Varanasi View full book textPage 9
________________ 2 : श्रमण, वर्ष 66, अंक 2, अप्रैल-जून, 2015 आचार्य सोमदेव सरि ने यशस्तिलकचम्पू में गुणों के आधार पर श्रमण के क्षपणक आदि तेईस नामों का उल्लेख किया है, जिनमें श्रमण भी एक है। उनके अनुसार तपश्चरण रूप श्रम के कारण मुनिराज को श्रमण कहते हैं। चूंकि तीर्थङ्कर भगवान् महावीर स्वामी के द्वारा उपदिष्ट वाणी को गौतम आदि गणधरों ने गूंथा है और तदनन्तर उसी को आधार बनाकर आचार्य कुन्दकुन्द ने आगम तुल्य ग्रन्थों का सृजन किया है और सोलहवीं शती के बहुश्रुत विद्वान् आचार्य श्रुतसागरसूरि ने उन्हें कालिकाल सर्वज्ञ कहा है, अत: एक दृष्टि से आचार्य कुन्दकुन्द का भगवान् की वाणी से सीधा सम्बन्ध है और सीधा सम्बन्ध होने से उनके ग्रन्थों में जिनेन्द्र वाणी का सम्यक् प्रतिपादन हुआ है, इसलिए आचार्य कुन्दकुन्द के अनुसार यहाँ श्रमण के स्वरूप का विवेचन किया जा रहा है। क्योंकि श्रामण्य पद धारण किये बिना न तो दुःखों से छुटकारा पाया जा सकता है और न ही शाश्वत सुख के आधारभूत निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य कुन्दकुन्द का स्पष्ट कथन है कि यदि दुःखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो श्रमण पद को स्वीकार करो। क्योंकि यह श्रमण रूप जैन लिङ्ग अपुनर्भव का मूल कारण है। बाह्यलिङ्ग और अन्तरङ्गलिङ्ग का वर्णन करते हुये आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी का कहना है कि जो सद्योजात बालक के समान निर्विकार निम्रन्थ रूप के धारण करने से होता है, जिसमें शिर और दाढ़ी-मूंछ के बाल उखाड़ दिये जाते हैं, जो शुद्ध है, निर्विकार है, हिंसादि पापों से रहित है और शरीर की सम्भाल तथा सजावट से रहित है वह बाह्यलिङ्ग है तथा मूर्छा - पर पदार्थों में ममत्व परिणाम और आरम्भ से रहित है, उपयोग और योग की शुद्धि से युक्त है, पर की अपेक्षा से दूर है एवं मोक्ष का कारण है वह अन्तरङ्गलिङ्ग अर्थात् भावलिङ्ग है। इसी को और स्पष्ट करते हुये पं० पन्नालाल साहित्याचार्य लिखते हैं कि- जैनागम में बहिरङ्गलिङ्ग और अन्तरङ्गलिङ्ग दोनों ही लिङ्ग परस्पर सापेक्ष रहकर ही कार्य के साधक बतलाये गये हैं। अन्तरङ्गलिङ्ग के बिना बहिरङ्ग केवल नट के समान वेष मात्र है। उससे आत्मा का कुछ भी कल्याण साध्य नहीं है और बहिरङ्गलिङ्ग के बिना अन्तरङ्गलिङ्ग का होना सम्भव नहीं है। क्योंकि जब तक बाह्य परिग्रह का त्याग होकर यथार्थ निर्ग्रन्थ अवस्था प्रकट नहीं हो जाती तब तक मूर्छा या आरम्भ रूप आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग नहीं हो सकता है और जब तक हिंसादि पापों का अभाव तथा शरीरासक्ति का भाव दूर नहीं हो जाता तब तक उपयोग और योग की सिद्धि नहींPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 210