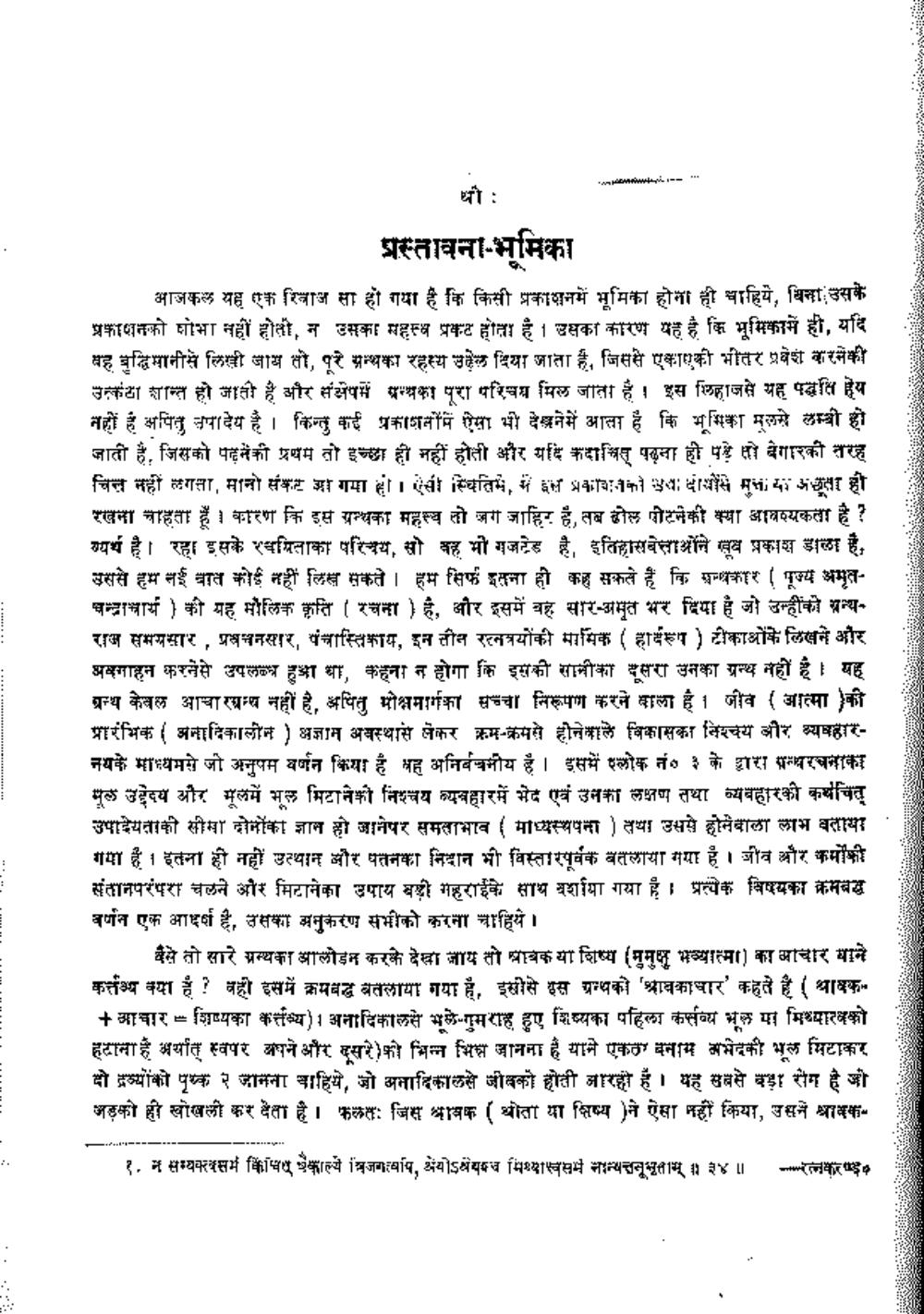Book Title: Purusharthsiddhyupay Author(s): Amrutchandracharya, Munnalal Randheliya Varni Publisher: Swadhin Granthamala Sagar View full book textPage 5
________________ -in श्री : प्रस्तावना - भूमिका 1 आजकल यह एक रिवाज सा हो गया है कि किसी प्रकाशनमें भूमिका होना ही चाहिये, बिना उसके oturn पोभा नहीं होती, न उसका महत्व प्रकट होता है । उसका कारण यह है कि भूमिकामें ही, यदि वह बुद्धिमानी से लिखी जाय तो पूरे ग्रन्थका रहस्य उकेल दिया जाता है, जिससे एकाएकी भीतर प्रवेश करनेकी उत्कंठा शान्त हो जाती है और संक्षेपमें ग्रन्थका पूरा परिचय मिल जाता है। इस लिहाज से यह पद्धति है नहीं है अपितु उपादेय है। किन्तु कई प्रकाशनोंमें ऐसा भी देखने में आता है कि भूमिका मुलसे लम्बी हो जाती हैं, जिसको पढ़ने की प्रथम तो इच्छा ही नहीं होती और यदि कदाचित् पढ़ना ही पड़े तो बेगारकी तरह चि नहीं लगता, मानो संकट आ गया हो। ऐसी स्थिति में इस प्रकाशनको यादमुक्ता अछूता ही रखना चाहता हूँ । कारण कि इस ग्रन्थका महस्व तो जग जाहिर है, तब ढोल पीटने की क्या आवश्यकता है ? व्यर्थ है। रहा इसके रचयिताका परिचय, सो वह भी गजटेड है, इतिहासवेत्ताओंने खूब प्रकाश डाला है, उससे हम नई बात कोई नहीं लिख सकते। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ग्रन्थकार ( पूज्य अमृतwater ) की यह मौलिक कृति ( रचना ) है, और इसमें वह सार-अमृत भर दिया है जो उन्हींको ग्रन्थराज समार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, इन तीन रत्नत्रयोंकी मार्मिक ( हार्दरूप ) टीकाओंके लिखने और अमान करनेसे उपलब्ध हुआ था, कहना न होगा कि इसकी सानीका दूसरा उनका ग्रन्थ नहीं हूँ। यह ग्रन्थ केवल आचारम्य नहीं है, अपितु मोक्षमार्गका सच्चा निरूपण करने वाला है । जीव ( आत्मा ) की प्रारंभिक ( अनादिकालीन ) अज्ञान अवस्थासे लेकर क्रम-क्रमसे होनेवाले विकासका निश्चय और व्यवहारनथके माध्यम से जो अनुपम वर्णन किया है वह अनिर्वचनीय है । इसमें श्लोक नं० ३ के द्वारा सन्थरचनाका मूल उद्देश्य और मूलमें भूल मिटानेको निश्चय व्यवहारमें भेद एवं उनका लक्षण तथा व्यवहारकी कर्यचित् उपादेयताकी सीमा दोनोंका ज्ञान हो जानेपर समताभाव ( माध्यस्थपना ) तथा उससे होनेवाला लाभ बताया गया है । इतना ही नहीं उत्थान और पतनका निदान भी विस्तारपूर्वक बतलाया गया है। जीव और कर्मोकी संतानपरंपरा चलने और मिटानेका उपाय बड़ी महराईके साथ वर्शाया गया है। प्रत्येक विषयका कम वर्णन एक आदर्श है, उसका अनुकरण सभीको करना चाहिये। वैसे तो सारे ग्रन्थका आलोडन करके देखा जाय तो श्रावक या शिष्य (मुमुक्षु भव्यात्मा) का आचार याने for a है ? वह इसमें क्रमबद्ध बतलाया गया है, इससे इस ग्रन्थको 'श्रावकाचार' कहते हैं ( आवक+ आचार = शिष्यका कर्त्तव्य ) | अनादिकालसे भूळे गुमराह हुए शिष्यका पहिला कर्तव्य भूल या मियाको हटाना है अर्थात् स्वपर अपने और दूसरे को भिन्न भिन्न जानना है याने एकता बनाम अभेद भूल मिटाकर दो को पृथ्क २ जानना चाहिये, जो अनादिकालसे जीवको होती जारही है। यह सबसे बड़ा रोग है जो reer ही खोखली कर देता है । फलत: जिस श्रावक ( श्रोता या शिष्य ) ने ऐसा नहीं किया, उसने श्रावक १. न सम्यक्स किंवा त्रिजगत् योऽयक्च मिश्यास्वसमे नान्यन्तनुभृताम् ॥ ३४ ॥ रत्नकरण्डPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 478