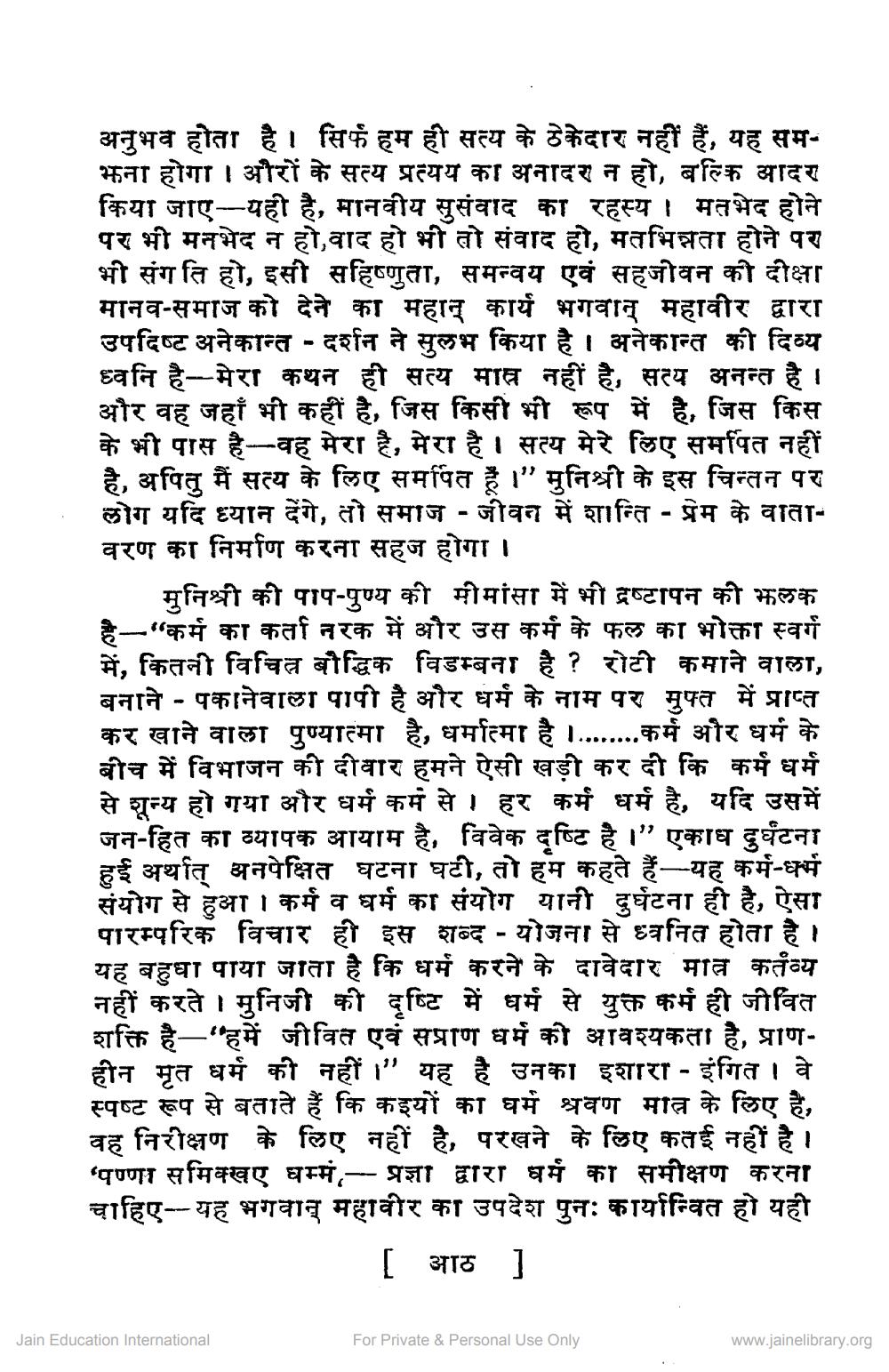Book Title: Chintan ke Zarokhese Part 3 Author(s): Amarmuni Publisher: Tansukhrai Daga Veerayatan View full book textPage 9
________________ अनुभव होता है। सिर्फ हम ही सत्य के ठेकेदार नहीं हैं, यह समझना होगा । औरों के सत्य प्रत्यय का अनादर न हो, बल्कि आदर किया जाए-यही है, मानवीय सुसंवाद का रहस्य । मतभेद होने पर भी मनभेद न हो,वाद हो भी तो संवाद हो, मतभिन्नता होने पर भी संगति हो, इसी सहिष्णुता, समन्वय एवं सहजीवन की दीक्षा मानव-समाज को देने का महान कार्य भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट अनेकान्त - दर्शन ने सुलभ किया है। अनेकान्त की दिव्य ध्वनि है-मेरा कथन ही सत्य मात्र नहीं है, सत्य अनन्त है । और वह जहाँ भी कहीं है, जिस किसी भी रूप में है, जिस किस के भी पास है-वह मेरा है, मेरा है। सत्य मेरे लिए समर्पित नहीं है, अपितु मैं सत्य के लिए समर्पित हैं।" मुनिश्री के इस चिन्तन पर लोग यदि ध्यान देंगे, तो समाज - जीवन में शान्ति - प्रेम के वातावरण का निर्माण करना सहज होगा। मनिश्री की पाप-पुण्य की मीमांसा में भी द्रष्टापन की झलक है-"कर्म का कर्ता नरक में और उस कर्म के फल का भोक्ता स्वर्ग में, कितनी विचित्र बौद्धिक विडम्बना है ? रोटी कमाने वाला, बनाने - पकानेवाला पापी है और धर्म के नाम पर मुफ्त में प्राप्त कर खाने वाला पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है।........कर्म और धर्म के बीच में विभाजन की दीवार हमने ऐसी खड़ी कर दी कि कर्म धर्म से शून्य हो गया और धर्म कम से। हर कर्म धर्म है, यदि उसमें जन-हित का व्यापक आयाम है, विवेक दृष्टि है।" एकाध दुर्घटना हुई अर्थात् अनपेक्षित घटना घटी, तो हम कहते हैं-यह कर्म-धर्म संयोग से हुआ । कर्म व धर्म का संयोग यानी दुर्घटना ही है, ऐसा पारम्परिक विचार ही इस शब्द - योजना से ध्वनित होता है। यह बहुधा पाया जाता है कि धर्म करने के दावेदार मात्र कर्तव्य नहीं करते । मुनिजी की दृष्टि में धर्म से युक्त कर्म ही जीवित शक्ति है-"हमें जीवित एवं सप्राण धर्म की आवश्यकता है, प्राणहीन मृत धर्म की नहीं।" यह है उनका इशारा - इंगित । वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कइयों का धर्म श्रवण मात्र के लिए है, वह निरीक्षण के लिए नहीं है, परखने के लिए कतई नहीं है। 'पण्णा समिक्खए धम्म-प्रज्ञा द्वारा धर्म का समीक्षण करना चाहिए-यह भगवान् महावीर का उपदेश पुनः कार्यान्वित हो यही [ आठ ] Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 166