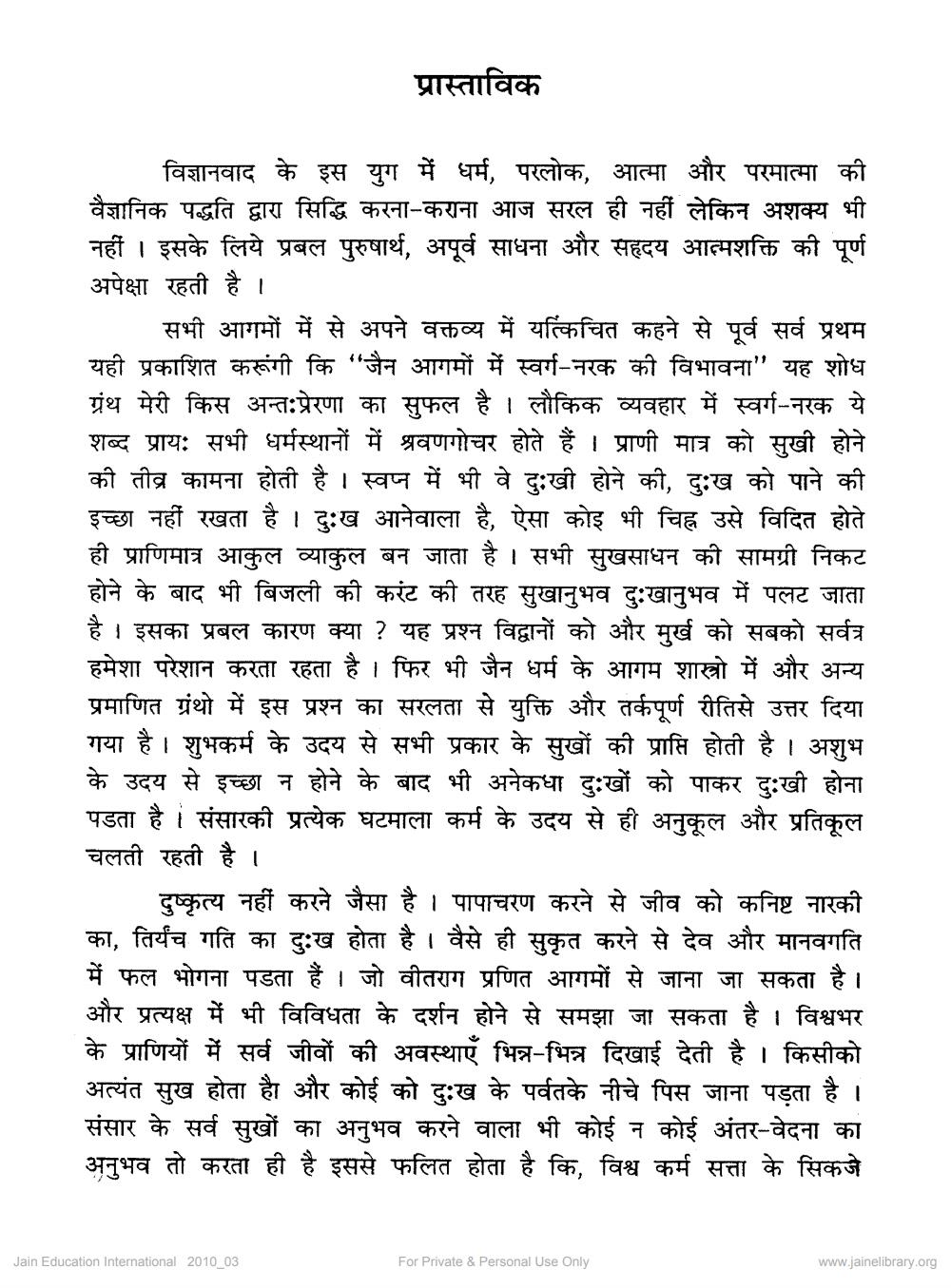Book Title: Jain Agamo me Swarg Narak ki Vibhavana Author(s): Hemrekhashreeji Publisher: Vichakshan Prakashan Trust View full book textPage 6
________________ प्रास्ताविक विज्ञानवाद के इस युग में धर्म, परलोक, आत्मा और परमात्मा की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सिद्धि करना - कराना आज सरल ही नहीं लेकिन अशक्य भी नहीं । इसके लिये प्रबल पुरुषार्थ, अपूर्व साधना और सहृदय आत्मशक्ति की पूर्ण अपेक्षा रहती है । सभी आगमों में से अपने वक्तव्य में यत्किंचित कहने से पूर्व सर्व प्रथम यही प्रकाशित करूंगी कि "जैन आगमों में स्वर्ग-नरक की विभावना" यह शोध ग्रंथ मेरी किस अन्त: प्रेरणा का सुफल है । लौकिक व्यवहार में स्वर्ग-नरक ये शब्द प्रायः सभी धर्मस्थानों में श्रवणगोचर होते हैं । प्राणी मात्र को सुखी होने की तीव्र कामना होती है । स्वप्न में भी वे दुःखी होने की, दुःख को पाने की इच्छा नहीं रखता है । दुःख आनेवाला है, ऐसा कोई भी चिह्न उसे विदित होते ही प्राणिमात्र आकुल व्याकुल बन जाता है । सभी सुखसाधन की सामग्री निकट होने के बाद भी बिजली की करंट की तरह सुखानुभव दुःखानुभव में पलट जाता है । इसका प्रबल कारण क्या ? यह प्रश्न विद्वानों को और मुर्ख को सबको सर्वत्र हमेशा परेशान करता रहता है । फिर भी जैन धर्म के आगम शास्त्रो में और अन्य प्रमाणित ग्रंथों में इस प्रश्न का सरलता से युक्ति और तर्कपूर्ण रीतिसे उत्तर दिया गया है । शुभकर्म के उदय से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है । अशुभ के उदय से इच्छा न होने के बाद भी अनेकधा दुःखों को पाकर दुःखी होना पडता है । संसारकी प्रत्येक घटमाला कर्म के उदय से ही अनुकूल और प्रतिकूल चलती रहती है । दुष्कृत्य नहीं करने जैसा है । पापाचरण करने से जीव को कनिष्ट नारकी का, तिर्यंच गति का दुःख होता है । वैसे ही सुकृत करने से देव और मानवत में फल भोगना पडता हैं । जो वीतराग प्रणित आगमों से जाना जा सकता है । और प्रत्यक्ष में भी विविधता के दर्शन होने से समझा जा सकता है । विश्वभर के प्राणियों में सर्व जीवों की अवस्थाएँ भिन्न-भिन्न दिखाई देती है । किसीको अत्यंत सुख होता है और कोई को दुःख के पर्वतके नीचे पिस जाना पड़ता है । संसार के सर्व सुखों का अनुभव करने वाला भी कोई न कोई अंतर - वेदना का अनुभव तो करता ही है इससे फलित होता है कि, विश्व कर्म सत्ता के सिकजे Jain Education International 2010_03 For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 324