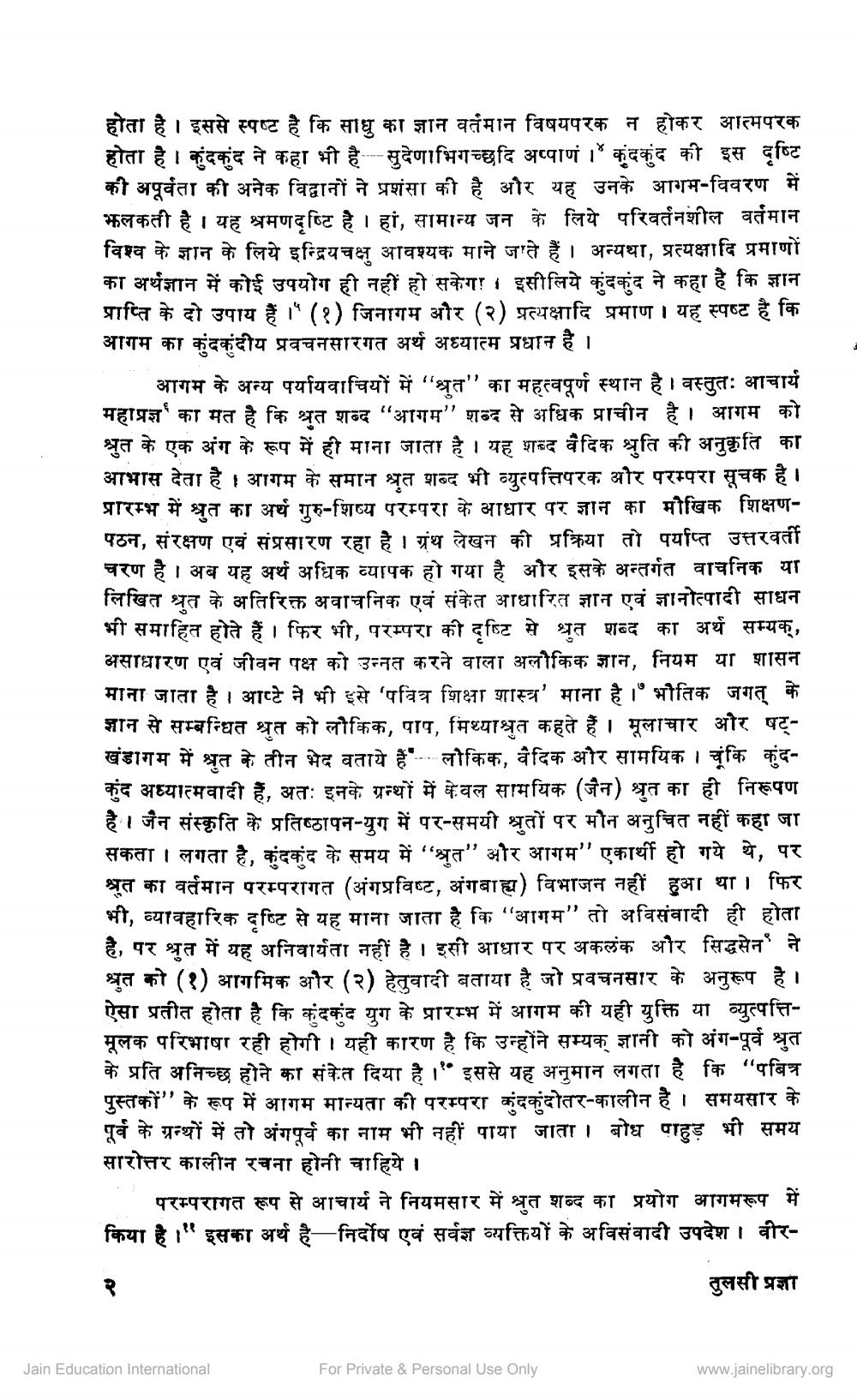Book Title: Tulsi Prajna 1995 04 Author(s): Parmeshwar Solanki Publisher: Jain Vishva Bharati View full book textPage 7
________________ होता है। इससे स्पष्ट है कि साधु का ज्ञान वर्तमान विषयपरक न होकर आत्मपरक होता है। कुंदकुंद ने कहा भी है --सुदेणाभिगच्छदि अप्पाणं ।' कुंदकुंद की इस दृष्टि की अपूर्वता की अनेक विद्वानों ने प्रशंसा की है और यह उनके आगम-विवरण में झलकती है । यह श्रमणदृष्टि है । हां, सामान्य जन के लिये परिवर्तनशील वर्तमान विश्व के ज्ञान के लिये इन्द्रियचक्षु आवश्यक माने जाते हैं। अन्यथा, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अर्थज्ञान में कोई उपयोग ही नहीं हो सकेगा। इसीलिये कुंदकुंद ने कहा है कि ज्ञान प्राप्ति के दो उपाय हैं । (१) जिनागम और (२) प्रत्यक्षादि प्रमाण । यह स्पष्ट है कि आगम का कुंदकुंदीय प्रवचनसारगत अर्थ अध्यात्म प्रधान है । आगम के अन्य पर्यायवाचियों में "श्रुत'' का महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः आचार्य महाप्रज्ञ' का मत है कि श्रुत शब्द "आगम' शब्द से अधिक प्राचीन है। आगम को श्रुत के एक अंग के रूप में ही माना जाता है । यह शब्द वैदिक श्रुति की अनुकृति का आभास देता है । आगम के समान श्रुत शब्द भी व्युत्पत्तिपरक और परम्परा सूचक है। प्रारम्भ में श्रुत का अर्थ गुरु-शिष्य परम्परा के आधार पर ज्ञान का मौखिक शिक्षणपठन, संरक्षण एवं संप्रसारण रहा है । ग्रंथ लेखन की प्रक्रिया तो पर्याप्त उत्तरवर्ती चरण है। अब यह अर्थ अधिक व्यापक हो गया है और इसके अन्तर्गत वाचनिक या लिखित श्रुत के अतिरिक्त अवाचनिक एवं संकेत आधारित ज्ञान एवं ज्ञानोत्पादी साधन भी समाहित होते हैं । फिर भी, परम्परा की दृष्टि से श्रुत शब्द का अर्थ सम्यक्, असाधारण एवं जीवन पक्ष को उन्नत करने वाला अलौकिक ज्ञान, नियम या शासन माना जाता है । आप्टे ने भी इसे 'पवित्र शिक्षा शास्त्र' माना है । भौतिक जगत् के ज्ञान से सम्बन्धित श्रुत को लौकिक, पाप, मिथ्याश्रुत कहते हैं । मूलाचार और षट्खंडागम में श्रुत के तीन भेद बताये हैं। लौकिक, वैदिक और सामयिक । चूंकि कुंदकुंद अध्यात्मवादी हैं, अतः इनके ग्रन्थों में केवल सामयिक (जैन) श्रुत का ही निरूपण है । जैन संस्कृति के प्रतिष्ठापन-युग में पर-समयी श्रुतों पर मौन अनुचित नहीं कहा जा सकता । लगता है, कुंदकुंद के समय में "श्रुत" और आगम'' एकार्थी हो गये थे, पर श्रुत का वर्तमान परम्परागत (अंगप्रविष्ट, अंगबाह्य) विभाजन नहीं हुआ था। फिर भी, व्यावहारिक दृष्टि से यह माना जाता है कि "आगम' तो अविसंवादी ही होता है, पर श्रुत में यह अनिवार्यता नहीं है । इसी आधार पर अकलंक और सिद्धसेन ने श्रुत को (१) आगमिक और (२) हेतुवादी बताया है जो प्रवचनसार के अनुरूप है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुंदकुंद युग के प्रारम्भ में आगम की यही युक्ति या व्युत्पत्तिमूलक परिभाषा रही होगी। यही कारण है कि उन्होंने सम्यक् ज्ञानी को अंग-पूर्व श्रुत के प्रति अनिच्छ होने का संकेत दिया है। इससे यह अनुमान लगता है कि "पबित्र पुस्तकों" के रूप में आगम मान्यता की परम्परा कुंदकुंदोतर-कालीन है । समयसार के पूर्व के ग्रन्थों में तो अंगपूर्व का नाम भी नहीं पाया जाता। बोध पाहुड़ भी समय सारोत्तर कालीन रचना होनी चाहिये । परम्परागत रूप से आचार्य ने नियमसार में श्रुत शब्द का प्रयोग आगमरूप में किया है। इसका अर्थ है–निर्दोष एवं सर्वज्ञ व्यक्तियों के अविसंवादी उपदेश । वीर तुलसी प्रज्ञा Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 158