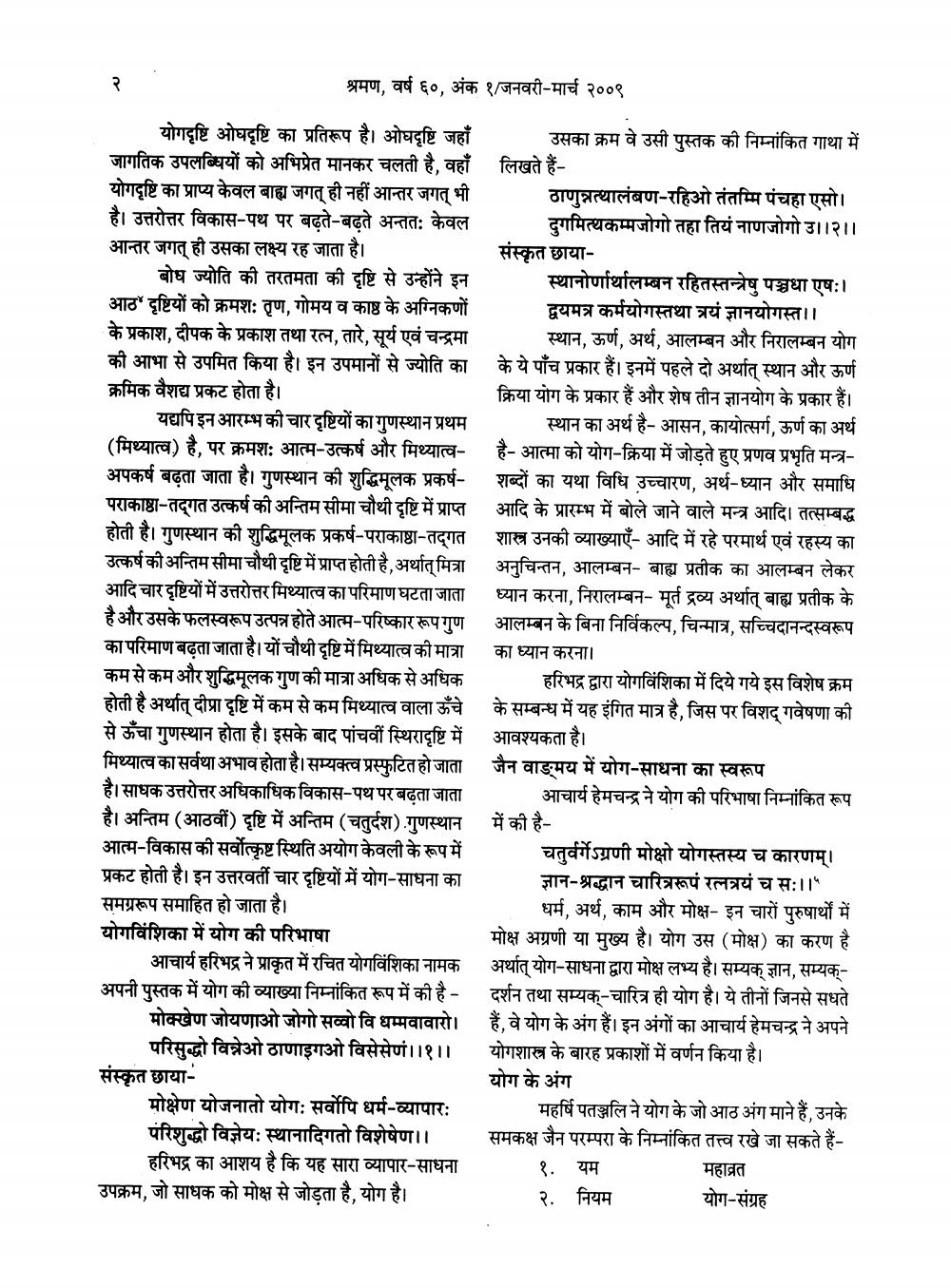Book Title: Sramana 2009 01 Author(s): Shreeprakash Pandey, Vijay Kumar Publisher: Parshvanath Vidhyashram Varanasi View full book textPage 7
________________ २ श्रमण, वर्ष ६०, अंक १ / जनवरी-मार्च २००९ योगदृष्टि ओघदृष्टि का प्रतिरूप है। ओघदृष्टि जहाँ जागतिक उपलब्धियों को अभिप्रेत मानकर चलती है, वहाँ योगदृष्टि का प्राप्य केवल बाह्य जगत् ही नहीं आन्तर जगत् भी है । उत्तरोत्तर विकास पथ पर बढ़ते-बढ़ते अन्ततः केवल आन्तर जगत् ही उसका लक्ष्य रह जाता है। बोध ज्योति की तरतमता की दृष्टि से उन्होंने इन आठ दृष्टियों को क्रमशः तृण, गोमय व काष्ठ के अग्निकणों के प्रकाश, दीपक के प्रकाश तथा रत्न, तारे, सूर्य एवं चन्द्रमा की आभा से उपमित किया है। इन उपमानों से ज्योति का क्रमिक वैशद्य प्रकट होता है। यद्यपि इन आरम्भ की चार दृष्टियों का गुणस्थान प्रथम (मिथ्यात्व) है, पर क्रमशः आत्म - उत्कर्ष और मिथ्यात्व अपकर्ष बढ़ता जाता है। गुणस्थान की शुद्धिमूलक प्रकर्षपराकाष्ठा-तद्गत उत्कर्ष की अन्तिम सीमा चौथी दृष्टि में प्राप्त होती है। गुणस्थान की शुद्धिमूलक प्रकर्ष- पराकाष्ठा - तद्गत उत्कर्ष की अन्तिम सीमा चौथी दृष्टि में प्राप्त होती है, अर्थात् मित्रा आदि चार दृष्टियों में उत्तरोत्तर मिथ्यात्व का परिमाण घटता जाता है और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होते आत्म-परिष्कार रूप गुण का परिमाण बढ़ता जाता है। यों चौथी दृष्टि में मिथ्यात्व की मात्रा कम से कम और शुद्धिमूलक गुण की मात्रा अधिक से अधिक होती है अर्थात् दीप्रा दृष्टि में कम से कम मिथ्यात्व वाला ऊँचे से ऊँचा गुणस्थान होता है। इसके बाद पांचवीं स्थिरादृष्टि में मिथ्यात्व का सर्वथा अभाव होता है। सम्यक्त्व प्रस्फुटित हो जाता है। साधक उत्तरोत्तर अधिकाधिक विकास पथ पर बढ़ता जाता है। अन्तिम (आठवीं) दृष्टि में अन्तिम ( चतुर्दश) गुणस्थान आत्म-विकास की सर्वोत्कृष्ट स्थिति अयोग केवली के रूप में प्रकट होती है। इन उत्तरवर्ती चार दृष्टियों में योग-साधना का समग्ररूप समाहित हो जाता है। योगविंशिका में योग की परिभाषा आचार्य हरिभद्र ने प्राकृत में रचित योगविंशिका नामक अपनी पुस्तक में योग की व्याख्या निम्नांकित रूप में की है - मोक्खेण जोयणाओ जोगो सव्वो वि धम्मवावारो । परिसुद्धो विन्नेओ ठाणाइगओ विसेसेणं । । १ । । संस्कृत छाया मोक्षेण योजनातो योग: सर्वोपि धर्म - व्यापारः परिशुद्ध विज्ञेयः स्थानादिगतो विशेषेण ।। हरिभद्र का आशय है कि यह सारा व्यापार - साधना उपक्रम, जो साधक को मोक्ष से जोड़ता है, योग है। उसका क्रम वे उसी पुस्तक की निम्नांकित गाथा में लिखते हैं ठाणुन्नत्थालंबण-रहिओ तंतम्मि पंचहा एसो । दुगमित्थकम्मजोगो तहा तियं नाणजोगो उ । । २ । । संस्कृत छाया स्थानोर्णार्थालम्बन रहितस्तन्त्रेषु पञ्चधा एषः । द्वयमत्र कर्मयोगस्तथा त्रयं ज्ञानयोगस्त । । स्थान, ऊर्ण, अर्थ, आलम्बन और निरालम्बन योग के ये पाँच प्रकार हैं। इनमें पहले दो अर्थात् स्थान और ऊर्ण क्रिया योग के प्रकार हैं और शेष तीन ज्ञानयोग के प्रकार हैं। स्थान का अर्थ है- आसन, कायोत्सर्ग, ऊर्ण का अर्थ है- आत्मा को योग क्रिया में जोड़ते हुए प्रणव प्रभृति मन्त्रशब्दों का यथा विधि उच्चारण, अर्थ-ध्यान और समाधि आदि के प्रारम्भ में बोले जाने वाले मन्त्र आदि । तत्सम्बद्ध शास्त्र उनकी व्याख्याएँ- आदि में रहे परमार्थ एवं रहस्य का अनुचिन्तन, आलम्बन- बाह्य प्रतीक का आलम्बन लेकर ध्यान करना, निरालम्बन- मूर्त द्रव्य अर्थात् बाह्य प्रतीक के आलम्बन के बिना निर्विकल्प, चिन्मात्र, सच्चिदानन्दस्वरूप का ध्यान करना। हरिभद्र द्वारा योगविंशिका में दिये गये इस विशेष क्रम सम्बन्ध में यह इंगित मात्र है, जिस पर विशद् गवेषणा की आवश्यकता है। जैन वाङ्मय में योग-साधना का स्वरूप आचार्य हेमचन्द्र ने योग की परिभाषा निम्नांकित रूप में की है चतुर्वर्गेऽग्रणी मोक्षो योगस्तस्य च कारणम् । ज्ञान- श्रद्धान चारित्ररूपं रत्नत्रयं च सः । । ५ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष अग्रणी या मुख्य है। योग उस (मोक्ष) का करण है अर्थात् योग-साधना द्वारा मोक्ष लभ्य है। सम्यक् ज्ञान, सम्यक्दर्शन तथा सम्यक् चारित्र ही योग है। ये तीनों जिनसे सधते हैं, वे योग के अंग हैं। इन अंगों का आचार्य हेमचन्द्र ने अपने योगशास्त्र के बारह प्रकाशों में वर्णन किया है। योग के अंग महर्षि पतञ्जलि ने योग के जो आठ अंग माने हैं, उनके समकक्ष जैन परम्परा के निम्नांकित तत्त्व रखे जा सकते हैं१. महाव्रत २. नियम योग-संग्रह यमPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 100