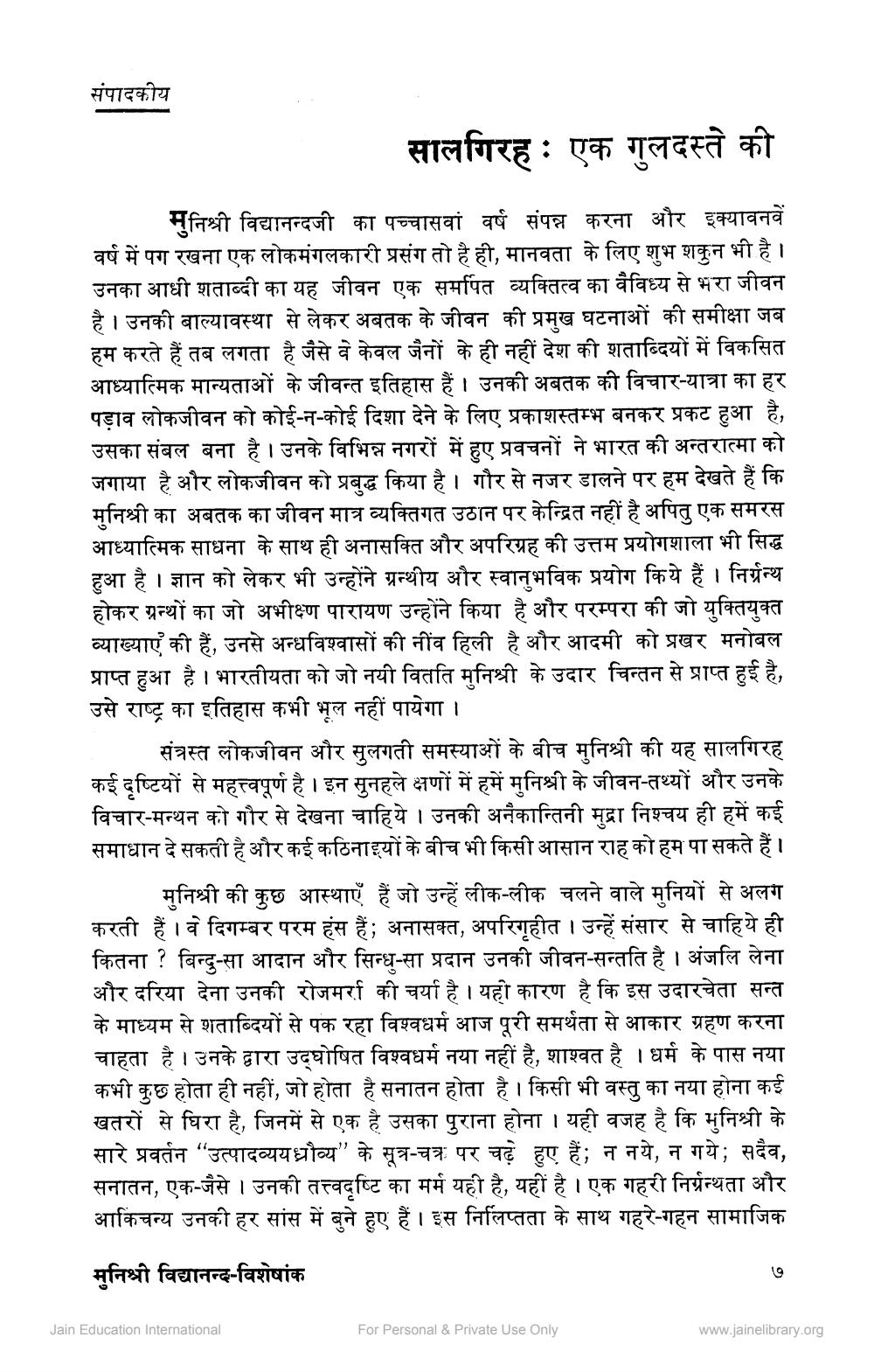Book Title: Tirthankar 1974 04 Author(s): Nemichand Jain Publisher: Hira Bhaiyya Prakashan Indore View full book textPage 6
________________ संपादकीय सालगिरह : एक गुलदस्ते की मुनिश्री विद्यानन्दजी का पच्चासवां वर्ष संपन्न करना और इक्यावनवें वर्ष में पग रखना एक लोकमंगलकारी प्रसंग तो है ही, मानवता के लिए शुभ शकुन भी है। उनका आधी शताब्दी का यह जीवन एक समर्पित व्यक्तित्व का वैविध्य से भरा जीवन है। उनकी बाल्यावस्था से लेकर अबतक के जीवन की प्रमुख घटनाओं की समीक्षा जब हम करते हैं तब लगता है जैसे वे केवल जैनों के ही नहीं देश की शताब्दियों में विकसित आध्यात्मिक मान्यताओं के जीवन्त इतिहास हैं। उनकी अबतक की विचार-यात्रा का हर पड़ाव लोकजीवन को कोई-न-कोई दिशा देने के लिए प्रकाशस्तम्भ बनकर प्रकट हुआ है, उसका संबल बना है। उनके विभिन्न नगरों में हुए प्रवचनों ने भारत की अन्तरात्मा को जगाया है और लोकजीवन को प्रबुद्ध किया है। गौर से नजर डालने पर हम देखते हैं कि मुनिश्री का अबतक का जीवन मात्र व्यक्तिगत उठान पर केन्द्रित नहीं है अपितु एक समरस आध्यात्मिक साधना के साथ ही अनासक्ति और अपरिग्रह की उत्तम प्रयोगशाला भी सिद्ध हुआ है । ज्ञान को लेकर भी उन्होंने ग्रन्थीय और स्वानुभविक प्रयोग किये हैं । निर्ग्रन्थ होकर ग्रन्थों का जो अभीक्ष्ण पारायण उन्होंने किया है और परम्परा की जो युक्तियुक्त व्याख्याएं की हैं, उनसे अन्धविश्वासों की नींव हिली है और आदमी को प्रखर मनोबल प्राप्त हुआ है। भारतीयता को जो नयी वितति मुनिश्री के उदार चिन्तन से प्राप्त हुई है, उसे राष्ट्र का इतिहास कभी भूल नहीं पायेगा। संत्रस्त लोकजीवन और सुलगती समस्याओं के बीच मुनिश्री की यह सालगिरह कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । इन सुनहले क्षणों में हमें मुनिश्री के जीवन-तथ्यों और उनके विचार-मन्थन को गौर से देखना चाहिये । उनकी अनैकान्तिनी मुद्रा निश्चय ही हमें कई समाधान दे सकती है और कई कठिनाइयों के बीच भी किसी आसान राह को हम पा सकते हैं। मनिश्री की कुछ आस्थाएँ हैं जो उन्हें लीक-लीक चलने वाले मनियों से अलग करती हैं । वे दिगम्बर परम हंस हैं; अनासक्त, अपरिगृहीत । उन्हें संसार से चाहिये ही कितना ? बिन्दु-सा आदान और सिन्धु-सा प्रदान उनकी जीवन-सन्तति है । अंजलि लेना और दरिया देना उनकी रोजमर्रा की चर्या है । यही कारण है कि इस उदारचेता सन्त के माध्यम से शताब्दियों से पक रहा विश्वधर्म आज पूरी समर्थता से आकार ग्रहण करना चाहता है। उनके द्वारा उद्घोषित विश्वधर्म नया नहीं है, शाश्वत है । धर्म के पास नया कभी कुछ होता ही नहीं, जो होता है सनातन होता है। किसी भी वस्तु का नया होना कई खतरों से घिरा है, जिनमें से एक है उसका पुराना होना । यही वजह है कि मुनिश्री के सारे प्रवर्तन "उत्पादव्ययध्रौव्य' के सूत्र-चत्र पर चढ़े हुए हैं; न नये, न गये; सदैव, सनातन, एक-जैसे । उनकी तत्त्वदृष्टि का मर्म यही है, यहीं है । एक गहरी निर्ग्रन्थता और आकिंचन्य उनकी हर सांस में बुने हुए हैं । इस निर्लिप्तता के साथ गहरे-गहन सामाजिक मुनिश्री विद्यानन्द-विशेषांक Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 230