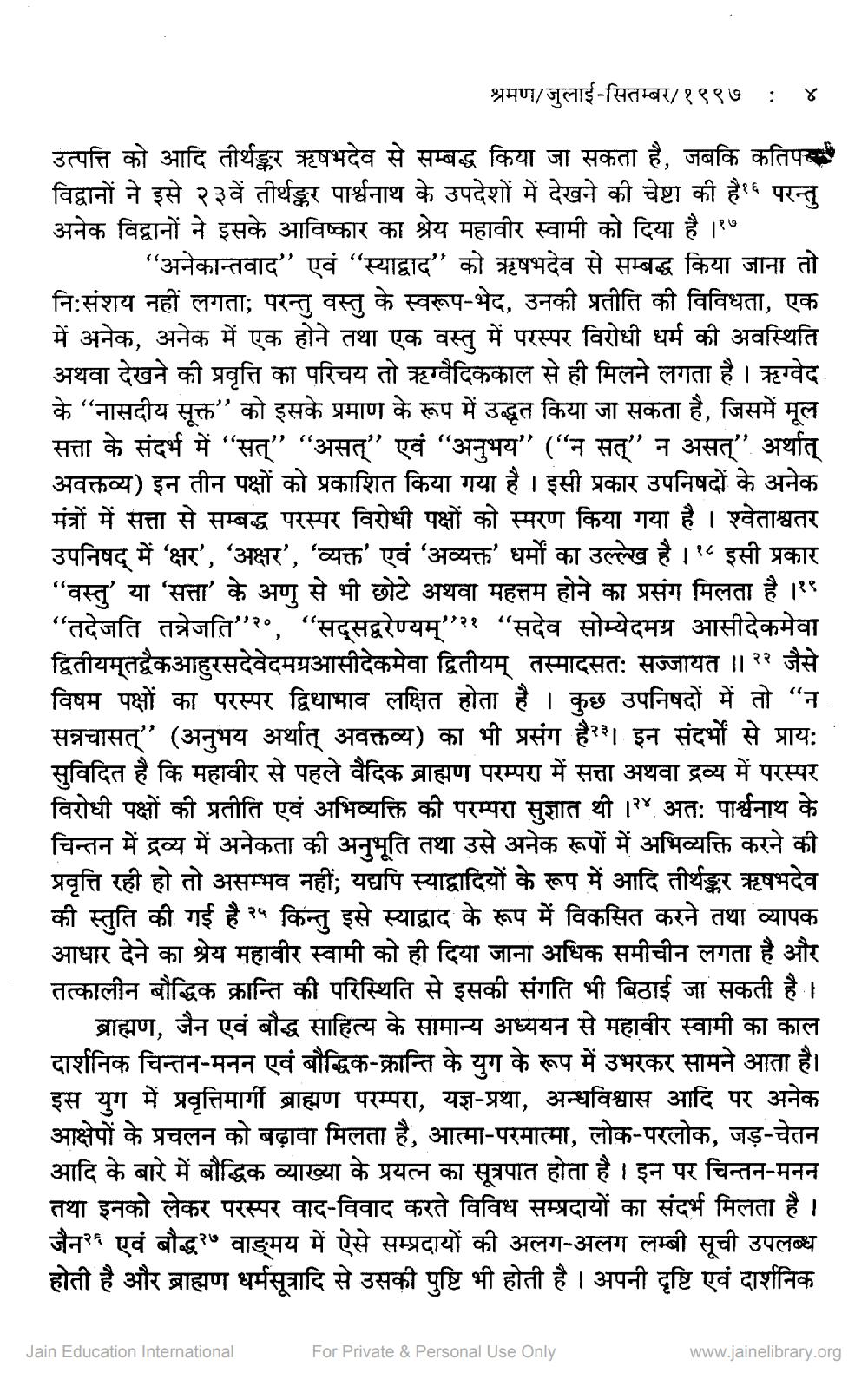Book Title: Sramana 1997 07 Author(s): Ashok Kumar Singh Publisher: Parshvanath Vidhyashram Varanasi View full book textPage 7
________________ श्रमण/जुलाई-सितम्बर/१९९७ : ४ उत्पत्ति को आदि तीर्थङ्कर ऋषभदेव से सम्बद्ध किया जा सकता है, जबकि कतिपय विद्वानों ने इसे २३वें तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ के उपदेशों में देखने की चेष्टा की है१६ परन्तु अनेक विद्वानों ने इसके आविष्कार का श्रेय महावीर स्वामी को दिया है ।१७ “अनेकान्तवाद' एवं “स्याद्वाद" को ऋषभदेव से सम्बद्ध किया जाना तो नि:संशय नहीं लगता; परन्तु वस्तु के स्वरूप-भेद, उनकी प्रतीति की विविधता, एक में अनेक, अनेक में एक होने तथा एक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म की अवस्थिति अथवा देखने की प्रवृत्ति का परिचय तो ऋग्वैदिककाल से ही मिलने लगता है । ऋग्वेद के “नासदीय सूक्त” को इसके प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है, जिसमें मूल सत्ता के संदर्भ में "सत्" "असत्" एवं "अनुभय" ("न सत्" न असत्" अर्थात् अवक्तव्य) इन तीन पक्षों को प्रकाशित किया गया है । इसी प्रकार उपनिषदों के अनेक मंत्रों में सत्ता से सम्बद्ध परस्पर विरोधी पक्षों को स्मरण किया गया है । श्वेताश्वतर उपनिषद् में 'क्षर', 'अक्षर', 'व्यक्त' एवं 'अव्यक्त' धर्मों का उल्लेख है । १८ इसी प्रकार "वस्तु' या 'सत्ता' के अणु से भी छोटे अथवा महत्तम होने का प्रसंग मिलता है ।१९ "तदेजति तनेजति" २०, “सद्सद्वरेण्यम्"२१ “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्तद्वैकआहरसदेवेदमग्रआसीदेकमेवा द्वितीयम् तस्मादसत: सज्जायत ।। २२ जैसे विषम पक्षों का परस्पर द्विधाभाव लक्षित होता है । कुछ उपनिषदों में तो "न सनचासत्” (अनुभय अर्थात् अवक्तव्य) का भी प्रसंग है२२। इन संदर्भो से प्रायः सुविदित है कि महावीर से पहले वैदिक ब्राह्मण परम्परा में सत्ता अथवा द्रव्य में परस्पर विरोधी पक्षों की प्रतीति एवं अभिव्यक्ति की परम्परा सुज्ञात थी ।२४ अत: पार्श्वनाथ के चिन्तन में द्रव्य में अनेकता की अनुभूति तथा उसे अनेक रूपों में अभिव्यक्ति करने की प्रवृत्ति रही हो तो असम्भव नहीं; यद्यपि स्याद्वादियों के रूप में आदि तीर्थङ्कर ऋषभदेव की स्तुति की गई है २५ किन्तु इसे स्याद्वाद के रूप में विकसित करने तथा व्यापक आधार देने का श्रेय महावीर स्वामी को ही दिया जाना अधिक समीचीन लगता है और तत्कालीन बौद्धिक क्रान्ति की परिस्थिति से इसकी संगति भी बिठाई जा सकती है। ब्राह्मण, जैन एवं बौद्ध साहित्य के सामान्य अध्ययन से महावीर स्वामी का काल दार्शनिक चिन्तन-मनन एवं बौद्धिक-क्रान्ति के युग के रूप में उभरकर सामने आता है। इस युग में प्रवृत्तिमार्गी ब्राह्मण परम्परा, यज्ञ-प्रथा, अन्धविश्वास आदि पर अनेक आक्षेपों के प्रचलन को बढ़ावा मिलता है, आत्मा-परमात्मा, लोक-परलोक, जड़-चेतन आदि के बारे में बौद्धिक व्याख्या के प्रयत्न का सूत्रपात होता है। इन पर चिन्तन-मनन तथा इनको लेकर परस्पर वाद-विवाद करते विविध सम्प्रदायों का संदर्भ मिलता है । जैन२६ एवं बौद्ध वाङ्मय में ऐसे सम्प्रदायों की अलग-अलग लम्बी सूची उपलब्ध होती है और ब्राह्मण धर्मसूत्रादि से उसकी पुष्टि भी होती है । अपनी दृष्टि एवं दार्शनिक Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 144