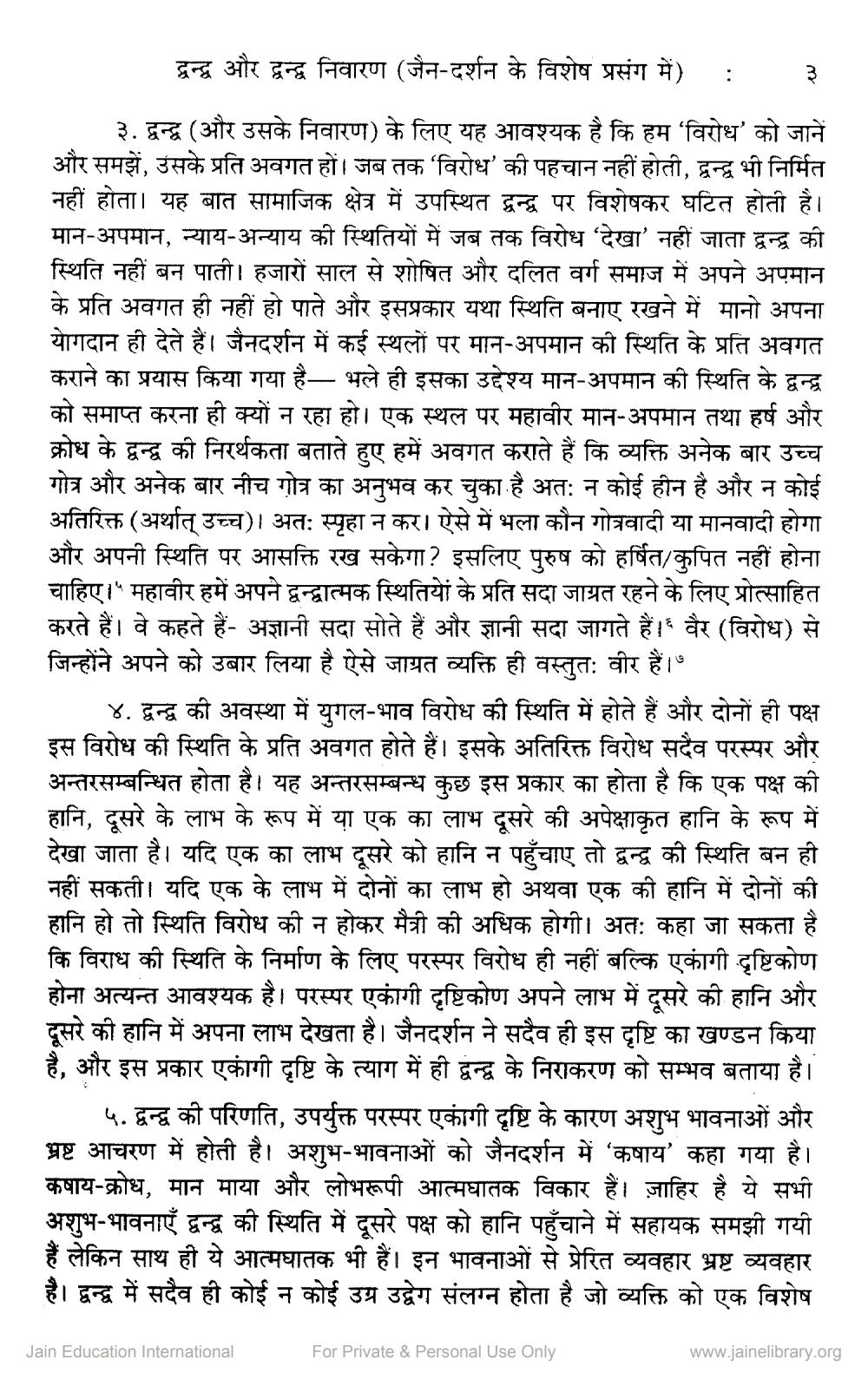Book Title: Sramana 1996 10 Author(s): Ashok Kumar Singh Publisher: Parshvanath Vidhyashram Varanasi View full book textPage 6
________________ द्वन्द्व और द्वन्द्व निवारण (जैन दर्शन के विशेष प्रसंग में) : ३. द्वन्द्व (और उसके निवारण) के लिए यह आवश्यक है कि हम 'विरोध' को जानें और समझें, उसके प्रति अवगत हों। जब तक 'विरोध' की पहचान नहीं होती, द्वन्द्व भी निर्मित नहीं होता। यह बात सामाजिक क्षेत्र में उपस्थित द्वन्द्व पर विशेषकर घटित होती है। मान-अपमान, न्याय-अन्याय की स्थितियों में जब तक विरोध 'देखा' नहीं जाता द्वन्द्व की स्थिति नहीं बन पाती। हजारों साल से शोषित और दलित वर्ग समाज में अपने अपमान के प्रति अवगत ही नहीं हो पाते और इसप्रकार यथा स्थिति बनाए रखने में मानो अपना योगदान ही देते हैं । जैनदर्शन में कई स्थलों पर मान-अपमान की स्थिति के प्रति अवगत कराने का प्रयास किया गया है- भले ही इसका उद्देश्य मान-अपमान की स्थिति के द्वन्द्व को समाप्त करना ही क्यों न रहा हो। एक स्थल पर महावीर मान-अपमान तथा हर्ष और क्रोध के द्वन्द्व की निरर्थकता बताते हुए हमें अवगत कराते हैं कि व्यक्ति अनेक बार उच्च गोत्र और अनेक बार नीच गोत्र का अनुभव कर चुका है अतः न कोई हीन है और न कोई अतिरिक्त (अर्थात् उच्च) । अतः स्पृहा न कर। ऐसे में भला कौन गोत्रवादी या मानवादी होगा और अपनी स्थिति पर आसक्ति रख सकेगा? इसलिए पुरुष को हर्षित / कुपित नहीं होना चाहिए।' महावीर हमें अपने द्वन्द्वात्मक स्थितियों के प्रति सदा जाग्रत रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं- अज्ञानी सदा सोते हैं और ज्ञानी सदा जागते हैं । ६ वैर (विरोध) से जिन्होंने अपने को उबार लिया है ऐसे जाग्रत व्यक्ति ही वस्तुतः वीर हैं । ७ ४. द्वन्द्व की अवस्था में युगल - भाव विरोध की स्थिति में होते हैं और दोनों ही पक्ष इस विरोध की स्थिति के प्रति अवगत होते हैं। इसके अतिरिक्त विरोध सदैव परस्पर और अन्तरसम्बन्धित होता है । यह अन्तरसम्बन्ध कुछ इस प्रकार का होता है कि एक पक्ष की हानि, दूसरे के लाभ के रूप में या एक का लाभ दूसरे की अपेक्षाकृत हानि के रूप में देखा जाता है। यदि एक का लाभ दूसरे को हानि न पहुँचाए तो द्वन्द्व की स्थिति बन ही नहीं सकती। यदि एक के लाभ में दोनों का लाभ हो अथवा एक की हानि में दोनों की हानि हो तो स्थिति विरोध की न होकर मैत्री की अधिक होगी। अतः कहा जा सकता है। कि विराध की स्थिति के निर्माण के लिए परस्पर विरोध ही नहीं बल्कि एकांगी दृष्टिकोण होना अत्यन्त आवश्यक है । परस्पर एकांगी दृष्टिकोण अपने लाभ में दूसरे की हानि और दूसरे की हानि में अपना लाभ देखता है। जैनदर्शन ने सदैव ही इस दृष्टि का खण्डन किया है, और इस प्रकार एकांगी दृष्टि के त्याग में ही द्वन्द्व के निराकरण को सम्भव बताया है। ५. द्वन्द्व की परिणति, उपर्युक्त परस्पर एकांगी दृष्टि के कारण अशुभ भावनाओं और भ्रष्ट आचरण में होती है। अशुभ भावनाओं को जैनदर्शन में 'कषाय' कहा गया है। कषाय-क्रोध, मान माया और लोभरूपी आत्मघातक विकार हैं। ज़ाहिर है ये सभी अशुभ-भावनाएँ द्वन्द्व की स्थिति में दूसरे पक्ष को हानि पहुँचाने में सहायक समझी गयी हैं लेकिन साथ ही ये आत्मघातक भी हैं। इन भावनाओं से प्रेरित व्यवहार भ्रष्ट व्यवहार है । द्वन्द्व में सदैव ही कोई न कोई उग्र उद्वेग संलग्न होता है जो व्यक्ति को एक विशेष Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 128