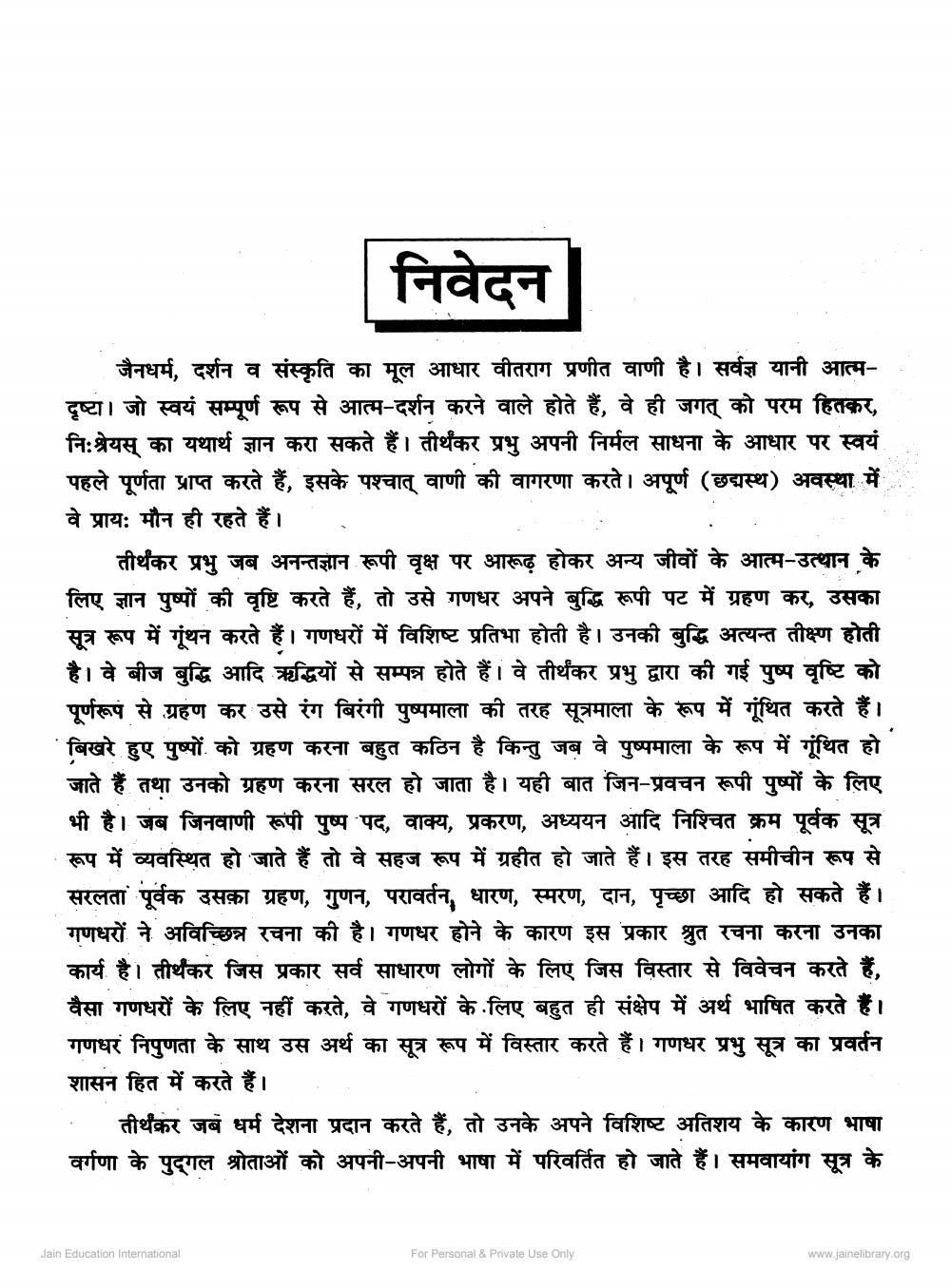Book Title: Nandi Sutra Author(s): Parasmuni Publisher: Akhil Bharatiya Sudharm Jain Sanskruti Rakshak Sangh View full book textPage 6
________________ निवेदन जैनधर्म, दर्शन व संस्कृति का मूल आधार वीतराग प्रणीत वाणी है। सर्वज्ञ यानी आत्मदृष्टा। जो स्वयं सम्पूर्ण रूप से आत्म-दर्शन करने वाले होते हैं, वे ही जगत् को परम हितकर, निःश्रेयस् का यथार्थ ज्ञान करा सकते हैं। तीर्थंकर प्रभु अपनी निर्मल साधना के आधार पर स्वयं पहले पूर्णता प्राप्त करते हैं, इसके पश्चात् वाणी की वागरणा करते। अपूर्ण (छद्मस्थ) अवस्था में वे प्रायः मौन ही रहते हैं। . तीर्थकर प्रभु जब अनन्तज्ञान रूपी वृक्ष पर आरूढ़ होकर अन्य जीवों के आत्म-उत्थान के लिए ज्ञान पुष्पों की वृष्टि करते हैं, तो उसे गणधर अपने बुद्धि रूपी पट में ग्रहण कर, उसका सूत्र रूप में गूंथन करते हैं। गणधरों में विशिष्ट प्रतिभा होती है। उनकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण होती है। वे बीज बुद्धि आदि ऋद्धियों से सम्पन्न होते हैं। वे तीर्थंकर प्रभु द्वारा की गई पुष्प वृष्टि को पूर्णरूप से ग्रहण कर उसे रंग बिरंगी पुष्पमाला की तरह सूत्रमाला के रूप में गूंथित करते हैं। बिखरे हुए पुष्पों को ग्रहण करना बहुत कठिन है किन्तु जब वे पुष्पमाला के रूप में गूंथित हो जाते हैं तथा उनको ग्रहण करना सरल हो जाता है। यही बात जिन-प्रवचन रूपी पुष्पों के लिए भी है। जब जिनवाणी रूपी पुष्प पद, वाक्य, प्रकरण, अध्ययन आदि निश्चित क्रम पूर्वक सूत्र रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं तो वे सहज रूप में ग्रहीत हो जाते हैं। इस तरह समीचीन रूप से सरलता पूर्वक उसका ग्रहण, गुणन, परावर्तन, धारण, स्मरण, दान, पृच्छा आदि हो सकते हैं। गणधरों ने अविच्छिन्न रचना की है। गणधर होने के कारण इस प्रकार श्रुत रचना करना उनका कार्य है। तीर्थकर जिस प्रकार सर्व साधारण लोगों के लिए जिस विस्तार से विवेचन करते हैं, वैसा गणधरों के लिए नहीं करते, वे गणधरों के लिए बहुत ही संक्षेप में अर्थ भाषित करते हैं। गणधरं निपुणता के साथ उस अर्थ का सूत्र रूप में विस्तार करते हैं। गणधर प्रभु सूत्र का प्रवर्तन शासन हित में करते हैं। तीर्थकर जब धर्म देशना प्रदान करते हैं, तो उनके अपने विशिष्ट अतिशय के कारण भाषा वर्गणा के पुद्गल श्रोताओं को अपनी-अपनी भाषा में परिवर्तित हो जाते हैं। समवायांग सूत्र के Jain Education International For Personal & Private Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 314