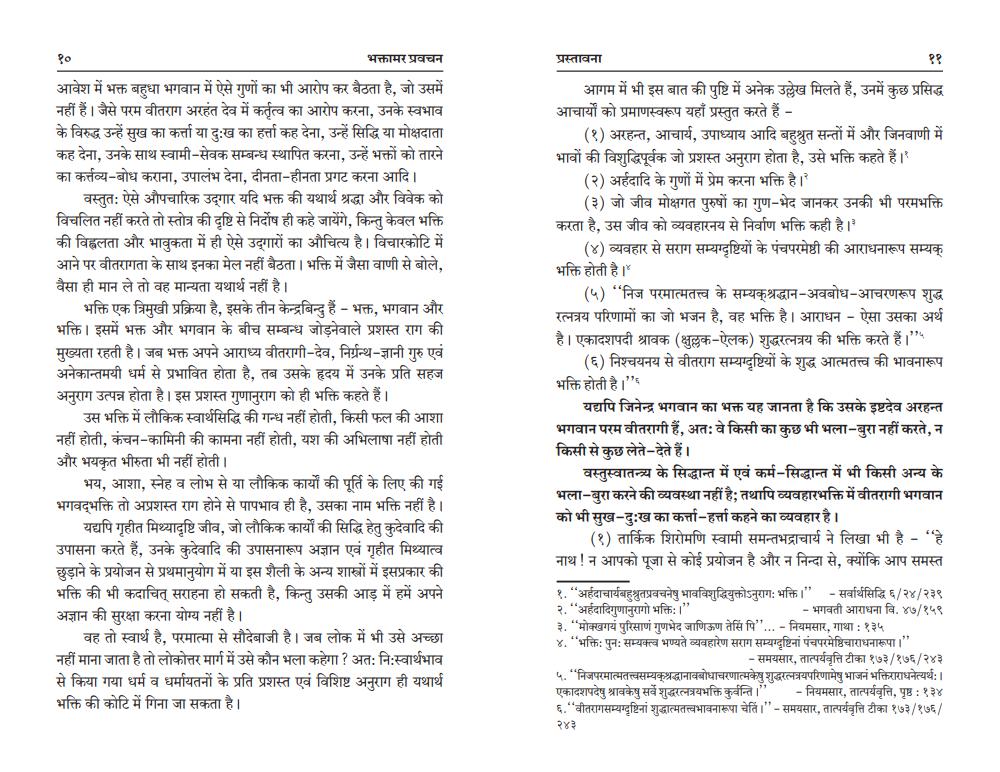Book Title: Bhaktamara Pravachan Author(s): Ratanchand Bharilla Publisher: Todarmal Granthamala Jaipur View full book textPage 6
________________ भक्तामर प्रवचन प्रस्तावना आवेश में भक्त बहुधा भगवान में ऐसे गुणों का भी आरोप कर बैठता है, जो उसमें नहीं हैं। जैसे परम वीतराग अरहंत देव में कर्तृत्व का आरोप करना, उनके स्वभाव के विरुद्ध उन्हें सुख का कर्ता या दुःख का हर्ता कह देना, उन्हें सिद्धि या मोक्षदाता कह देना, उनके साथ स्वामी-सेवक सम्बन्ध स्थापित करना, उन्हें भक्तों को तारने का कर्त्तव्य-बोध कराना, उपालंभ देना, दीनता-हीनता प्रगट करना आदि। वस्तुतः ऐसे औपचारिक उद्गार यदि भक्त की यथार्थ श्रद्धा और विवेक को विचलित नहीं करते तो स्तोत्र की दृष्टि से निर्दोष ही कहे जायेंगे, किन्तु केवल भक्ति की विह्वलता और भावुकता में ही ऐसे उद्गारों का औचित्य है। विचारकोटि में आने पर वीतरागता के साथ इनका मेल नहीं बैठता। भक्ति में जैसा वाणी से बोले, वैसा ही मान ले तो वह मान्यता यथार्थ नहीं है। भक्ति एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसके तीन केन्द्रबिन्दु हैं - भक्त, भगवान और भक्ति। इसमें भक्त और भगवान के बीच सम्बन्ध जोड़नेवाले प्रशस्त राग की मुख्यता रहती है। जब भक्त अपने आराध्य वीतरागी-देव, निर्ग्रन्थ-ज्ञानी गुरु एवं अनेकान्तमयी धर्म से प्रभावित होता है, तब उसके हृदय में उनके प्रति सहज अनुराग उत्पन्न होता है। इस प्रशस्त गुणानुराग को ही भक्ति कहते हैं। उस भक्ति में लौकिक स्वार्थसिद्धि की गन्ध नहीं होती, किसी फल की आशा नहीं होती, कंचन-कामिनी की कामना नहीं होती, यश की अभिलाषा नहीं होती और भयकृत भीरुता भी नहीं होती। भय, आशा, स्नेह व लोभ से या लौकिक कार्यों की पूर्ति के लिए की गई भगवद्भक्ति तो अप्रशस्त राग होने से पापभाव ही है, उसका नाम भक्ति नहीं है। यद्यपि गृहीत मिथ्यादृष्टि जीव, जो लौकिक कार्यों की सिद्धि हेतु कुदेवादि की उपासना करते हैं, उनके कुदेवादि की उपासनारूप अज्ञान एवं गृहीत मिथ्यात्व छुड़ाने के प्रयोजन से प्रथमानुयोग में या इस शैली के अन्य शास्त्रों में इसप्रकार की भक्ति की भी कदाचित् सराहना हो सकती है, किन्तु उसकी आड़ में हमें अपने अज्ञान की सुरक्षा करना योग्य नहीं है। वह तो स्वार्थ है, परमात्मा से सौदेबाजी है। जब लोक में भी उसे अच्छा नहीं माना जाता है तो लोकोत्तर मार्ग में उसे कौन भला कहेगा? अत: नि:स्वार्थभाव से किया गया धर्म व धर्मायतनों के प्रति प्रशस्त एवं विशिष्ट अनुराग ही यथार्थ भक्ति की कोटि में गिना जा सकता है। आगम में भी इस बात की पुष्टि में अनेक उल्लेख मिलते हैं, उनमें कुछ प्रसिद्ध आचार्यों को प्रमाणस्वरूप यहाँ प्रस्तुत करते हैं - (१) अरहन्त, आचार्य, उपाध्याय आदि बहुश्रुत सन्तों में और जिनवाणी में भावों की विशुद्धिपूर्वक जो प्रशस्त अनुराग होता है, उसे भक्ति कहते हैं।' (२) अर्हदादि के गुणों में प्रेम करना भक्ति है।' (३) जो जीव मोक्षगत पुरुषों का गुण-भेद जानकर उनकी भी परमभक्ति करता है, उस जीव को व्यवहारनय से निर्वाण भक्ति कही है।' (४) व्यवहार से सराग सम्यग्दृष्टियों के पंचपरमेष्ठी की आराधनारूप सम्यक् भक्ति होती है। (५) “निज परमात्मतत्त्व के सम्यक्श्रद्धान-अवबोध-आचरणरूप शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन है, वह भक्ति है। आराधन - ऐसा उसका अर्थ है। एकादशपदी श्रावक (क्षुल्लक-ऐलक) शुद्धरत्नत्रय की भक्ति करते हैं।"५ (६) निश्चयनय से वीतराग सम्यग्दृष्टियों के शुद्ध आत्मतत्त्व की भावनारूप भक्ति होती है।" यद्यपि जिनेन्द्र भगवान का भक्त यह जानता है कि उसके इष्टदेव अरहन्त भगवान परम वीतरागी हैं, अत: वे किसी का कुछ भी भला-बुरा नहीं करते, न किसी से कुछ लेते-देते हैं। वस्तुस्वातन्त्र्य के सिद्धान्त में एवं कर्म-सिद्धान्त में भी किसी अन्य के भला-बुरा करने की व्यवस्था नहीं है; तथापि व्यवहारभक्ति में वीतरागी भगवान को भी सुख-दुःख का कर्ता-हर्ता कहने का व्यवहार है। (१) तार्किक शिरोमणि स्वामी समन्तभद्राचार्य ने लिखा भी है - "हे नाथ! न आपको पूजा से कोई प्रयोजन है और न निन्दा से, क्योंकि आप समस्त १. “अहंदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनेषु भावविशुद्धियुक्तोऽनुराग: भक्ति।" - सर्वार्थसिद्धि ६/२४/२३९ २. “अहंदादिगुणानुरागो भक्तिः।” -भगवती आराधना वि. ४७/१५९ ३. "मोक्खगयं पुरिसाणं गुणभेद जाणिऊण तेसि पि"... - नियमसार, गाथा : १३५ ४. "भक्तिः पुनः सम्यक्त्व भण्यते व्यवहारेण सराग सम्यग्दृष्टिनां पंचपरमेष्ठिचाराधनारूपा।" -समयसार, तात्पर्यवृत्ति टीका १७३/१७६/२४३ ५. "निजपरमात्मतत्त्वसम्यश्रद्धानावबोधाचरणात्मकेषु शुद्धरत्नत्रयपरिणामेषु भाजनं भक्तिराराधनेत्यर्थः । एकादशपदेषु श्रावकेषु सर्वे शुद्धरत्नत्रयभक्ति कुर्वन्ति।" - नियमसार, तात्पर्यवृत्ति, पृष्ठ : १३४ ६.“वीतरागसम्यग्दृष्टिनां शुद्धात्मतत्त्वभावनारूपा चेति।" - समयसार, तात्पर्यवृत्ति टीका १७३/१७६/ २४३Page Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 80