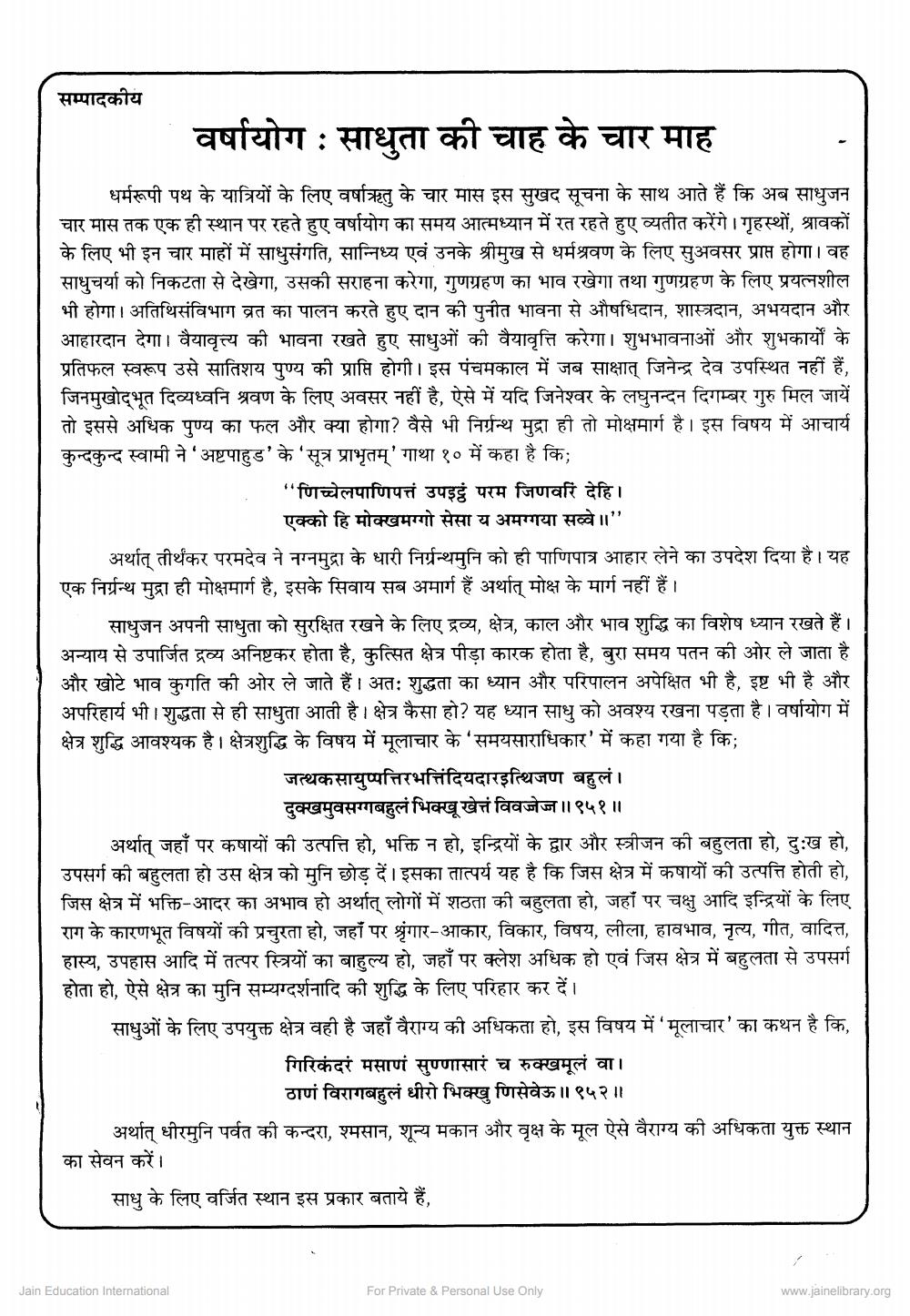Book Title: Jinabhashita 2005 08 Author(s): Ratanchand Jain Publisher: Sarvoday Jain Vidyapith Agra View full book textPage 5
________________ सम्पादकीय वर्षायोग : साधुता की चाह के चार माह धर्मरूपी पथ के यात्रियों के लिए वर्षाऋतु के चार मास इस सुखद सूचना के साथ आते हैं कि अब साधुजन चार मास तक एक ही स्थान पर रहते हुए वर्षायोग का समय आत्मध्यान में रत रहते हुए व्यतीत करेंगे। गृहस्थों, श्रावकों के लिए भी इन चार माहों में साधुसंगति, सान्निध्य एवं उनके श्रीमुख से धर्मश्रवण के लिए सुअवसर प्राप्त होगा। वह साधुचर्या को निकटता से देखेगा, उसकी सराहना करेगा, गणग्रहण का भाव रखेगा तथा गुणग्रहण के लिए प्रयत्नशील भी होगा। अतिथिसंविभाग व्रत का पालन करते हए दान की पुनीत भावना से औषधिदान, शास्त्रदान, अभयदान और आहारदान देगा। वैयावृत्त्य की भावना रखते हुए साधुओं की वैयावृत्ति करेगा। शुभभावनाओं और शुभकार्यों के प्रतिफल स्वरूप उसे सातिशय पुण्य की प्राप्ति होगी। इस पंचमकाल में जब साक्षात् जिनेन्द्र देव उपस्थित नहीं हैं, जिनमुखोद्भूत दिव्यध्वनि श्रवण के लिए अवसर नहीं है, ऐसे में यदि जिनेश्वर के लघुनन्दन दिगम्बर गुरु मिल जायें तो इससे अधिक पुण्य का फल और क्या होगा? वैसे भी निर्ग्रन्थ मुद्रा ही तो मोक्षमार्ग है। इस विषय में आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने 'अष्टपाहुड' के 'सूत्र प्राभृतम्' गाथा १० में कहा है कि; "णिच्चेलपाणिपत्तं उपडद्रं परम जिणवरि देहि। एक्को हि मोक्खमग्गो सेसा य अमग्गया सव्वे॥" अर्थात् तीर्थंकर परमदेव ने नग्नमुद्रा के धारी निर्ग्रन्थमनि को ही पाणिपात्र आहार लेने का उपदेश दिया है। यह एक निर्ग्रन्थ मुद्रा ही मोक्षमार्ग है, इसके सिवाय सब अमार्ग हैं अर्थात् मोक्ष के मार्ग नहीं हैं। साधुजन अपनी साधुता को सुरक्षित रखने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव शुद्धि का विशेष ध्यान रखते हैं। अन्याय से उपार्जित द्रव्य अनिष्टकर होता है, कुत्सित क्षेत्र पीड़ा कारक होता है, बुरा समय पतन की ओर ले जाता है और खोटे भाव कुगति की ओर ले जाते हैं। अतः शुद्धता का ध्यान और परिपालन अपेक्षित भी है, इष्ट भी है और अपरिहार्य भी। शुद्धता से ही साधुता आती है। क्षेत्र कैसा हो? यह ध्यान साधु को अवश्य रखना पड़ता है। वर्षायोग में क्षेत्र शुद्धि आवश्यक है। क्षेत्रशुद्धि के विषय में मूलाचार के 'समयसाराधिकार' में कहा गया है कि; जत्थकसायुप्पत्तिरभत्तिंदियदारइत्थिजण बहुलं । दुक्खमुवसग्गबहुलं भिक्खूखेत्तं विवजेज॥९५१ ।। अर्थात् जहाँ पर कषायों की उत्पत्ति हो, भक्ति न हो, इन्द्रियों के द्वार और स्त्रीजन की बहुलता हो, दु:ख हो, उपसर्ग की बहुलता हो उस क्षेत्र को मुनि छोड़ दें। इसका तात्पर्य यह है कि जिस क्षेत्र में कषायों की उत्पत्ति होती हो, भक्ति-आदर का अभाव हो अर्थात लोगों में शठता की बहलता हो, जहाँ पर चक्ष आदि इन्द्रियों के लिए राग के कारणभूत विषयों की प्रचुरता हो, जहाँ पर श्रृंगार-आकार, विकार, विषय, लीला, हावभाव, नृत्य, गीत, वादित्त, हास्य, उपहास आदि में तत्पर स्त्रियों का बाहुल्य हो, जहाँ पर क्लेश अधिक हो एवं जिस क्षेत्र में बहुलता से उपसर्ग होता हो, ऐसे क्षेत्र का मुनि सम्यग्दर्शनादि की शुद्धि के लिए परिहार कर दें। साधुओं के लिए उपयुक्त क्षेत्र वही है जहाँ वैराग्य की अधिकता हो, इस विषय में 'मूलाचार' का कथन है कि, | गिरिकंदरं मसाणं सुण्णासारं च रुक्खमूलं वा। ठाणं विरागबहुलं धीरो भिक्खु णिसेवेऊ॥९५२॥ अर्थात् धीरमुनि पर्वत की कन्दरा, श्मसान, शून्य मकान और वृक्ष के मूल ऐसे वैराग्य की अधिकता युक्त स्थान का सेवन करें। साधु के लिए वर्जित स्थान इस प्रकार बताये हैं, जिस क्षेत्र में भक्ति-आदर क Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36