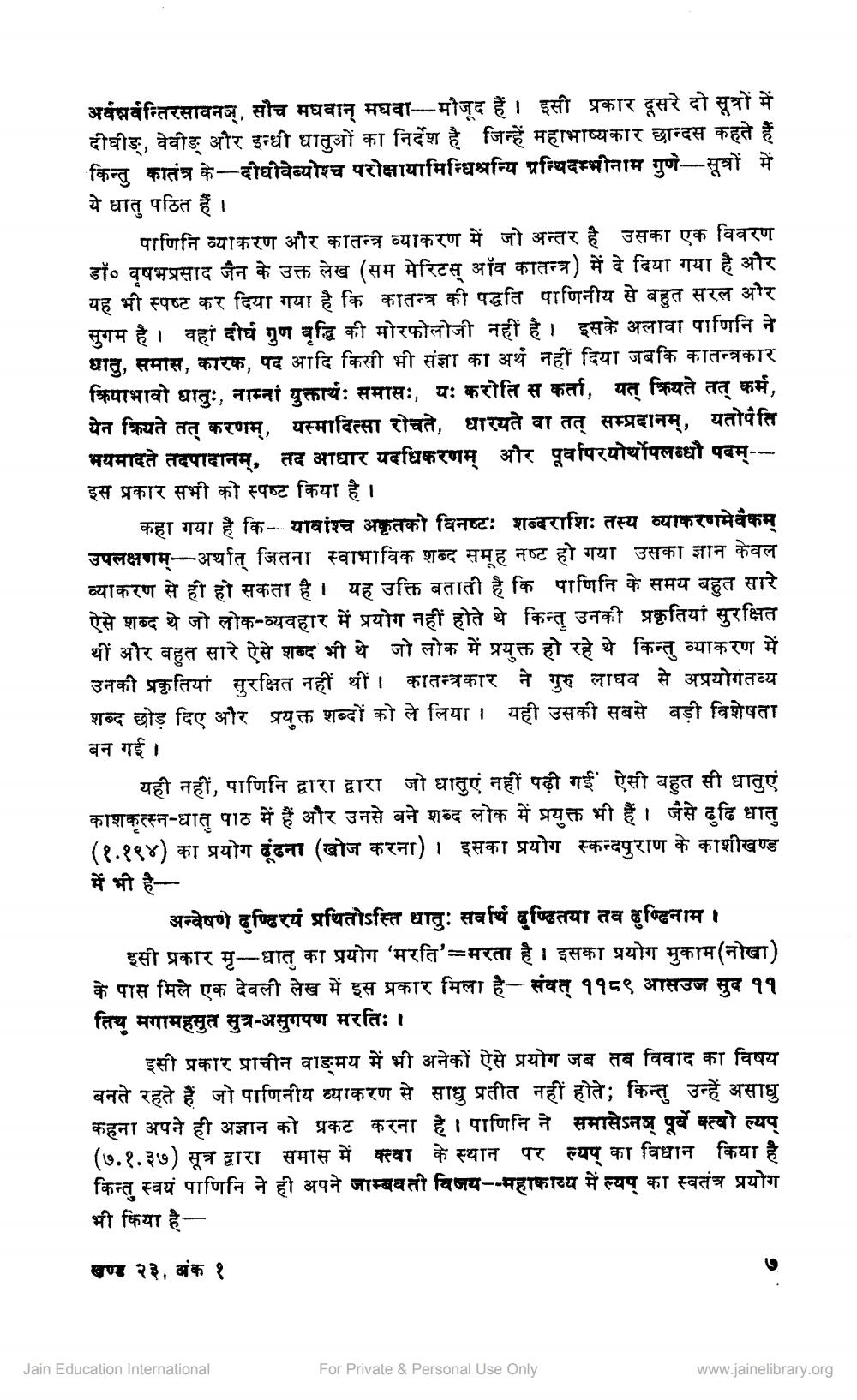Book Title: Tulsi Prajna 1997 04 Author(s): Parmeshwar Solanki Publisher: Jain Vishva Bharati View full book textPage 8
________________ अर्वशर्वन्तिरसावनञ्, सौच मघवान् मघवा --- - मौजूद हैं। इसी प्रकार दूसरे दो सूत्रों में दीघीङ्, वेवीङ् और इन्धी धातुओं का निर्देश है जिन्हें महाभाष्यकार छान्दस कहते हैं किन्तु कातंत्र के दीघीवेन्योश्च परोक्षायामिन्धिश्रन्यि ग्रन्थिदम्भोनाम गुणे -- सूत्रों में ये धातु पठित हैं । - पाणिनि व्याकरण और कातन्त्र व्याकरण में जो अन्तर है उसका एक विवरण डॉ० वृषभप्रसाद जैन के उक्त लेख (सम मेरिटस् ऑव कातन्त्र ) में दे दिया गया है और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कातन्त्र की पद्धति पाणिनीय से बहुत सरल और सुगम है। वहां दीर्घ गुण वृद्धि की मोरफोलोजी नहीं है। इसके अलावा पाणिनि ने धातु, समास, कारक, पद आदि किसी भी संज्ञा का अर्थ नहीं दिया जबकि कातन्त्रकार frerभावो धातुः, नाम्नां युक्तार्थः समासः यः करोति स कर्ता, यत् क्रियते तत् कर्म, येन क्रियते तत् करणम्, यस्मादित्सा रोचते, धारयते वा तत् सम्प्रदानम्, यतोपैति भयमादते तदपादानम्, तद आधार यदधिकरणम् और पूर्वापरयोर्थोपलब्धौ पदम्-इस प्रकार सभी को स्पष्ट किया है । कहा गया है कि - यावांश्च अकृतको विनष्टः शब्दराशिः तस्य व्याकरणमेवैकम् उपलक्षणम्-अर्थात् जितना स्वाभाविक शब्द समूह नष्ट हो गया उसका ज्ञान केवल व्याकरण से ही हो सकता है । यह उक्ति बताती है कि पाणिनि के समय बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो लोक व्यवहार में प्रयोग नहीं होते थे किन्तु उनकी प्रकृतियां सुरक्षित जो लोक में प्रयुक्त हो रहे थे किन्तु व्याकरण में कातन्त्रकार ने गुरु लाघव से अप्रयोगंतव्य ले लिया। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता और बहुत सारे ऐसे शब्द भी थे उनकी प्रकृतियां सुरक्षित नहीं थीं । शब्द छोड़ दिए और प्रयुक्त शब्दों को बन गई । यही नहीं, पाणिनि द्वारा द्वारा जो धातुएं नहीं पढ़ी गई ऐसी बहुत सी धातुएं ' हैं और उनसे बने शब्द लोक में प्रयुक्त भी हैं । जैसे दुढि धातु काशकृत्स्न-धातु पाठ ( १. १९४) का प्रयोग ढूंढना ( खोज करना) । इसका प्रयोग स्कन्दपुराण के काशीखण्ड में भी है अन्वेषणे दृष्ठिरयं प्रथितोऽस्ति धातुः सर्वार्थ दुष्टितया तव दुष्टिनाम । इसी प्रकार मृ-धातु का प्रयोग 'मरति' = मरता है । इसका प्रयोग मुकाम (नोखा ) के पास मिले एक देवली लेख में इस प्रकार मिला है - संवत् ११८९ आसउज सुद ११ तिथु मगामहसुत सुत्र - असुगपण मरतिः । इसी प्रकार प्राचीन वाङ्मय में भी बनते रहते हैं जो पाणिनीय व्याकरण से कहना अपने ही अज्ञान को प्रकट करना है । पाणिनि ने ( ७.१.३७) सूत्र द्वारा समास में क्त्वा के स्थान पर ल्यप् का विधान किया है किन्तु स्वयं पाणिनि ने ही अपने जाम्बवती विजय - महाकाव्य में ल्यप् का स्वतंत्र प्रयोग अनेकों ऐसे प्रयोग जब तब विवाद का विषय साधु प्रतीत नहीं होते; किन्तु उन्हें असाधु समासेऽनञ् पूर्वे क्त्वो ल्यप् भी किया है खण्ड २३, अंक १ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 216