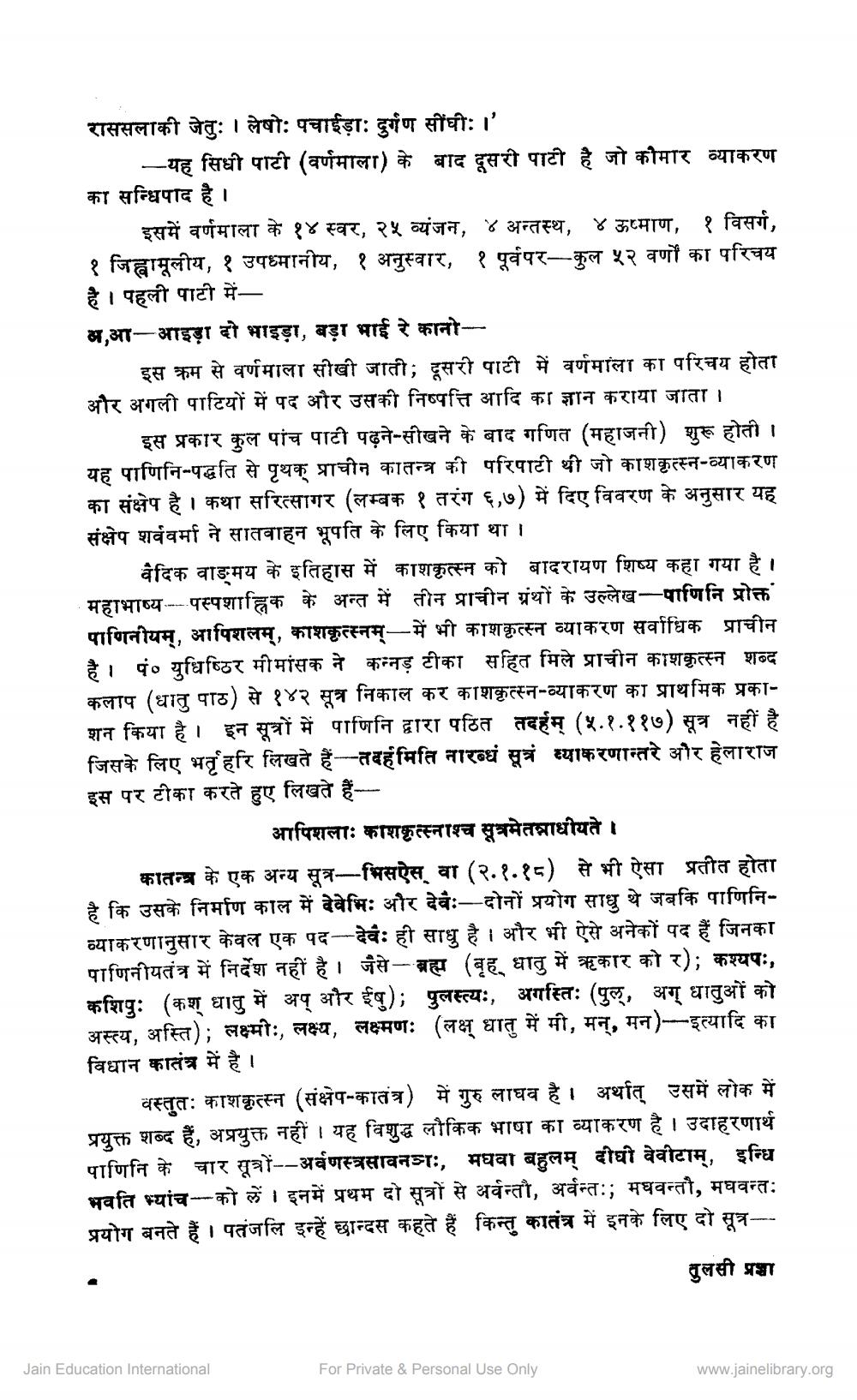Book Title: Tulsi Prajna 1997 04 Author(s): Parmeshwar Solanki Publisher: Jain Vishva Bharati View full book textPage 7
________________ राससलाकी जेतुः । लेषोः पचाईड़ा: दुर्गण सींघीः।' -यह सिधी पाटी (वर्णमाला) के बाद दूसरी पाटी है जो कौमार व्याकरण का सन्धिपाद है। इसमें वर्णमाला के १४ स्वर, २५ व्यंजन, ४ अन्तस्थ, ४ ऊष्माण, १ विसर्ग, १ जिह्वामूलीय, १ उपध्मानीय, १ अनुस्वार, १ पूर्वपर-कुल ५२ वर्णों का परिचय है। पहली पाटी मेंअ,आ-आइड़ा दो भाइड़ा, बड़ा भाई रे कानो इस क्रम से वर्णमाला सीखी जाती; दूसरी पाटी में वर्णमाला का परिचय होता और अगली पाटियों में पद और उसकी निष्पत्ति आदि का ज्ञान कराया जाता। इस प्रकार कुल पांच पाटी पढ़ने-सीखने के बाद गणित (महाजनी) शुरू होती। यह पाणिनि-पद्धति से पृथक् प्राचीन कातन्त्र की परिपाटी थी जो काशकृत्स्न-व्याकरण का संक्षेप है। कथा सरित्सागर (लम्बक १ तरंग ६,७) में दिए विवरण के अनुसार यह संक्षेप शर्ववर्मा ने सातवाहन भूपति के लिए किया था। वैदिक वाङ्मय के इतिहास में काशकृत्स्न को बादरायण शिष्य कहा गया है। महाभाष्य-----पस्पशाह्निक के अन्त में तीन प्राचीन ग्रंथों के उल्लेख-पाणिनि प्रोक्त पाणिनीयम्, आपिशलम्, काशकृत्स्नम्-में भी काशकृत्स्न व्याकरण सर्वाधिक प्राचीन है। पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने कन्नड़ टीका सहित मिले प्राचीन काशकृत्स्न शब्द कलाप (धातु पाठ) से १४२ सूत्र निकाल कर काशकृत्स्न-व्याकरण का प्राथमिक प्रकाशन किया है। इन सूत्रों में पाणिनि द्वारा पठित तदहम् (५.१.११७) सूत्र नहीं है जिसके लिए भर्तृहरि लिखते हैं-तदह मिति नारब्धं सूत्रं व्याकरणान्तरे और हेलाराज इस पर टीका करते हुए लिखते हैं आपिशलाः काशकृत्स्नाश्च सूत्रमेतन्नाधीयते । कातन्त्र के एक अन्य सूत्र-भिसऐस वा २.१.१८) से भी ऐसा प्रतीत होता है कि उसके निर्माण काल में देवेभिः और देवैः-दोनों प्रयोग साधु थे जबकि पाणिनिव्याकरणानुसार केवल एक पद-देवः ही साधु है । और भी ऐसे अनेकों पद हैं जिनका पाणिनीयतंत्र में निर्देश नहीं है। जैसे- ब्रह्म (बृह, धातु में ऋकार को र); कश्यपः, कशिपुः (कश् धातु में अप् और ईषु); पुलस्त्यः, अगस्तिः (पुल, अग् धातुओं को अस्त्य, अस्ति); लक्ष्मीः , लक्ष्य, लक्ष्मणः (लक्ष् धातु में मी, मन्, मन)-इत्यादि का विधान कातंत्र में है। वस्तुतः काशकृत्स्न (संक्षेप-कातंत्र) में गुरु लाघव है। अर्थात् उसमें लोक में प्रयुक्त शब्द हैं, अप्रयुक्त नहीं । यह विशुद्ध लौकिक भाषा का व्याकरण है। उदाहरणार्थ पाणिनि के चार सूत्रों--अर्वणस्त्रसावनञः, मघवा बहुलम् दीघी वेवीटाम्, इन्धि भवति भ्यांच-को लें। इनमें प्रथम दो सूत्रों से अर्वन्तौ, अर्वन्तः; मघवन्तौ, मघवन्तः प्रयोग बनते हैं। पतंजलि इन्हें छान्दस कहते हैं किन्तु कातंत्र में इनके लिए दो सूत्र-- तुलसी प्रशा Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 216