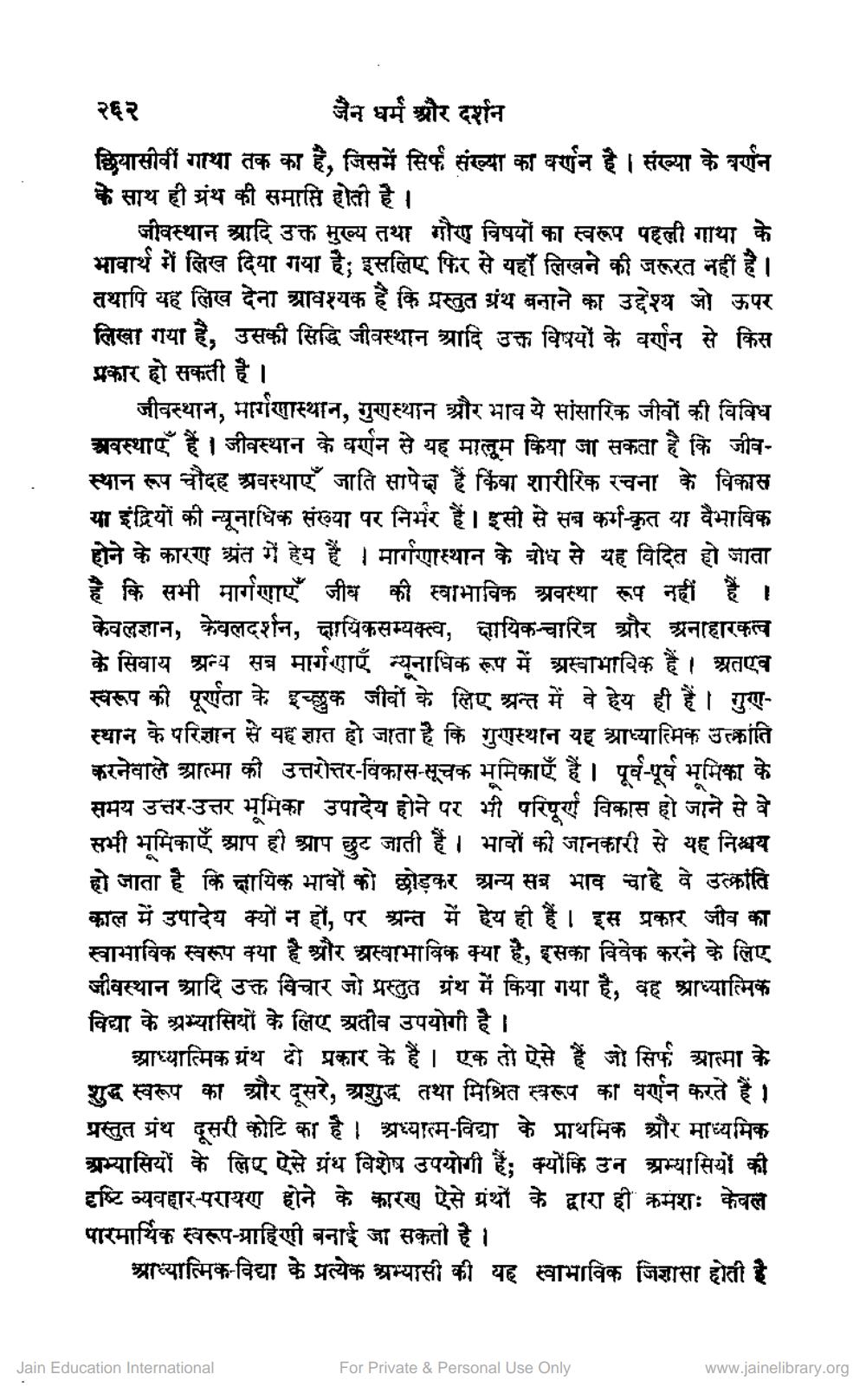Book Title: Shadashitika Author(s): Sukhlal Sanghavi Publisher: Z_Darshan_aur_Chintan_Part_1_2_002661.pdf View full book textPage 6
________________ २६२ जैन धर्म और दर्शन छियासीवीं गाथा तक का है, जिसमें सिर्फ संख्या का वर्णन है । संख्या के वर्णन के साथ ही ग्रंथ की समाप्ति होती है । जीवस्थान आदि उक्त मुख्य तथा गौण विषयों का स्वरूप पहली गाथा के भावार्थ में लिख दिया गया है; इसलिए फिर से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है । तथापि यह लिख देना आवश्यक है कि प्रस्तुत ग्रंथ बनाने का उद्देश्य जो ऊपर लिखा गया है, उसकी सिद्धि जीवस्थान आदि उक्त विषयों के वर्णन से किस प्रकार हो सकती है । 1 जीवस्थान, मार्गणास्थान, गुणस्थान और भाव ये सांसारिक जीवों की विविध अवस्थाएँ हैं । जीवस्थान के वर्णन से यह मालूम किया जा सकता है कि जीवस्थान रूप चौदह अवस्थाएँ जाति सापेक्ष हैं किंवा शारीरिक रचना के विकास या इंद्रियों की न्यूनाधिक संख्या पर निर्भर हैं। इसी से सब कर्म-कृत या वैभाविक होने के कारण अंत में हेय हैं । मार्गणास्थान के बोध से यह विदित हो जाता है कि सभी मार्गणाएँ जीव की स्वाभाविक अवस्था रूप नहीं हैं । केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र और अनाहारकत्व के सिवाय अन्य सत्र मार्गणाएँ न्यूनाधिक रूप में अस्वाभाविक हैं । अतएव स्वरूप की पूर्णता के इच्छुक जीवों के लिए अन्त में वे हेय ही हैं। गुणस्थान के परिज्ञान से यह ज्ञात हो जाता है कि गुणस्थान यह श्राध्यात्मिक उत्क्रांति करनेवाले श्रात्मा की उत्तरोत्तर विकास सूचक भूमिकाएँ हैं । पूर्व-पूर्व भूमिका के समय उत्तर- उत्तर भूमिका उपादेय होने पर भी परिपूर्ण विकास हो जाने से वे सभी भूमिकाएँ आप ही आप छुट जाती हैं। भावों की जानकारी से यह निश्चय हो जाता है कि क्षायिक भावों को छोड़कर अन्य सब भाव चाहे वे उत्क्रांति काल में उपादेय क्यों न हों, पर अन्त में हेय ही हैं। इस प्रकार जीव का स्वाभाविक स्वरूप क्या है और अस्वाभाविक क्या है, इसका विवेक करने के लिए जीवस्थान आदि उक्त विचार जो प्रस्तुत ग्रंथ में किया गया है, वह श्राध्यात्मिक विद्या के अभ्यासियों के लिए अतीव उपयोगी है । आध्यात्मिक ग्रंथ दो प्रकार के हैं । एक तो ऐसे हैं जो सिर्फ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और दूसरे, अशुद्ध, तथा मिश्रित स्वरूप का वर्णन करते हैं । प्रस्तुत ग्रंथ दूसरी कोटि का है । अध्यात्मविद्या के प्राथमिक और माध्यमिक अभ्यासियों के लिए ऐसे ग्रंथ विशेष उपयोगी हैं; क्योंकि उन अभ्यासियों की दृष्टि व्यवहार-परायण होने के कारण ऐसे ग्रंथों के द्वारा ही क्रमशः केवल पारमार्थिक स्वरूप ग्राहिणी बनाई जा सकती है । श्रध्यात्मिक-विद्या के प्रत्येक अभ्यासी की यह स्वाभाविक जिज्ञासा होती है Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40