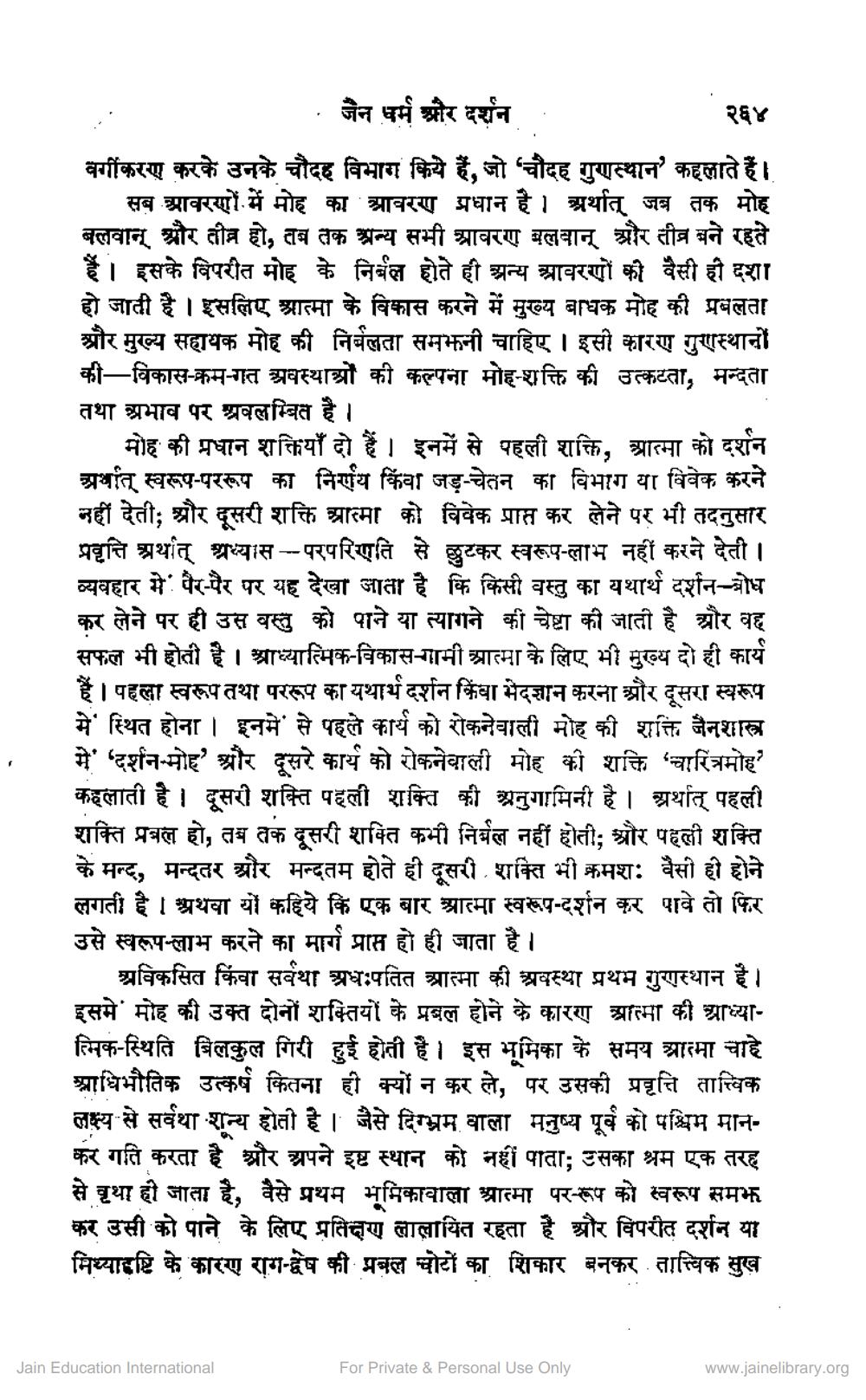Book Title: Shadashitika Author(s): Sukhlal Sanghavi Publisher: Z_Darshan_aur_Chintan_Part_1_2_002661.pdf View full book textPage 8
________________ . जैन धर्म और दर्शन . २६४ वर्गीकरण करके उनके चौदह विभाग किये हैं, जो 'चौदह गुणस्थान' कहलाते हैं। ___सब आवरणों में मोह का आवरण प्रधान है। अर्थात् जब तक मोह बलवान् और तीन हो, तब तक अन्य सभी प्रावरण बलवान् और तीव्र बने रहते है। इसके विपरीत मोह के निर्बल होते ही अन्य आवरणों की वैसी ही दशा हो जाती है । इसलिए श्रात्मा के विकास करने में मुख्य बाधक मोह की प्रबलता और मुख्य सहायक मोह की निर्बलता समझनी चाहिए । इसी कारण गुणस्थानों की-विकास-क्रम-गत अवस्थाओं की कल्पना मोह-शक्ति की उत्कटता, मन्दता तथा अभाव पर अवलम्बित है। मोह की प्रधान शक्तियाँ दो हैं। इनमें से पहली शक्ति, आत्मा को दर्शन अर्थात् स्वरूप-पररूप का निर्णय किंवा जड़-चेतन का विभाग या विवेक करने नहीं देती; और दूसरी शक्ति प्रात्मा को विवेक प्राप्त कर लेने पर भी तदनुसार प्रवृत्ति अर्थात् अथ्यास -- परपरिणति से छुटकर स्वरूप-लाभ नहीं करने देती । व्यवहार में पैर-पैर पर यह देखा जाता है कि किसी वस्तु का यथार्थ दर्शन-बोध कर लेने पर ही उस वस्तु को पाने या त्यागने की चेष्टा की जाती है और वह सफल भी होती है । श्राध्यात्मिक-विकास-गामी आत्मा के लिए भी मुख्य दो ही कार्य है। पहला स्वरूप तथा पररूप का यथार्थ दर्शन किंवा भेदज्ञान करना और दूसरा स्वरूप में स्थित होना। इनमें से पहले कार्य को रोकनेवाली मोह की शक्ति जैनशास्त्र में 'दर्शन-मोह' और दूसरे कार्य को रोकनेवाली मोह की शक्ति 'चारित्रमोह' कहलाती है। दूसरी शक्ति पहली शक्ति की अनुगामिनी है। अर्थात् पहली शक्ति प्रबल हो, तब तक दूसरी शक्ति कभी निर्बल नहीं होती; और पहली शक्ति के मन्द, मन्दतर और मन्दतम होते ही दूसरी शक्ति भी क्रमशः वैसी ही होने लगती है । श्रथवा यों कहिये कि एक बार अात्मा स्वरूप-दर्शन कर पावे तो फिर उसे स्वरूप-लाभ करने का मार्ग प्राप्त हो ही जाता है। अविकसित किंवा सर्वथा अध:पतित आत्मा की अवस्था प्रथम गुणस्थान है। इसमे मोह की उक्त दोनों शक्तियों के प्रबल होने के कारण आत्मा की प्राध्यात्मिक-स्थिति बिलकुल गिरी हुई होती है। इस भमिका के समय आत्मा चाहे नाधिभौतिक उत्कर्ष कितना ही क्यों न कर ले, पर उसकी प्रवृत्ति तात्त्विक लक्ष्य से सर्वथा शून्य होती है। जैसे दिग्भ्रम वाला मनुष्य पूर्व को पश्चिम मानकर गति करता है और अपने इष्ट स्थान को नहीं पाता; उसका श्रम एक तरह से वृथा ही जाता है, वैसे प्रथम भूमिकावाला श्रात्मा पर-रूप को स्वरूप समझ कर उसी को पाने के लिए प्रतिक्षण लालायित रहता है और विपरीत दर्शन या मिथ्यादृष्टि के कारण राग-द्वेष की प्रबल चोटों का शिकार बनकर तात्त्विक सुख Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40