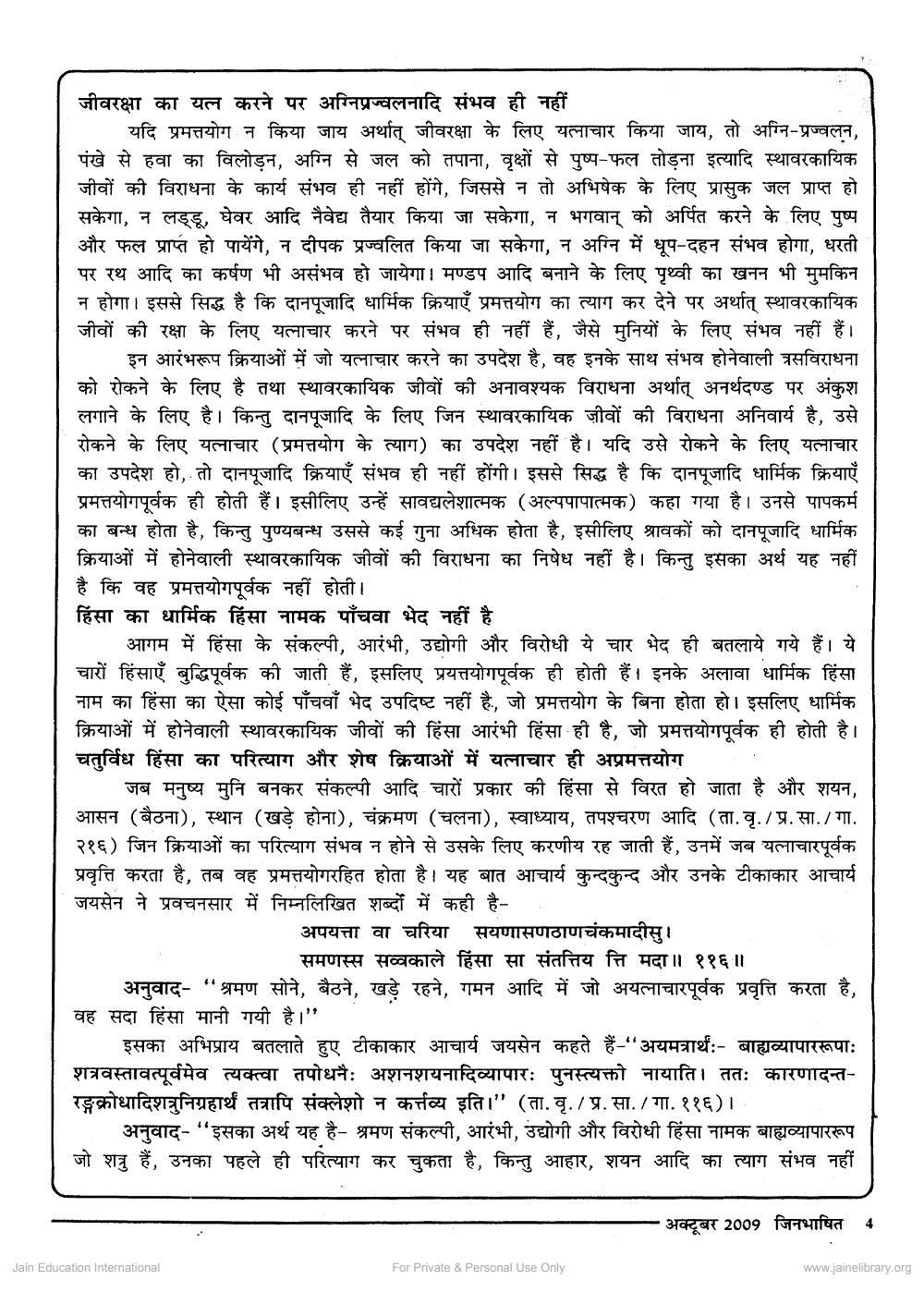Book Title: Jinabhashita 2009 10 Author(s): Ratanchand Jain Publisher: Sarvoday Jain Vidyapith Agra View full book textPage 6
________________ जीवरक्षा का यत्न करने पर अग्निप्रज्वलनादि संभव ही नहीं यदि प्रमत्तयोग न किया जाय अर्थात् जीवरक्षा के लिए यत्नाचार किया जाय, तो अग्नि-प्रज्वलन, पंखे से हवा का विलोड़न, अग्नि से जल को तपाना, वृक्षों से पुष्प-फल तोड़ना इत्यादि स्थावरकायिक जीवों की विराधना के कार्य संभव ही नहीं होंगे, जिससे न तो अभिषेक के लिए प्रासुक जल प्राप्त हो सकेगा, न लड्डू, घेवर आदि नैवेद्य तैयार किया जा सकेगा, न भगवान् को अर्पित करने के लिए पुष्प और फल प्राप्त हो पायेंगे, न दीपक प्रज्वलित किया जा सकेगा, न अग्नि में धूप-दहन संभव होगा, धरती पर रथ आदि का कर्षण भी असंभव हो जायेगा। मण्डप आदि बनाने के लिए पृथ्वी का खनन भी मुमकिन न होगा। इससे सिद्ध है कि दानपूजादि धार्मिक क्रियाएँ प्रमत्तयोग का त्याग कर देने पर अर्थात् स्थावरकायिक जीवों की रक्षा के लिए यत्नाचार करने पर संभव ही नहीं हैं, जैसे मुनियों के लिए संभव नहीं हैं। इन आरंभरूप क्रियाओं में जो यत्नाचार करने का उपदेश है, वह इनके साथ संभव होनेवाली त्रसविराधना को रोकने के लिए है तथा स्थावरकायिक जीवों की अनावश्यक विराधना अर्थात् अनर्थदण्ड पर अंकुश लगाने के लिए है। किन्तु दानपूजादि के लिए जिन स्थावरकायिक जीवों की विराधना अनिवार्य है, उसे रोकने के लिए यत्नाचार (प्रमत्तयोग के त्याग) का उपदेश नहीं है। यदि उसे रोकने के लिए यत्नाचार का उपदेश हो, तो दानपूजादि क्रियाएँ संभव ही नहीं होंगी। इससे सिद्ध है कि दानपूजादि धार्मिक क्रियाएँ प्रमत्तयोगपूर्वक ही होती हैं। इसीलिए उन्हें सावद्यलेशात्मक (अल्पपापात्मक) कहा गया है। उनसे पापकर्म का बन्ध होता है, किन्तु पुण्यबन्ध उससे कई गुना अधिक होता है, इसीलिए श्रावकों को दानपूजादि धार्मिक क्रियाओं में होनेवाली स्थावरकायिक जीवों की विराधना का निषेध नहीं है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह प्रमत्तयोगपूर्वक नहीं होती। हिंसा का धार्मिक हिंसा नामक पाँचवा भेद नहीं है आगम में हिंसा के संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी ये चार भेद ही बतलाये गये हैं। ये चारों हिंसाएँ बुद्धिपूर्वक की जाती हैं, इसलिए प्रयत्तयोगपूर्वक ही होती हैं। इनके अलावा धार्मिक हिंसा नाम का हिंसा का ऐसा कोई पाँचवाँ भेद उपदिष्ट नहीं है, जो प्रमत्तयोग के बिना होता हो। इसलिए धार्मिक क्रियाओं में होनेवाली स्थावरकायिक जीवों की हिंसा आरंभी हिंसा ही है, जो प्रमत्तयोगपूर्वक ही होती है। चतुर्विध हिंसा का परित्याग और शेष क्रियाओं में यत्नाचार ही अप्रमत्तयोग जब मनुष्य मुनि बनकर संकल्पी आदि चारों प्रकार की हिंसा से विरत हो जाता है और शयन, आसन (बैठना), स्थान (खड़े होना), चंक्रमण (चलना), स्वाध्याय, तपश्चरण आदि (ता. वृ./ प्र. सा. / गा. २१६) जिन क्रियाओं का परित्याग संभव न होने से उसके लिए करणीय रह जाती हैं, उनमें जब यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है, तब वह प्रमत्तयोगरहित होता है। यह बात आचार्य कुन्दकुन्द और उनके टीकाकार आचार्य जयसेन ने प्रवचनसार में निम्नलिखित शब्दों में कही है-.. अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु। समणस्स सव्वकाले हिंसा सा संतत्तिय त्ति मदा॥ ११६॥ अनुवाद- "श्रमण सोने, बैठने, खड़े रहने, गमन आदि में जो अयत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है, वह सदा हिंसा मानी गयी है।" इसका अभिप्राय बतलाते हुए टीकाकार आचार्य जयसेन कहते हैं-"अयमत्रार्थ:- बाह्यव्यापाररूपाः शत्रवस्तावत्पूर्वमेव त्यक्त्वा तपोधनैः अशनशयनादिव्यापारः पुनस्त्यक्तो नायाति। ततः कारणादन्तरङ्गक्रोधादिशत्रुनिग्रहार्थं तत्रापि संक्लेशो न कर्त्तव्य इति।" (ता. वृ./ प्र. सा./गा. ११६)। अनवाद- "इसका अर्थ यह है- श्रमण संकल्पी. आरंभी. उद्योगी और विरोधी हिंसा नामक बाह्यव्यापाररूप जो शत्रु हैं, उनका पहले ही परित्याग कर चुकता है, किन्तु आहार, शयन आदि का त्याग संभव नहीं -अक्टूबर 2009 जिनभाषित 4 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36