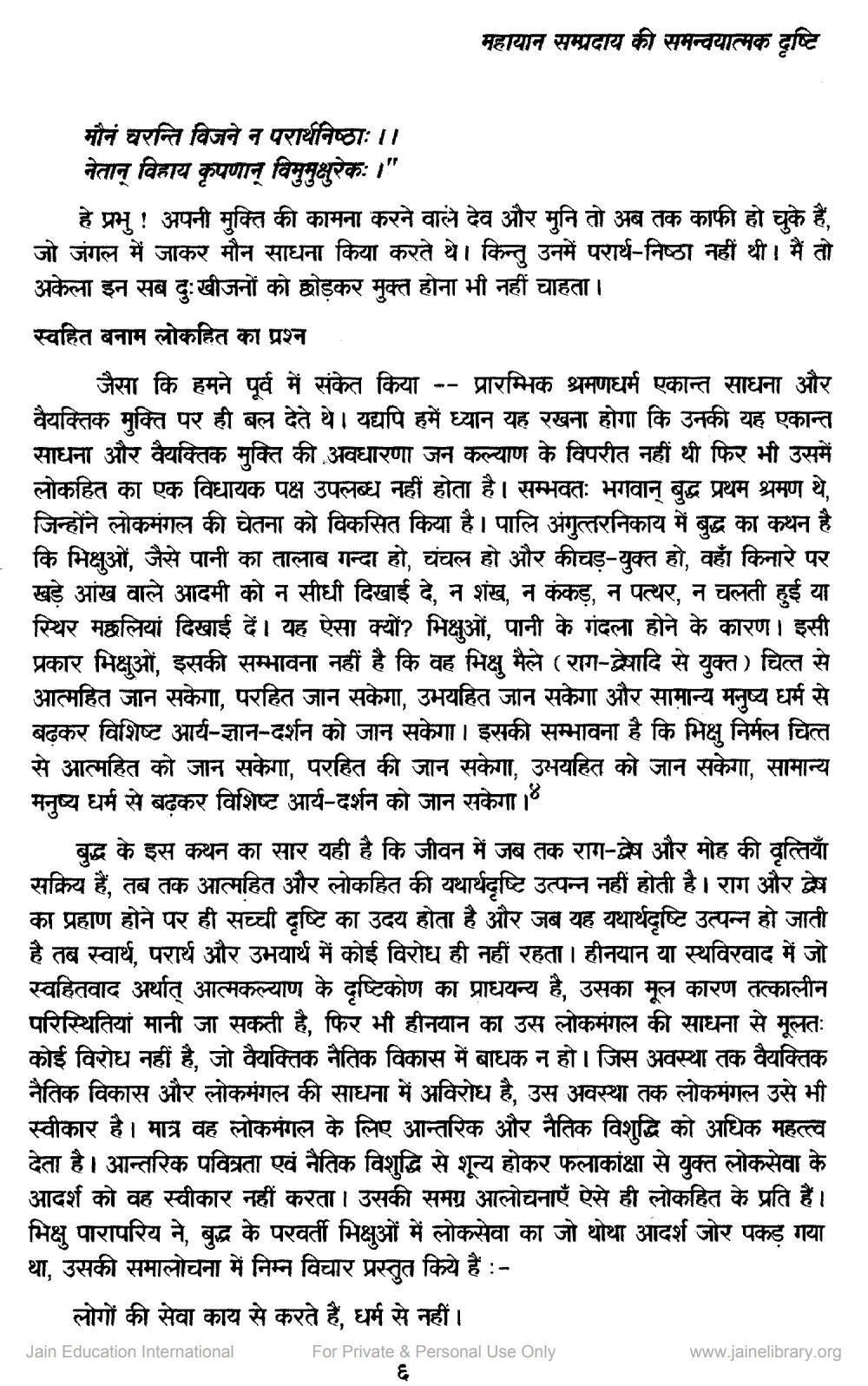Book Title: Sramana 1993 07 Author(s): Ashok Kumar Singh Publisher: Parshvanath Vidhyashram Varanasi View full book textPage 8
________________ महायान सम्प्रदाय की समन्वयात्मक दृष्टि मौनं घरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः ।। नेतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षुरेकः।" हे प्रभु ! अपनी मुक्ति की कामना करने वाले देव और मुनि तो अब तक काफी हो चुके हैं, जो जंगल में जाकर मौन साधना किया करते थे। किन्तु उनमें परार्थ-निष्ठा नहीं थी। मैं तो अकेला इन सब दुःखीजनों को छोड़कर मुक्त होना भी नहीं चाहता। स्वहित बनाम लोकहित का प्रश्न जैसा कि हमने पूर्व में संकेत किया -- प्रारम्भिक श्रमणधर्म एकान्त साधना और वैयक्तिक मुक्ति पर ही बल देते थे। यद्यपि हमें ध्यान यह रखना होगा कि उनकी यह एकान्त साधना और वैयक्तिक मुक्ति की अवधारणा जन कल्याण के विपरीत नहीं थी फिर भी उसमें लोकहित का एक विधायक पक्ष उपलब्ध नहीं होता है। सम्भवतः भगवान् बुद्ध प्रथम श्रमण थे, जिन्होंने लोकमंगल की चेतना को विकसित किया है। पालि अंगुत्तरनिकाय में बुद्ध का कथन है कि भिक्षुओं, जैसे पानी का तालाब गन्दा हो, चंचल हो और कीचड़-युक्त हो, वहाँ किनारे पर खड़े आंख वाले आदमी को न सीधी दिखाई दे, न शंख, न कंकड़, न पत्थर, न चलती हुई या स्थिर मछलियां दिखाई दें। यह ऐसा क्यों? भिक्षुओं, पानी के गंदला होने के कारण। इसी प्रकार भिक्षुओं, इसकी सम्भावना नहीं है कि वह भिक्षु मैले (राग-द्वेषादि से युक्त) चित्त से आत्महित जान सकेगा, परहित जान सकेगा, उभयहित जान सकेगा और सामान्य मनुष्य धर्म से बढ़कर विशिष्ट आर्य-ज्ञान-दर्शन को जान सकेगा। इसकी सम्भावना है कि भिक्षु निर्मल चित्त से आत्महित को जान सकेगा, परहित की जान सकेगा, उसयहित को जान सकेगा, सामान्य मनुष्य धर्म से बढ़कर विशिष्ट आर्य-दर्शन को जान सकेगा। बुद्ध के इस कथन का सार यही है कि जीवन में जब तक राग-द्वेष और मोह की वृत्तियाँ सक्रिय हैं, तब तक आत्महित और लोकहित की यथार्थदृष्टि उत्पन्न नहीं होती है। राग और द्वेष का प्रहाण होने पर ही सच्ची दृष्टि का उदय होता है और जब यह यथार्थदृष्टि उत्पन्न हो जाती है तब स्वार्थ, परार्थ और उभयार्थ में कोई विरोध ही नहीं रहता। हीनयान या स्थविरवाद में जो स्वहितवाद अर्थात् आत्मकल्याण के दृष्टिकोण का प्राधयन्य है, उसका मूल कारण तत्कालीन परिस्थितियां मानी जा सकती है, फिर भी हीनयान का उस लोकमंगल की साधना से मूलतः कोई विरोध नहीं है, जो वैयक्तिक नैतिक विकास में बाधक न हो। जिस अवस्था तक वैयक्तिक नैतिक विकास और लोकमंगल की साधना में अविरोध है, उस अवस्था तक लोकमंगल उसे भी स्वीकार है। मात्र वह लोकमंगल के लिए आन्तरिक और नैतिक विशुद्धि को अधिक महत्त्व देता है। आन्तरिक पवित्रता एवं नैतिक विशुद्धि से शून्य होकर फलाकांक्षा से युक्त लोकसेवा के आदर्श को वह स्वीकार नहीं करता। उसकी समग्र आलोचनाएँ ऐसे ही लोकहित के प्रति हैं। भिक्षु पारापरिय ने, बुद्ध के परवर्ती भिक्षुओं में लोकसेवा का जो थोथा आदर्श जोर पकड़ गया था, उसकी समालोचना में निम्न विचार प्रस्तुत किये हैं : लोगों की सेवा काय से करते हैं, धर्म से नहीं। Jain Education International www.jainelibrary.org For Private & Personal Use OnlyPage Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66