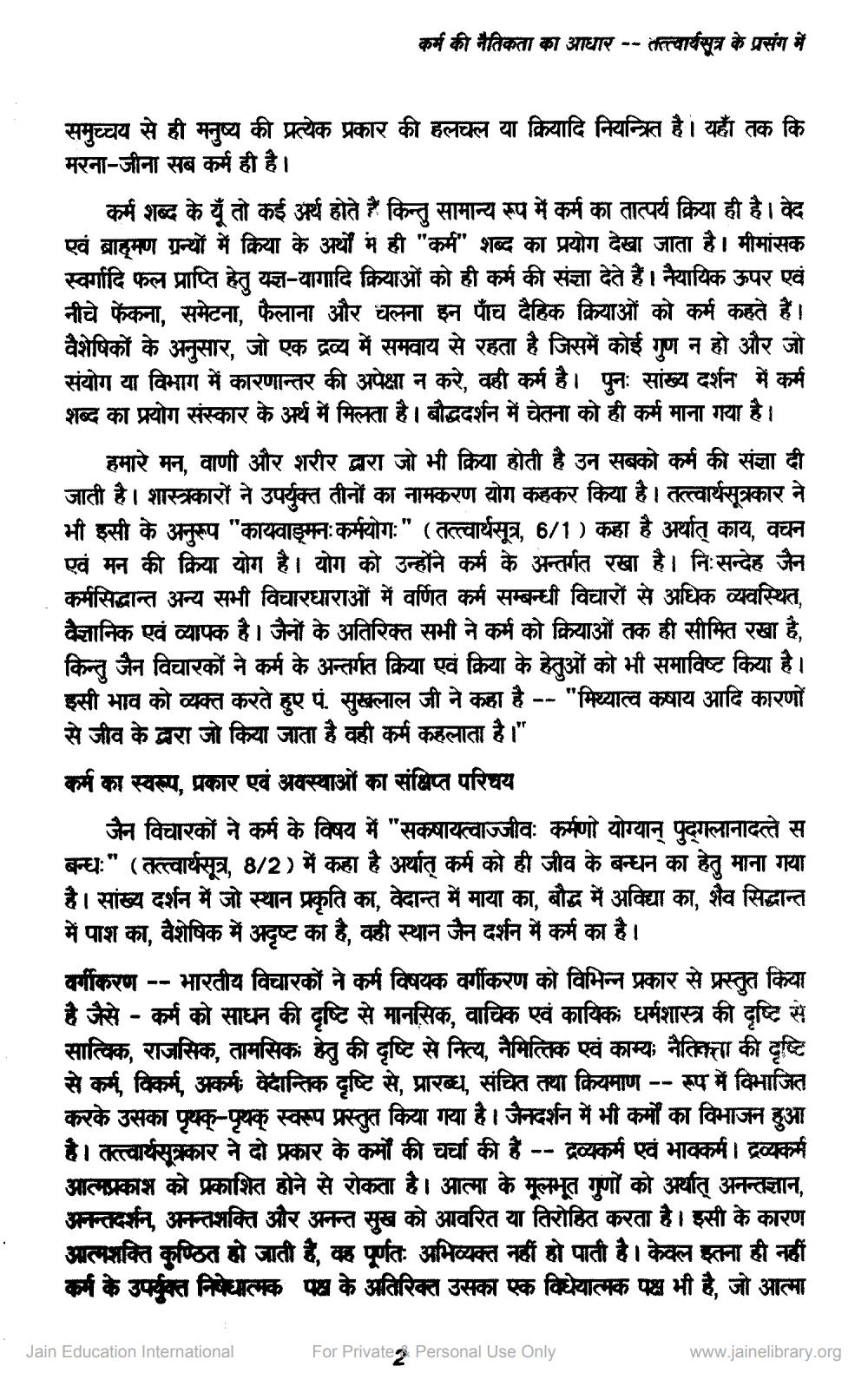Book Title: Sramana 1994 07 Author(s): Ashok Kumar Singh Publisher: Parshvanath Vidhyashram Varanasi View full book textPage 4
________________ कर्म की नैतिकता का आधार -- तत्त्वार्यसूत्र के प्रसंग में समुच्चय से ही मनुष्य की प्रत्येक प्रकार की हलचल या क्रियादि नियन्त्रित है। यहाँ तक कि मरना-जीना सब कर्म ही है। कर्म शब्द के यूँ तो कई अर्थ होते हैं किन्तु सामान्य स्प में कर्म का तात्पर्य क्रिया ही है। वेद एवं ब्राहमण ग्रन्थों में किया के अर्थों में ही "कर्म" शब्द का प्रयोग देखा जाता है। मीमांसक स्वर्गादि फल प्राप्ति हेतु यज्ञ-यागादि क्रियाओं को ही कर्म की संज्ञा देते हैं। नैयायिक ऊपर एवं नीचे फेंकना, समेटना, फैलाना और चलना इन पाँच दैहिक क्रियाओं को कर्म कहते हैं। वैशेषिकों के अनुसार, जो एक द्रव्य में समवाय से रहता है जिसमें कोई गुण न हो और जो संयोग या विभाग में कारणान्तर की अपेक्षा न करे, वही कर्म है। पुनः सांख्य दर्शन में कर्म शब्द का प्रयोग संस्कार के अर्थ में मिलता है। बौद्धदर्शन में चेतना को ही कर्म माना गया है। ___हमारे मन, वाणी और शरीर द्वारा जो भी क्रिया होती है उन सबको कर्म की संज्ञा दी जाती है। शास्त्रकारों ने उपर्युक्त तीनों का नामकरण योग कहकर किया है। तत्त्वार्थसूत्रकार ने भी इसी के अनुरूप "कायवाङ्मनःकर्मयोगः" (तत्त्वार्थसूत्र, 6/1) कहा है अर्थात् काय, वचन एवं मन की क्रिया योग है। योग को उन्होंने कर्म के अन्तर्गत रखा है। निःसन्देह जैन कर्मसिद्धान्त अन्य सभी विचारधाराओं में वर्णित कर्म सम्बन्धी विचारों से अधिक व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं व्यापक है। जैनों के अतिरिक्त सभी ने कर्म को क्रियाओं तक ही सीमित रखा है, किन्तु जैन विचारकों ने कर्म के अन्तर्गत क्रिया एवं क्रिया के हेतुओं को भी समाविष्ट किया है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए पं. सुखलाल जी ने कहा है -- "मिथ्यात्व कषाय आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया जाता है वही कर्म कहलाता है।" कर्म का स्वरूप, प्रकार एवं अवस्थाओं का संक्षिप्त परिचय जैन विचारकों ने कर्म के विषय में "सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः" (तत्त्वार्थसत्र, 8/2) में कहा है अर्थात कर्म को ही जीव के बन्धन का हेतु माना गया है। सांख्य दर्शन में जो स्थान प्रकृति का, वेदान्त में माया का, बौद्ध में अविद्या का, शैव सिद्धान्त में पाश का, वैशेषिक में अदृष्ट का है, वही स्थान जैन दर्शन में कर्म का है। वर्गीकरण -- भारतीय विचारकों ने कर्म विषयक वर्गीकरण को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया है जैसे - कर्म को साधन की दृष्टि से मानसिक, वाचिक एवं कायिक धर्मशास्त्र की दृष्टि से सात्विक, राजसिक, तामसिक हेतु की दृष्टि से नित्य, नैमित्तिक एवं काम्यः नैतिकता की दृष्टि से कर्म, विकर्म, अकर्मः वेदान्तिक दृष्टि से, प्रारब्ध, संचित तथा कियमाण -- रूप में विभाजित करके उसका पृथक-पृथक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। जैनदर्शन में भी कर्मों का विभाजन हुआ है। तत्त्वार्यसूत्रकार ने दो प्रकार के कर्मों की चर्चा की है -- द्रव्यकर्म एवं भावकर्म। द्रव्यकर्म आत्मप्रकाश को प्रकाशित होने से रोकता है। आत्मा के मूलभूत गुणों को अर्थात् अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्त सुख को आवरित या तिरोहित करता है। इसी के कारण आत्मशक्ति कुण्ठित हो जाती है, यह पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं हो पाती है। केवल इतना ही नहीं कर्म के उपर्युक्त निषेधात्मक पक्ष के अतिरिक्त उसका एक विधेयात्मक पक्ष भी है, जो आत्मा Jain Education International For Private Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 78