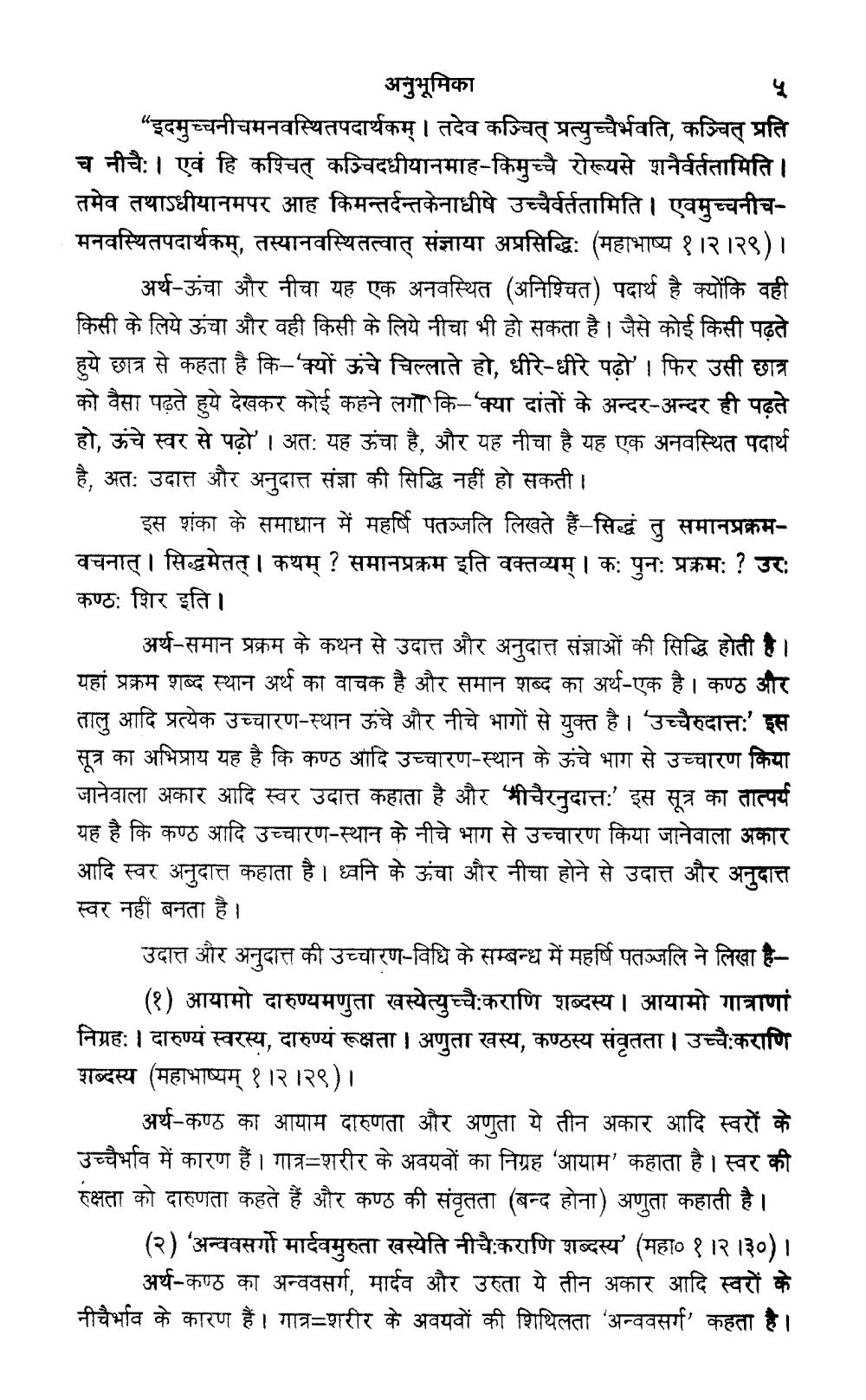Book Title: Paniniya Ashtadhyayi Pravachanam Part 05 Author(s): Sudarshanacharya Publisher: Bramharshi Swami Virjanand Arsh Dharmarth Nyas Zajjar View full book textPage 6
________________ अनुभूमिका “इदमुच्चनीचमनवस्थितपदार्थकम् । तदेव कञ्चित् प्रत्युच्चैर्भवति, कञ्चित् प्रति च नीचैः। एवं हि कश्चित् कञ्चिदधीयानमाह-किमुच्चै रोख्यसे शनैर्वर्ततामिति । तमेव तथाऽधीयानमपर आह किमन्तर्दन्तकेनाधीषे उच्चैर्वर्ततामिति । एवमुच्चनीचमनवस्थितपदार्थकम्, तस्यानवस्थितत्वात् संज्ञाया अप्रसिद्धिः (महाभाष्य १।२।२९)। अर्थ-ऊंचा और नीचा यह एक अनवस्थित (अनिश्चित) पदार्थ है क्योंकि वही किसी के लिये ऊंचा और वही किसी के लिये नीचा भी हो सकता है। जैसे कोई किसी पढ़ते हुये छात्र से कहता है कि-'क्यों ऊंचे चिल्लाते हो, धीरे-धीरे पढ़ो'। फिर उसी छात्र को वैसा पढ़ते हुये देखकर कोई कहने लगा कि-'क्या दांतों के अन्दर-अन्दर ही पढ़ते हो, ऊंचे स्वर से पढ़ो' । अत: यह ऊंचा है, और यह नीचा है यह एक अनवस्थित पदार्थ है, अत: उदात्त और अनुदात्त संज्ञा की सिद्धि नहीं हो सकती। इस शंका के समाधान में महर्षि पतञ्जलि लिखते हैं-सिद्धं तु समानप्रक्रमवचनात् । सिद्धमेतत् । कथम् ? समानप्रक्रम इति वक्तव्यम् । क: पुन: प्रक्रम: ? उर: कण्ठ: शिर इति। अर्थ-समान प्रक्रम के कथन से उदात्त और अनदात्त संज्ञाओं की सिद्धि होती है। यहां प्रक्रम शब्द स्थान अर्थ का वाचक है और समान शब्द का अर्थ-एक है। कण्ठ और तालु आदि प्रत्येक उच्चारण-स्थान ऊंचे और नीचे भागों से युक्त है। ‘उच्चैरुदात्त:' इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि कण्ठ आदि उच्चारण-स्थान के ऊंचे भाग से उच्चारण किया जानेवाला अकार आदि स्वर उदात्त कहाता है और भीचैरनुदात्त:' इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि कण्ठ आदि उच्चारण-स्थान के नीचे भाग से उच्चारण किया जानेवाला अकार आदि स्वर अनुदात्त कहाता है। ध्वनि के ऊंचा और नीचा होने से उदात्त और अनुदात्त स्वर नहीं बनता है। उदात्त और अनुदात्त की उच्चारण-विधि के सम्बन्ध में महर्षि पतञ्जलि ने लिखा है (१) आयामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चैःकराणि शब्दस्य । आयामो गात्राणां निग्रहः । दारुण्यं स्वरस्य, दारुण्यं रूक्षता । अणुता खस्य, कण्ठस्य संवृतता। उच्चैःकराणि शब्दस्य (महाभाष्यम् १।२।२९)। अर्थ-कण्ठ का आयाम दारुणता और अणुता ये तीन अकार आदि स्वरों के उच्चैर्भाव में कारण हैं। गात्र शरीर के अवयवों का निग्रह 'आयाम' कहाता है। स्वर की रुक्षता को दारुणता कहते हैं और कण्ठ की संवृतता (बन्द होना) अणुता कहाती है। (२) 'अन्ववसर्गो मार्दवमुरुता खस्येति नीचैःकराणि शब्दस्य' (महा० १।२ ।३०)। अर्थ-कण्ठ का अन्ववसर्ग, मार्दव और उरुता ये तीन अकार आदि स्वरों के नीचैर्भाव के कारण हैं। गात्र=शरीर के अवयवों की शिथिलता ‘अन्ववसर्ग' कहता है।Page Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 754