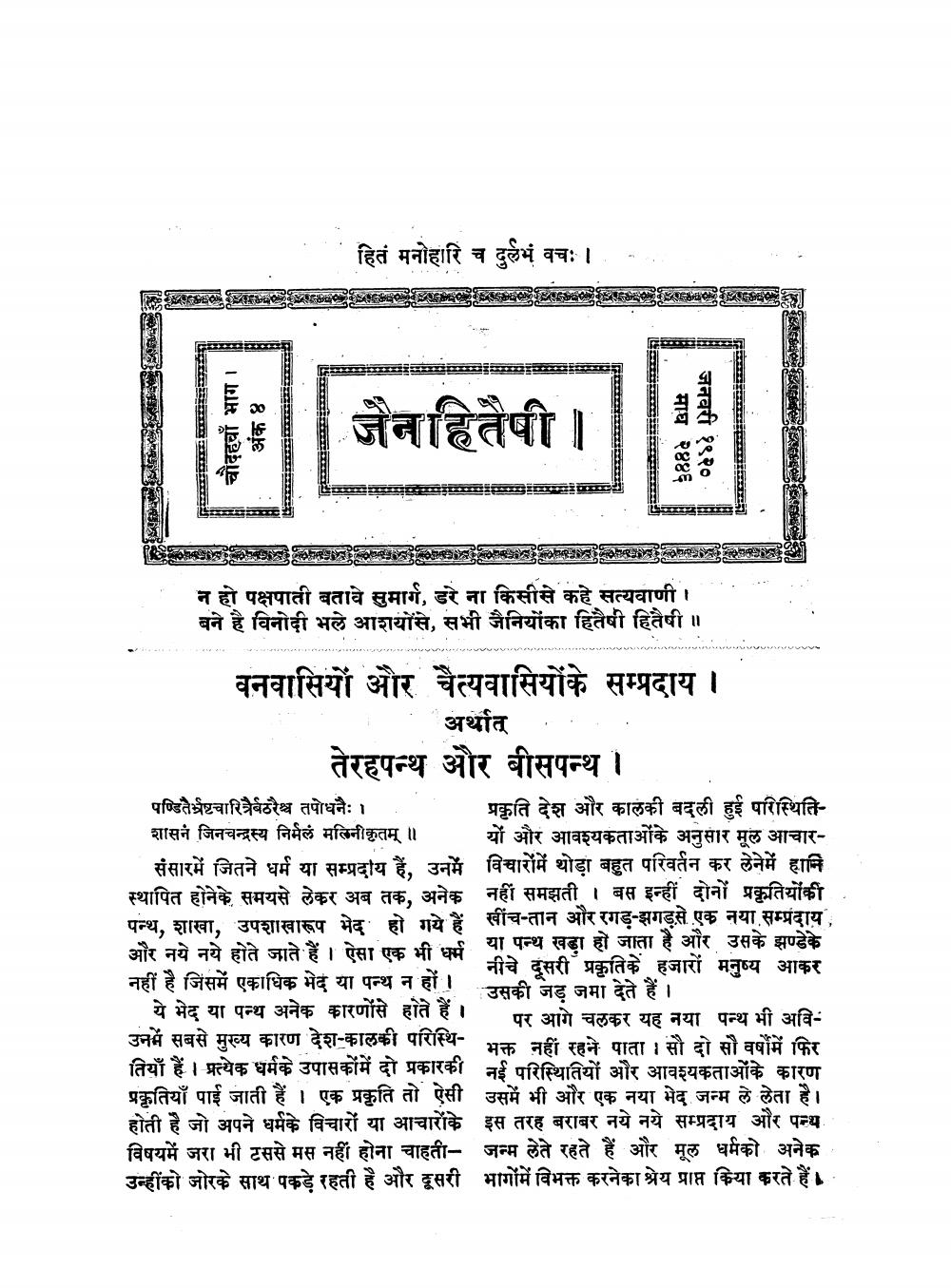Book Title: Jain Hiteshi 1920 01 02 Ank 04 05 Author(s): Nathuram Premi Publisher: Jain Granthratna Karyalay View full book textPage 3
________________ हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः ।। चौदहवाँ भाग। अंक ४ जैनहितैषी। माघ २४४६ जनवरी १९२० । न हो पक्षपाती बतावे सुमार्ग, डरे ना किसीसे कहे सत्यवाणी। बने है विनोदी भले आशयोंसे, सभी जैनियोंका हितैषी हितैषी ॥ वनवासियों और चैत्यवासियोंके सम्प्रदाय । अर्थात् ... तेरहपन्थ और बीसपन्थ । पण्डितैभ्रष्टचारित्रैर्बठरैश्च तपोधनैः। प्रकृति देश और कालकी बदली हुई परिस्थितिशासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनीकृतम् ॥ यों और आवश्यकताओंके अनुसार मूल आचार संसारमें जितने धर्म या सम्प्रदाय हैं, उनमें विचारोंमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेनेमें हानि स्थापित होनेके समयसे लेकर अब तक, अनेक नहीं समझती । बस इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी पन्थ, शाखा, उपशाखारूप भेद हो गये हैं खींच-तान और रगड़-झगड़से एक नया सम्प्रदाय और नये नये होते जाते हैं। ऐसा एक भी धर्म या पन्थ खड़ा हो जाता है और उसके झण्डेके " नीचे दुसरी प्रकृतिके हजारों मनुष्य आकर नहीं है जिसमें एकाधिक भेद या पन्थ न हों। - उसकी जड़ जमा देते हैं। ये भेद या पन्थ अनेक कारणोंसे होते हैं। पर आगे चलकर यह नया पन्थ भी अविउनमें सबसे मुख्य कारण देश-कालकी परिस्थि भक्त नहीं रहने पाता । सौ दो सौ वर्षों में फिर तियाँ हैं। प्रत्येक धर्मके उपासकोंमें दो प्रकारकी नई परिस्थितियों और आवश्यकताओंके कारण प्रकृतियाँ पाई जाती हैं । एक प्रकृति तो ऐसी उसमें भी और एक नया भेद जन्म ले लेता है। होती है जो अपने धर्मके विचारों या आचारोंके इस तरह बराबर नये नये सम्प्रदाय और पन्य विषयमें जरा भी टससे मस नहीं होना चाहती- जन्म लेते रहते हैं और मूल धर्मको अनेक उन्हींको जोरके साथ पकड़े रहती है और दूसरी भागोंमें विभक्त करनेका श्रेय प्राप्त किया करते हैं।Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 60