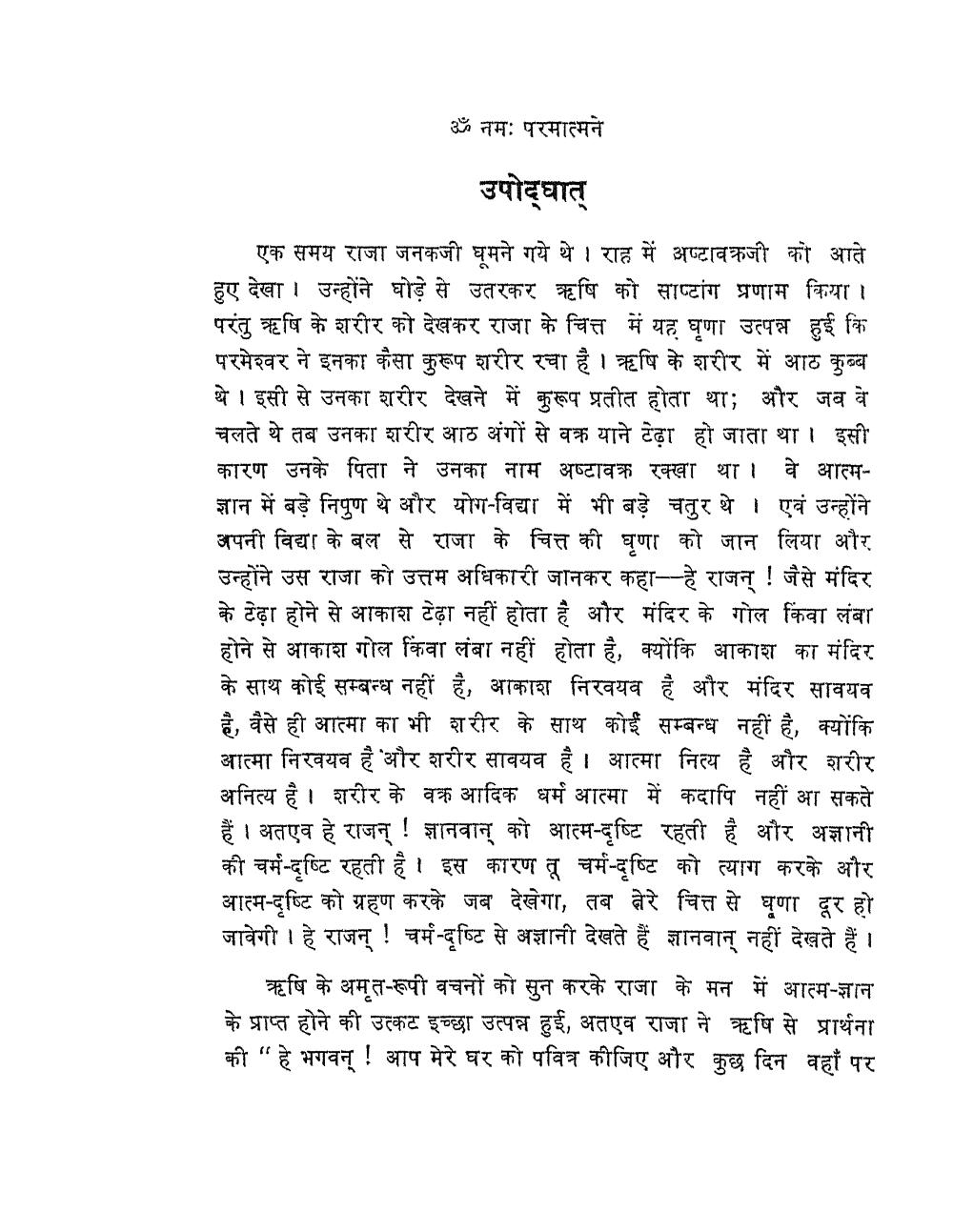Book Title: Astavakra Gita Author(s): Raibahaddur Babu Jalimsinh Publisher: Tejkumar Press View full book textPage 5
________________ ॐ नमः परमात्मने उपोद्घात् एक समय राजा जनकजी घूमने गये थे । राह में अष्टावक्रजी को आते हुए देखा। उन्होंने घोड़े से उतरकर ऋषि को साप्टांग प्रणाम किया। परंतु ऋषि के शरीर को देखकर राजा के चित्त में यह घृणा उत्पन्न हुई कि परमेश्वर ने इनका कैसा कुरूप शरीर रचा है । ऋषि के शरीर में आठ कुब्ब थे । इसी से उनका शरीर देखने में कुरूप प्रतीत होता था; और जब वे चलते थे तब उनका शरीर आठ अंगों से वक्र याने टेढ़ा हो जाता था। इसी कारण उनके पिता ने उनका नाम अष्टावक्र रक्खा था। वे आत्मज्ञान में बड़े निपुण थे और योग-विद्या में भी बड़े चतुर थे । एवं उन्होंने अपनी विद्या के बल से राजा के चित्त की घृणा को जान लिया और उन्होंने उस राजा को उत्तम अधिकारी जानकर कहा--हे राजन् ! जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और मंदिर के गोल किंवा लंबा होने से आकाश गोल किंवा लंबा नहीं होता है, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, आकाश निरवयव है और मंदिर सावयव है, वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा निरवयव है और शरीर सावयव है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। शरीर के वक्र आदिक धर्म आत्मा में कदापि नहीं आ सकते हैं । अतएव हे राजन् ! ज्ञानवान् को आत्म-दृष्टि रहती है और अज्ञानी की चर्म-दृष्टि रहती है। इस कारण तू चर्म-दृष्टि को त्याग करके और आत्म-दृष्टि को ग्रहण करके जब देखेगा, तब तेरे चित्त से घणा दूर हो जावेगी । हे राजन् ! चर्म-दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं ज्ञानवान् नहीं देखते हैं। ऋषि के अमृत-रूपी वचनों को सुन करके राजा के मन में आत्म-ज्ञान के प्राप्त होने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई, अतएव राजा ने ऋषि से प्रार्थना की " हे भगवन् ! आप मेरे घर को पवित्र कीजिए और कुछ दिन वहाँ परPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 405