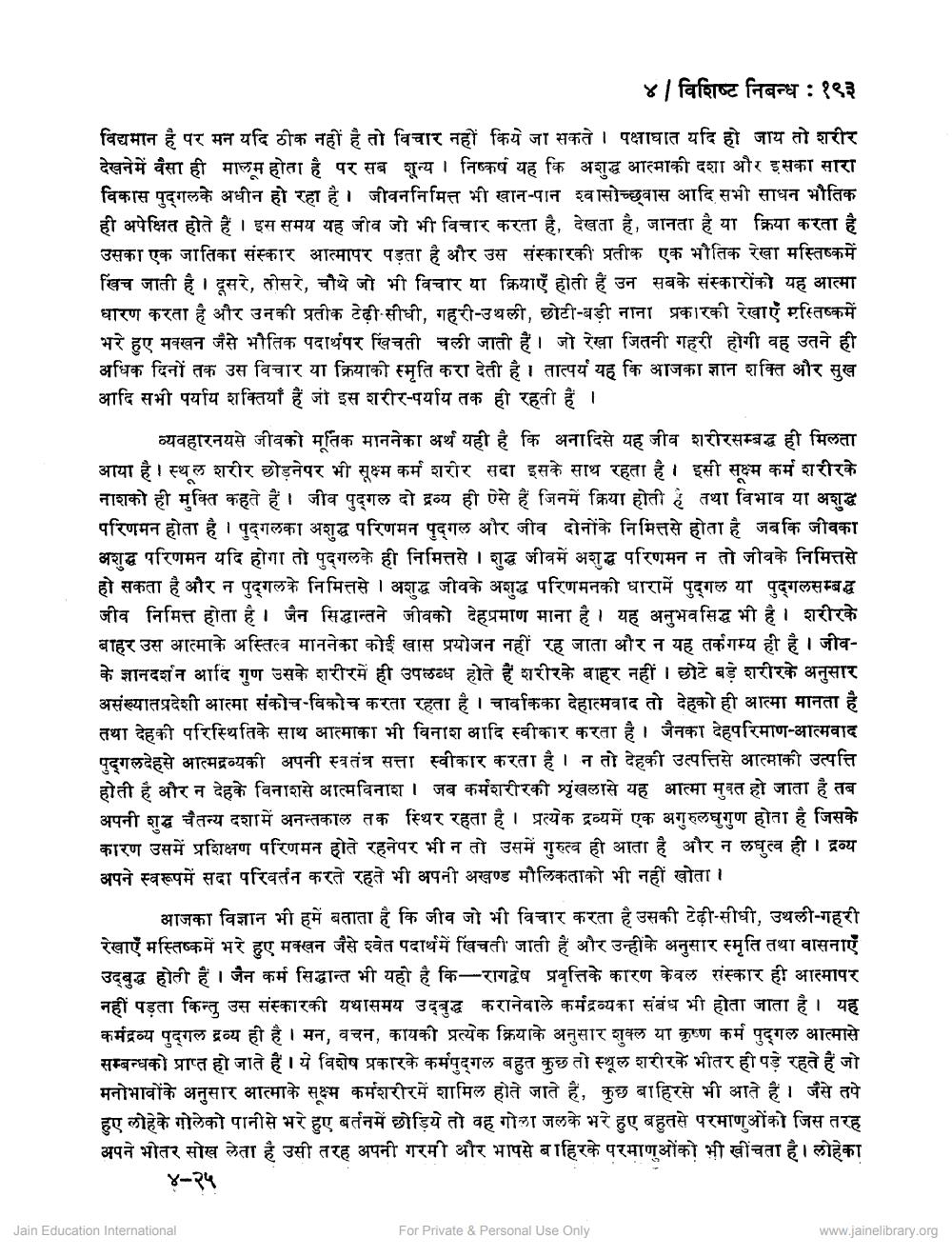Book Title: Tattvarth vrutti aur Shrutsagarsuri Author(s): Publisher: Z_Mahendrakumar_Jain_Nyayacharya_Smruti_Granth_012005.pdf View full book textPage 9
________________ ४/ विशिष्ट निबन्ध : १९३ विद्यमान है पर मन यदि ठीक नहीं है तो विचार नहीं किये जा सकते । पक्षाघात यदि हो जाय तो शरीर देखने में वैसा ही मालम होता है पर सब शून्य । निष्कर्ष यह कि अशुद्ध आत्माकी दशा और इसका सारा विकास पुद्गलके अधीन हो रहा है। जीवननिमित्त भी खान-पान श्वासोच्छ्वास आदि सभी साधन भौतिक ही अपेक्षित होते हैं । इस समय यह जीव जो भी विचार करता है, देखता है, जानता है या क्रिया करता है उसका एक जातिका संस्कार आत्मापर पड़ता है और उस संस्कारकी प्रतीक एक भौतिक रेखा मस्तिष्कमें खिंच जाती है । दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी विचार या क्रियाएँ होती हैं उन सबके संस्कारोंको यह आत्मा धारण करता है और उनकी प्रतीक टेढी सीधी. गहरी-उथली. छोटी-बडी नाना प्रकारकी रेखाएं मस्तिष्कमें भरे हुए मक्खन जैसे भौतिक पदार्थपर खिंचती चली जाती हैं। जो रेखा जितनी गहरी होगी वह उतने ही अधिक दिनों तक उस विचार या क्रियाको स्मति करा देती है। तात्पर्य यह कि आजका ज्ञान शक्ति और सुख आदि सभी पर्याय शक्तियाँ हैं जो इस शरीर-पर्याय तक ही रहती है । व्यवहारनयसे जीवको मूर्तिक माननेका अर्थ यही है कि अनादिसे यह जीव शरीरसम्बद्ध ही मिलता आया है। स्थूल शरीर छोड़नेपर भी सूक्ष्म कर्म शरीर सदा इसके साथ रहता है। इसी सूक्ष्म कर्म शरीरके नाशको ही मुक्ति कहते हैं। जीव पुद्गल दो द्रव्य ही ऐसे हैं जिनमें क्रिया होती है तथा विभाव या अशुद्ध परिणमन होता है । पुद्गलका अशुद्ध परिणमन पुद्गल और जीव दोनोंके निमित्तसे होता है जबकि जीवका अशद्ध परिणमन यदि होगा तो पुद्गलके ही निमित्तसे । शुद्ध जीवमें अशद्ध परिणमन न तो जीवके निमित्तसे हो सकता है और न पदगलके निमित्तसे । अशद्ध जीवके अशद्ध परिणमनको धारामें पदगल या पदगलसम्बद्ध जीव निमित्त होता है। जैन सिद्धान्तने जीवको देहप्रमाण माना है। यह अनुभवसिद्ध भी है। शरीरके बाहर उस आत्माके अस्तित्व माननेका कोई खास प्रयोजन नहीं रह जाता और न यह तर्कगम्य ही है । जीवके ज्ञानदर्शन आदि गुण उसके शरीरमें ही उपलब्ध होते है शरीरके बाहर नहीं। छोटे बड़े शरीरके अनुसार असंख्यातप्रदेशी आत्मा संकोच-विकोच करता रहता है । चार्वाकका देहात्मवाद तो देहको ही आत्मा मानता है तथा देहकी परिस्थितिके साथ आत्माका भी विनाश आदि स्वीकार करता है। जैनका देहपरिमाण-आत्मवाद पुद्गलदेहसे आत्मद्रव्यकी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता है । न तो देहकी उत्पत्तिसे आत्माकी उत्पत्ति होती है और न देहके विनाशसे आत्मविनाश । जब कर्मशरीरकी श्रृंखलासे यह आत्मा मुक्त हो जाता है तब अपनी शद्ध चैतन्य दशामें अनन्तकाल तक स्थिर रहता है। प्रत्येक द्रव्यमें एक अगुरुलघुगुण होता है जिसके कारण उसमें प्रशिक्षण परिणमन होते रहनेपर भी न तो उसमें गुरुत्व ही आता है और न लघुत्व ही । द्रव्य अपने स्वरूपमें सदा परिवर्तन करते रहते भी अपनी अखण्ड मौलिकताको भी नहीं खोता। आजका विज्ञान भी हमें बताता है कि जीव जो भी विचार करता है उसकी टेढ़ी-सीधी, उथली-गहरी रेखाएँ मस्तिष्कमें भरे हुए मक्खन जैसे श्वेत पदार्थ में खिंचती जाती है और उन्हीं के अनुसार स्मृति तथा वासनाएँ उबुद्ध होती हैं । जैन कर्म सिद्धान्त भी यही है कि-रागद्वेष प्रवृत्तिके कारण केवल संस्कार ही आत्मापर नहीं पड़ता किन्तु उस संस्कारको यथासमय उद्बुद्ध करानेवाले कर्मद्रव्यका संबंध भी होता जाता है। यह कर्मद्रव्य पुद्गल द्रव्य ही है । मन, वचन, कायकी प्रत्येक क्रियाके अनुसार शुक्ल या कृष्ण कर्म पुद्गल आत्मासे सम्बन्धको प्राप्त हो जाते हैं। ये विशेष प्रकारके कर्मपद्गल बहुत कुछ तो स्थूल शरीरके भीतर ही पड़े रहते हैं जो मनोभावोंके अनुसार आत्माके सूक्ष्म कर्मशरीरमें शामिल होते जाते हैं, कुछ बाहिरसे भी आते हैं। जैसे तपे हुए लोहेके गोलेको पानीसे भरे हुए बर्तनमें छोड़िये तो वह गोला जलके भरे हुए बहुतसे परमाणुओंको जिस तरह अपने भीतर सोख लेता है उसी तरह अपनी गरमी और भापसे बाहिरके परमाणुओंको भी खींचता है। लोहेका ४-२५ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70