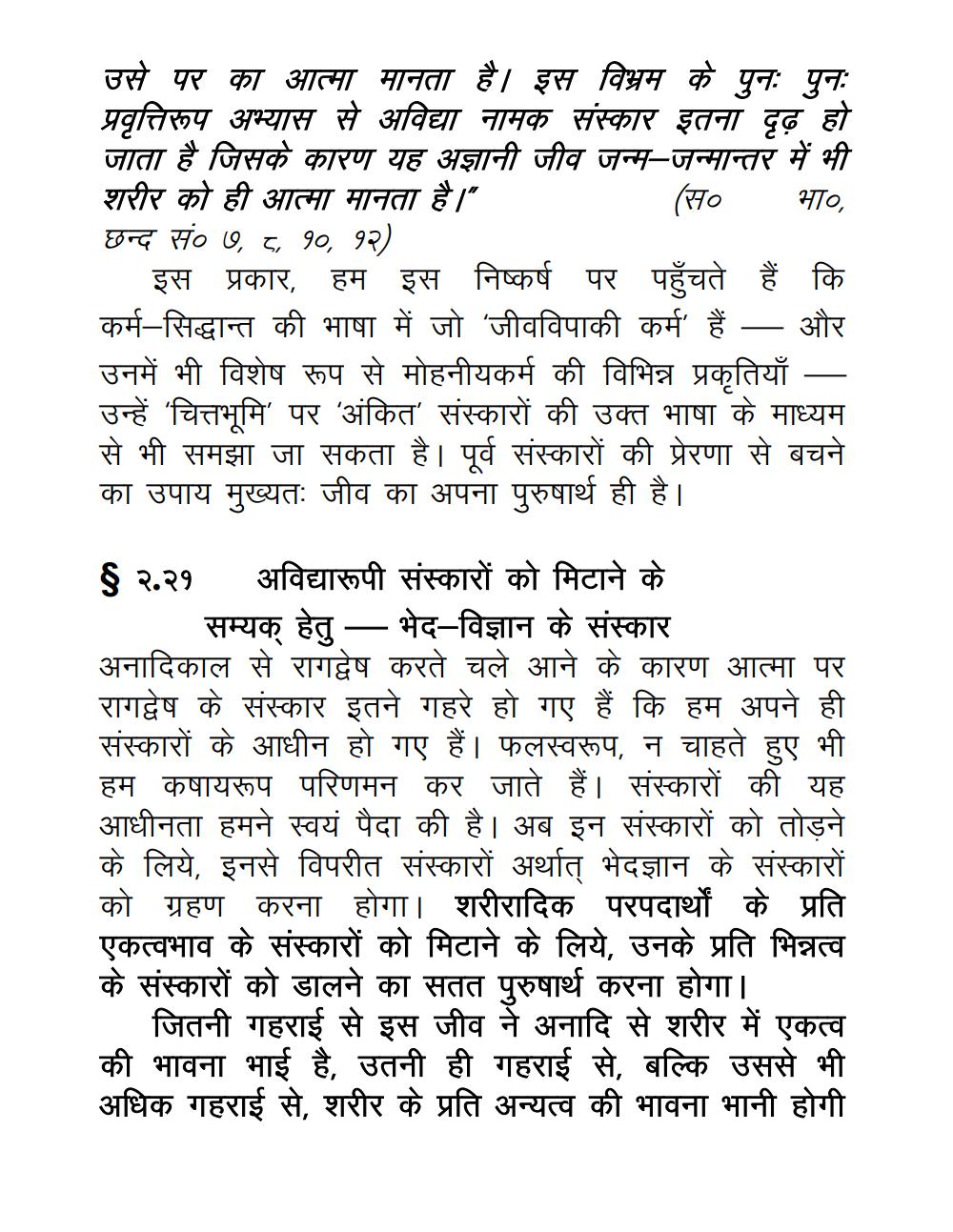Book Title: Mokshmarg ke Sandarbh me Nimitta ka Swarup Author(s): Babulal Publisher: Babulal View full book textPage 9
________________ उसे पर का आत्मा मानता है। इस विभ्रम के पुनः पुनः प्रवृत्तिरूप अभ्यास से अविद्या नामक संस्कार इतना दृढ़ हो जाता है जिसके कारण यह अज्ञानी जीव जन्म-जन्मान्तर में भी शरीर को ही आत्मा मानता है।" (स० भा०, छन्द सं० ७, ८, १०, १२) __इस प्रकार, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कर्म-सिद्धान्त की भाषा में जो 'जीवविपाकी कर्म' हैं – और उनमें भी विशेष रूप से मोहनीयकर्म की विभिन्न प्रकृतियाँ - उन्हें 'चित्तभूमि' पर 'अंकित' संस्कारों की उक्त भाषा के माध्यम से भी समझा जा सकता है। पूर्व संस्कारों की प्रेरणा से बचने का उपाय मुख्यतः जीव का अपना पुरुषार्थ ही है। ६ २.२१ अविद्यारूपी संस्कारों को मिटाने के सम्यक् हेतु — भेद-विज्ञान के संस्कार अनादिकाल से रागद्वेष करते चले आने के कारण आत्मा पर रागद्वेष के संस्कार इतने गहरे हो गए हैं कि हम अपने ही संस्कारों के आधीन हो गए हैं। फलस्वरूप, न चाहते हुए भी हम कषायरूप परिणमन कर जाते हैं। संस्कारों की यह आधीनता हमने स्वयं पैदा की है। अब इन संस्कारों को तोड़ने के लिये, इनसे विपरीत संस्कारों अर्थात् भेदज्ञान के संस्कारों को ग्रहण करना होगा। शरीरादिक परपदार्थों के प्रति एकत्वभाव के संस्कारों को मिटाने के लिये, उनके प्रति भिन्नत्व के संस्कारों को डालने का सतत पुरुषार्थ करना होगा। जितनी गहराई से इस जीव ने अनादि से शरीर में एकत्व की भावना भाई है, उतनी ही गहराई से, बल्कि उससे भी अधिक गहराई से, शरीर के प्रति अन्यत्व की भावना भानी होगीPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35