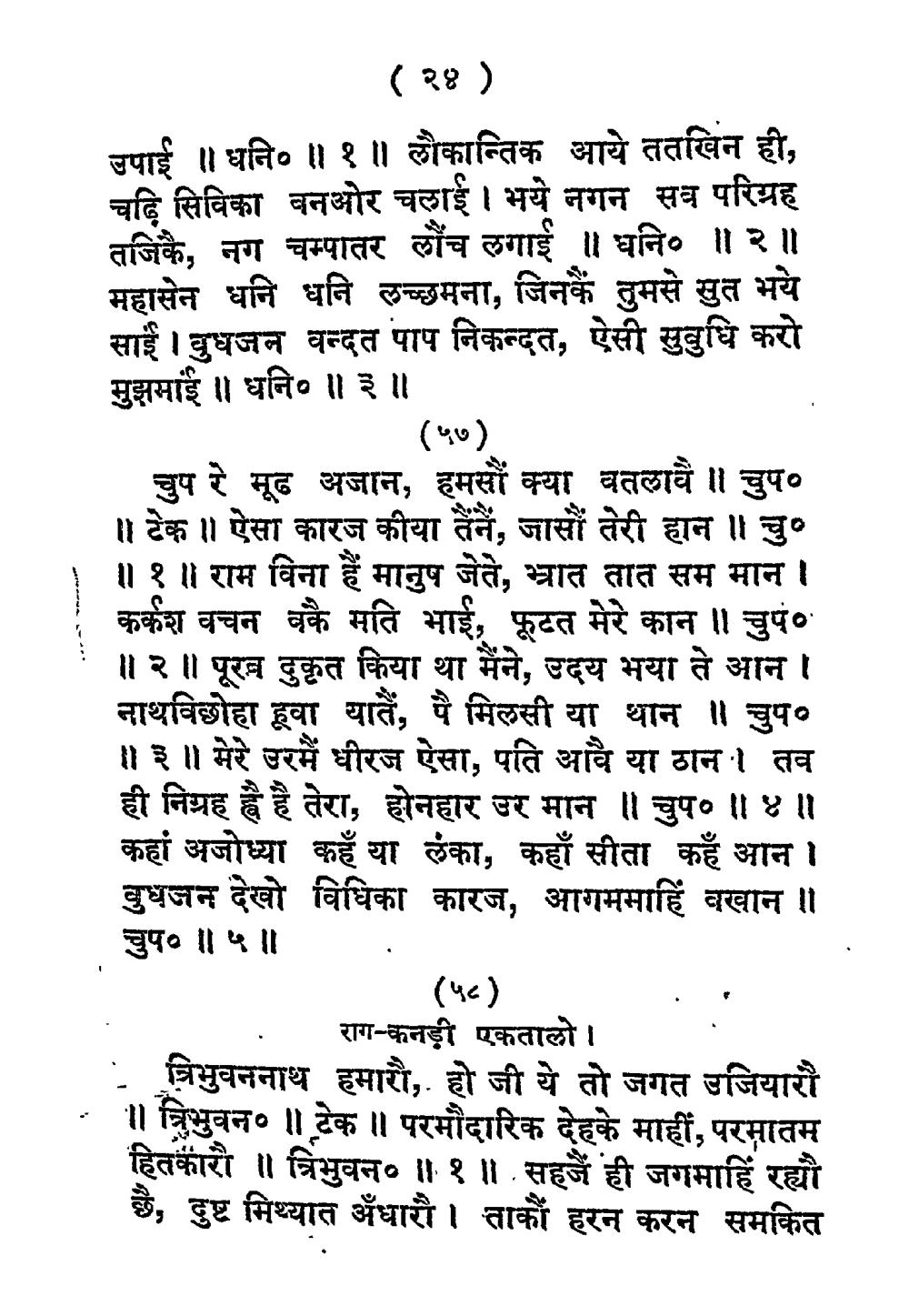Book Title: Jainpad Sangraha 01
Author(s): Nathuram Premi
Publisher: Jain Granth Ratnakar Karyalay
View full book text
________________
( २४ )
उपाई ॥ धनि० ॥ १ ॥ लौकान्तिक आये ततखिन ही, चढ़ि सिविका बनओर चलाई । भये नगन सब परिग्रह तजिकै, नग चम्पातर लौंच लगाई ॥ घनि० ॥२॥ महासेन धनि धनि लच्छमना, जिनकैं तुमसे सुत भये साईं । बुधजन वन्दत पाप निकन्दत, ऐसी सुबुधि करो मुझमाई ॥ धनि० ॥ ३ ॥
(५७)
चुप रे मूढ अजान, हमसौं क्या वतलावै ॥ चुप० ॥ टेक ॥ ऐसा कारज कीया तैंनें, जासौं तेरी हान ॥ चु० ॥ १ ॥ राम विना हैं मानुष जेते, भ्रात तात सम मान । कर्कश वचन वकै मति भाई, फूटत मेरे कान ॥ चुपं० ॥ २ ॥ पूरब दुकृत किया था मैंने, उदय भया ते आन । नाथविछोहा हूवा यातें, पै मिलसी या थान ॥ चुप० ॥ ३ ॥ मेरे उरमैं धीरज ऐसा, पति आवै या ठान । तव ही निग्रह है है तेरा, होनहार उर मान ॥ चुप० ॥ ४ ॥ कहां अजोध्या कहँ या लंका, कहाँ सीता कहँ आन । वुधजन देखो विधिका कारज, आगममाहिं बखान ॥ चुप० ॥ ५ ॥
(५८) राग - कनड़ी एकतालो ।
त्रिभुवननाथ हमारौ, हो जी ये तो जगत उजियारौ ॥ त्रिभुवन० ॥ टेक ॥ परमौदारिक देहके माहीं, परमातम हितकारी ॥ त्रिभुवन० ॥ १ ॥ सहजैं ही जगमाहिं रह्यौ छै, , दुष्ट मिथ्यात अंधारौ । ताकौं हरन करन समकित
.
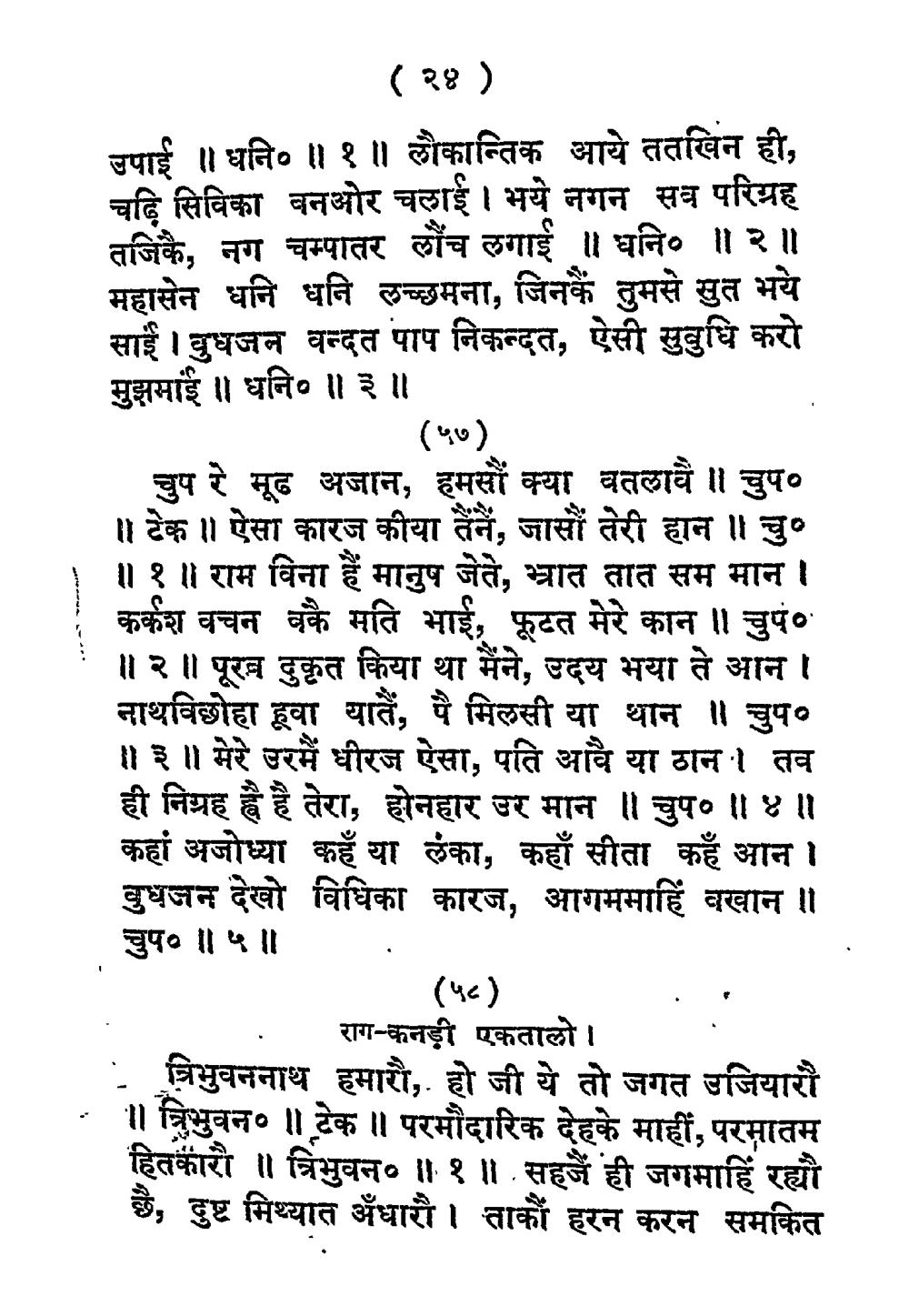
Page Navigation
1 ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253