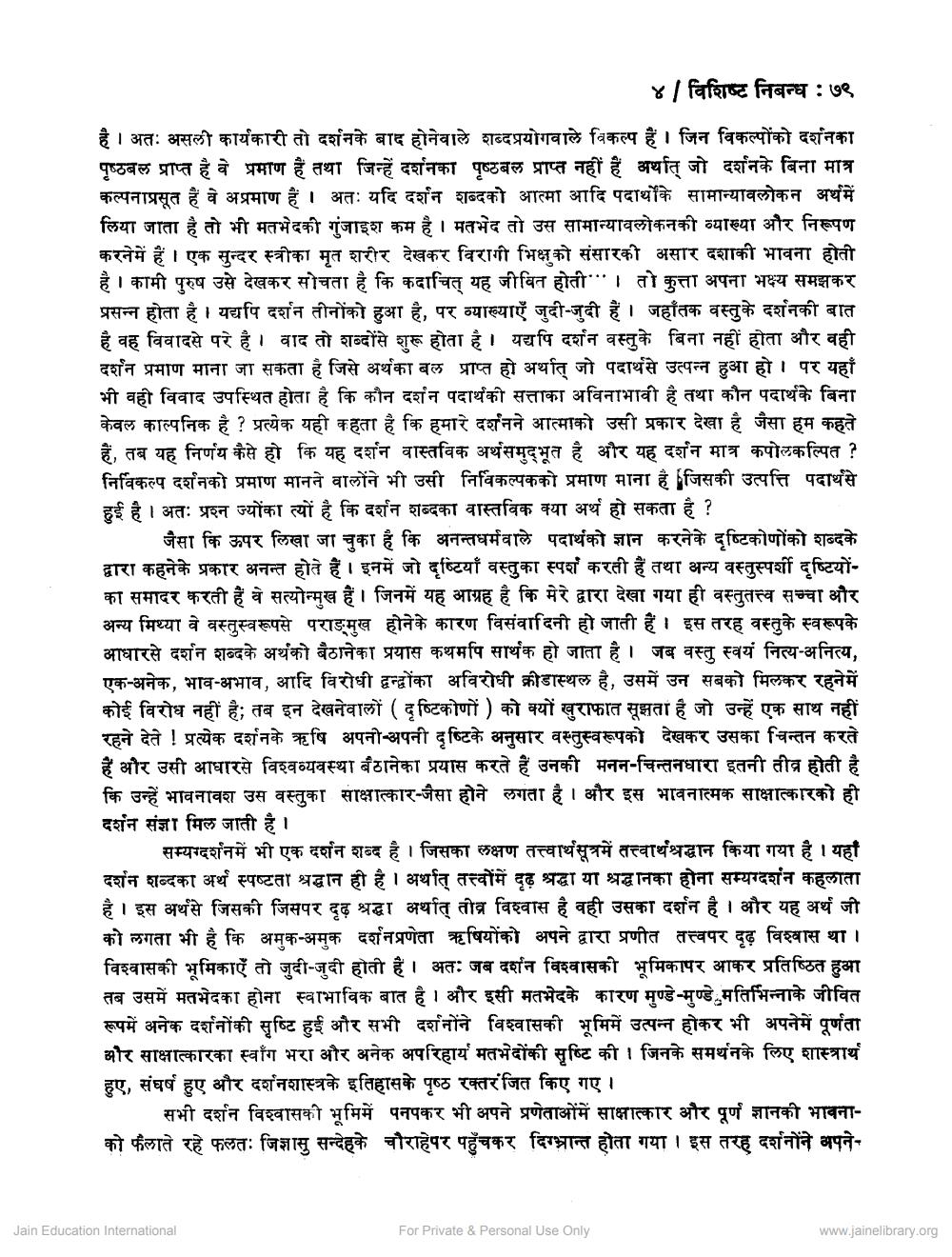Book Title: Nyayavinischay aur uska Vivechan Author(s): Publisher: Z_Mahendrakumar_Jain_Nyayacharya_Smruti_Granth_012005.pdf View full book textPage 6
________________ ४ / विशिष्ट निबन्ध : ७९ ह है । अतः असली कार्यकारी तो दर्शनके बाद होनेवाले शब्दप्रयोगवाले विकल्प हैं। जिन विकल्पोंको दर्शनका पृष्ठबल प्राप्त है वे प्रमाण हैं तथा जिन्हें दर्शनका पृष्ठबल प्राप्त नहीं हैं अर्थात् जो दर्शनके बिना मात्र कल्पनाप्रसूत हैं वे अप्रमाण हैं । अतः यदि दर्शन शब्दको आत्मा आदि पदार्थों के सामान्यावलोकन अर्थमें लिया जाता है तो भी मतभेदकी गुंजाइश कम है । मतभेद तो उस सामान्यावलोकनकी व्याख्या और निरूपण करने में हैं। एक सुन्दर स्त्रीका मृत शरीर देखकर विरागी भिक्षको संसारकी असार दशाकी भावना होती है। कामी पुरुष उसे देखकर सोचता है कि कदाचित यह जीवित होती । तो कुत्ता अपना भक्ष्य समझकर प्रसन्न होता है। यद्यपि दर्शन तीनोंको हआ है, पर व्याख्याएँ जुदी-जुदी है। जहाँतक वस्तुके दर्शनकी बात है वह विवादसे परे है। वाद तो शब्दोंसे शुरू होता है। यद्यपि दर्शन वस्तुके बिना नहीं होता और वही दर्शन प्रमाण माना जा सकता है जिसे अर्थका बल प्राप्त हो अर्थात् जो पदार्थसे उत्पन्न हुआ हो। पर यहाँ भी वही विवाद उपस्थित होता है कि कौन दर्शन पदार्थको सत्ताका अविनाभावी है तथा कौन पदार्थके बिना केवल काल्पनिक है ? प्रत्येक यही कहता है कि हमारे दर्शनने आत्माको उसी प्रकार देखा है जैसा हम कहते हैं, तब यह निर्णय कैसे हो कि यह दर्शन वास्तविक अर्थसमुद्भूत है और यह दर्शन मात्र कपोलकल्पित ? निर्विकल्प दर्शनको प्रमाण मानने वालोंने भी उसी निर्विकल्पकको प्रमाण माना है जिसकी उत्पत्ति पदार्थसे हुई है । अतः प्रश्न ज्योंका त्यों है कि दर्शन शब्दका वास्तविक क्या अर्थ हो सकता है ? जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि अनन्तधर्मवाले पदार्थको ज्ञान करनेके दृष्टिकोणोंको शब्दके द्वारा कहनेके प्रकार अनन्त होते हैं । इनमें जो दृष्टियाँ वस्तुका स्पर्श करती है तथा अन्य वस्तुस्पर्शी दृष्टियोंका समादर करती हैं वे सत्योन्मुख हैं। जिनमें यह आग्रह है कि मेरे द्वारा देखा गया ही वस्तुतत्त्व सच्चा और अन्य मिथ्या वे वस्तुस्वरूपसे पराङ्मुख होने के कारण विसंवादिनी हो जाती हैं। इस तरह वस्तुके स्वरूपके आधारसे दर्शन शब्दके अर्थको बैठानेका प्रयास कथमपि सार्थक हो जाता है। जब वस्तु स्वयं नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भाव-अभाव, आदि विरोधी द्वन्द्वोंका अविरोधी क्रीडास्थल है, उसमें उन सबको मिलकर रहने में कोई विरोध नहीं है; तब इन देखनेवालों ( दृष्टिकोणों) को क्यों खुराफात सूझता है जो उन्हें एक साथ नहीं रहने देते ! प्रत्येक दर्शनके ऋषि अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार वस्तुस्वरूपको देखकर उसका चिन्तन करते हैं और उसी आधारसे विश्वव्यवस्था बैठानेका प्रयास करते हैं उनकी मनन-चिन्तनधारा इतनी तीव्र होती है कि उन्हें भावनावश उस वस्तुका साक्षात्कार-जैसा होने लगता है। और इस भावनात्मक साक्षात्कारको ही दर्शन संज्ञा मिल जाती है। सम्यग्दर्शनमें भी एक दर्शन शब्द है । जिसका लक्षण तत्त्वार्थसूत्र में तत्त्वार्थश्रद्धान किया गया है । यहाँ दर्शन शब्दका अर्थ स्पष्टता श्रद्धान ही है । अर्थात् तत्त्वोंमें दृढ़ श्रद्धा या श्रद्धानका होना सम्यग्दर्शन कहलाता है । इस अर्थसे जिसकी जिसपर दृढ़ श्रद्धा अर्थात् तीव्र विश्वास है वही उसका दर्शन है । और यह अर्थ जी को लगता भी है कि अमुक-अमुक दर्शनप्रणेता ऋषियोंको अपने द्वारा प्रणीत तत्त्वपर दृढ़ विश्वास था। विश्वासकी भूमिकाएँ तो जुदी-जुदी होती है। अतः जब दर्शन विश्वासको भूमिकापर आकर प्रतिष्ठित हुआ तब उसमें मतभेदका होना स्वाभाविक बात है । और इसी मतभेदके कारण मुण्डे -मुण्डे मतिभिन्नाके जीवित रूपमें अनेक दर्शनोंकी सृष्टि हुई और सभी दर्शनोंने विश्वासकी भूमिमें उत्पन्न होकर भी अपनेमें पूर्णता और साक्षात्कारका स्वाँग भरा और अनेक अपरिहार्य मतभेदोंकी सृष्टि की । जिनके समर्थनके लिए शास्त्रार्थ हुए, संघर्ष हुए और दर्शनशास्त्रके इतिहासके पृष्ठ रक्तरंजित किए गए। सभी दर्शन विश्वासकी भूमिमें पनपकर भी अपने प्रणेताओंमें साक्षात्कार और पूर्ण ज्ञानकी भावनाको फैलाते रहे फलतः जिज्ञासु सन्देहके चौराहेपर पहुँचकर दिग्भ्रान्त होता गया । इस तरह दर्शनोंने अपने Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52