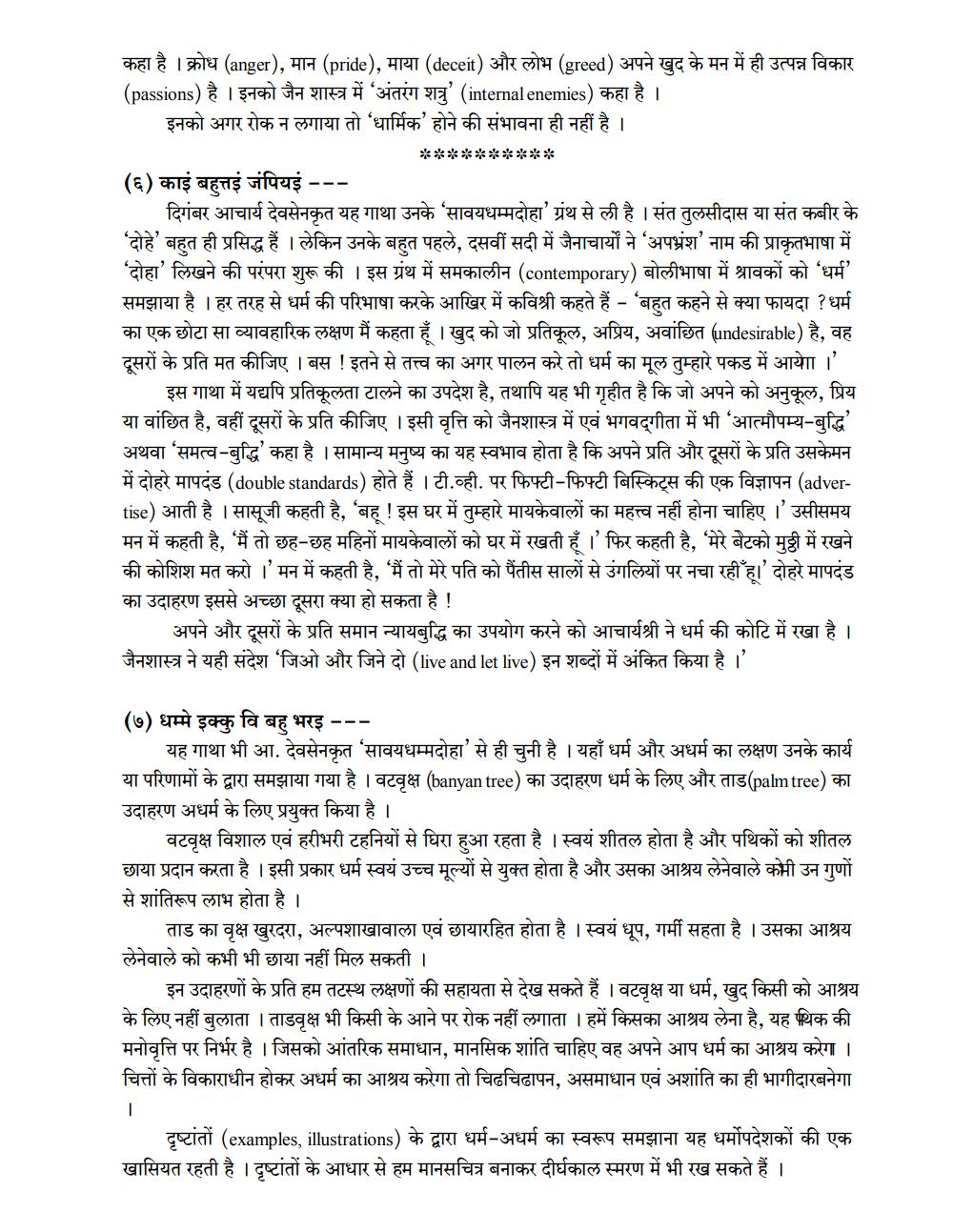Book Title: Jainology Parichaya 02 Author(s): Nalini Joshi Publisher: Sanmati Tirth Prakashan Pune View full book textPage 7
________________ कहा है । क्रोध (anger), मान (pride), माया (deceit) और लोभ (greed) अपने खुद के मन में ही उत्पन्न विकार (passions) है । इनको जैन शास्त्र में 'अंतरंग शत्रु' (internal enemies) कहा है । इनको अगर रोक न लगाया तो 'धार्मिक' होने की संभावना ही नहीं है । ********** (६) काइं बहुत्तई जंपियइं T दिगंबर आचार्य देवसेनकृत यह गाथा उनके 'सावयधम्मदोहा' ग्रंथ से ली है । संत तुलसीदास या संत कबीर के ‘दोहे' बहुत ही प्रसिद्ध हैं । लेकिन उनके बहुत पहले, दसवीं सदी में जैनाचार्यों ने 'अपभ्रंश' नाम की प्राकृतभाषा में 'दोहा' लिखने की परंपरा शुरू की । इस ग्रंथ में समकालीन (contemporary) बोलीभाषा में श्रावकों को 'धर्म' समझाया है । हर तरह से धर्म की परिभाषा करके आखिर में कविश्री कहते हैं - 'बहुत कहने से क्या फायदा ? धर्म का एक छोटा सा व्यावहारिक लक्षण मैं कहता हूँ । खुद को जो प्रतिकूल, अप्रिय, अवांछित (undesirable) है, वह दूसरों के प्रति मत कीजिए । बस ! इतने से तत्त्व का अगर पालन करे तो धर्म का मूल तुम्हारे पकड में आयेगा ।' इस गाथा में यद्यपि प्रतिकूलता टालने का उपदेश है, तथापि यह भी गृहीत है कि जो अपने को अनुकूल, प्रिय या वांछित है, वहीं दूसरों के प्रति कीजिए । इसी वृत्ति को जैनशास्त्र में एवं भगवद्गीता में भी 'आत्मौपम्य-बुद्धि' अथवा 'समत्व-बुद्धि' कहा है । सामान्य मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि अपने प्रति और दूसरों के प्रति उसके मन में दोहरे मापदंड (double standards) होते हैं । टी. व्ही. पर फिफ्टी-फिफ्टी बिस्किट्स की एक विज्ञापन (advertise) आती है । सासूजी कहती है, 'बहू ! इस घर में तुम्हारे मायकेवालों का महत्त्व नहीं होना चाहिए ।' उसीसमय मन में कहती है, ‘मैं तो छह-छह महिनों मायकेवालों को घर में रखती हूँ ।' फिर कहती है, 'मेरे बेटको मुठ्ठी में रखने की कोशिश मत करो ।' मन में कहती है, 'मैं तो मेरे पति को पैंतीस सालों से उंगलियों पर नचा रही हूँ ।' दोहरे मापदंड का उदाहरण इससे अच्छा दूसरा क्या हो सकता है ! अपने और दूसरों के प्रति समान न्यायबुद्धि का उपयोग करने को आचार्यश्री ने धर्म की कोटि में रखा है । जैनशास्त्र ने यही संदेश ‘जिओ और जिने दो ( live and let live) इन शब्दों में अंकित किया है ।' (७) धम्मे इक्कु वि बहु भरइ यह गाथा भी आ. देवसेनकृत 'सावयधम्मदोहा' से ही चुनी है । यहाँ धर्म और अधर्म का लक्षण उनके कार्य या परिणामों के द्वारा समझाया गया है । वटवृक्ष (banyan tree) का उदाहरण धर्म के लिए और ताड (palm tree) का उदाहरण अधर्म के लिए प्रयुक्त किया है । वटवृक्ष विशाल एवं हरीभरी टहनियों से घिरा हुआ रहता है । स्वयं शीतल होता है और पथिकों को शीतल छाया प्रदान करता है । इसी प्रकार धर्म स्वयं उच्च मूल्यों से युक्त होता है और उसका आश्रय लेनेवाले कमी उन गुणों से शांतिरूप लाभ होता है । ताड का वृक्ष खुरदरा, अल्पशाखावाला एवं छायारहित होता है । स्वयं धूप, गर्मी सहता है । उसका आश्रय लेनेवाले को कभी भी छाया नहीं मिल सकती । इन उदाहरणों के प्रति हम तटस्थ लक्षणों की सहायता से देख सकते हैं । वटवृक्ष या धर्म, खुद किसी को आश्रय के लिए नहीं बुलाता । ताडवृक्ष भी किसी के आने पर रोक नहीं लगाता । हमें किसका आश्रय लेना है, यह पथिक क मनोवृत्ति पर निर्भर है । जिसको आंतरिक समाधान, मानसिक शांति चाहिए वह अपने आप धर्म का आश्रय करेगा । चित्तों के विकाराधीन होकर अधर्म का आश्रय करेगा तो चिढचिढापन, असमाधान एवं अशांति का ही भागीदार बनेगा I दृष्टांतों (examples, illustrations) के द्वारा धर्म-अधर्म का स्वरूप समझाना यह धर्मोपदेशकों की एक खासियत रहती है । दृष्टांतों के आधार से हम मानसचित्र बनाकर दीर्घकाल स्मरण में भी रख सकते हैं ।Page Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41