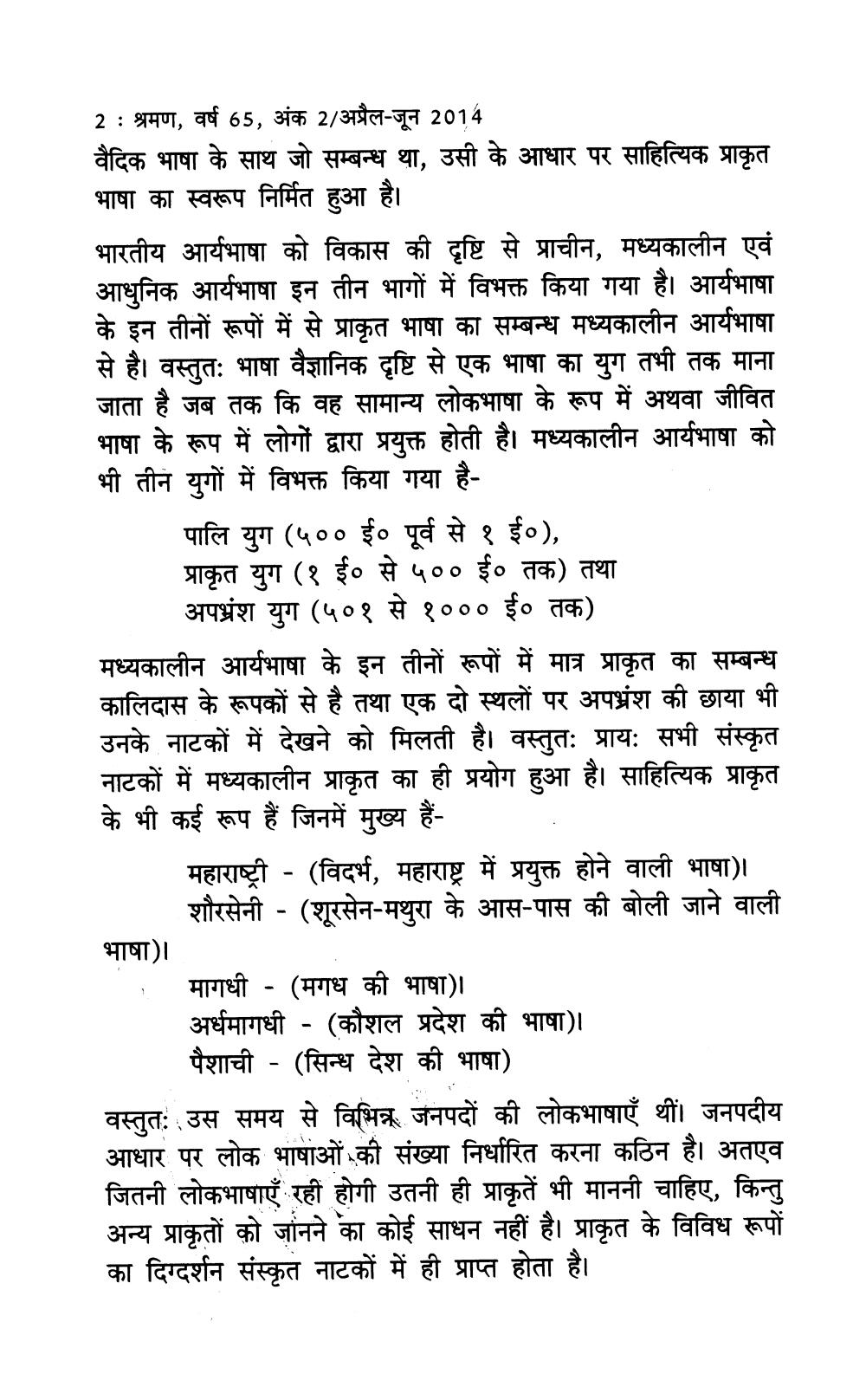Book Title: Sramana 2014 04 Author(s): Ashokkumar Singh, Rahulkumar Singh, Omprakash Singh Publisher: Parshvanath Vidhyashram Varanasi View full book textPage 7
________________ 2 : श्रमण, वर्ष 65, अंक 2/अप्रैल-जून 2014 वैदिक भाषा के साथ जो सम्बन्ध था, उसी के आधार पर साहित्यिक प्राकृत भाषा का स्वरूप निर्मित हुआ है। भारतीय आर्यभाषा को विकास की दृष्टि से प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक आर्यभाषा इन तीन भागों में विभक्त किया गया है। आर्यभाषा के इन तीनों रूपों में से प्राकृत भाषा का सम्बन्ध मध्यकालीन आर्यभाषा से है। वस्तुत: भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से एक भाषा का युग तभी तक माना जाता है जब तक कि वह सामान्य लोकभाषा के रूप में अथवा जीवित भाषा के रूप में लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है। मध्यकालीन आर्यभाषा को भी तीन युगों में विभक्त किया गया है पालि युग (५०० ई० पूर्व से १ ई०), प्राकृत युग (१ ई० से ५०० ई० तक) तथा अपभ्रंश युग (५०१ से १००० ई० तक) मध्यकालीन आर्यभाषा के इन तीनों रूपों में मात्र प्राकृत का सम्बन्ध कालिदास के रूपकों से है तथा एक दो स्थलों पर अपभ्रंश की छाया भी उनके नाटकों में देखने को मिलती है। वस्तुतः प्राय: सभी संस्कृत नाटकों में मध्यकालीन प्राकृत का ही प्रयोग हुआ है। साहित्यिक प्राकृत के भी कई रूप हैं जिनमें मुख्य हैं महाराष्ट्री - (विदर्भ, महाराष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा)। शौरसेनी - (शूरसेन-मथुरा के आस-पास की बोली जाने वाली भाषा)। मागधी - (मगध की भाषा)। अर्धमागधी - (कौशल प्रदेश की भाषा)। पैशाची - (सिन्ध देश की भाषा) वस्तुत: उस समय से विभिन्न जनपदों की लोकभाषाएँ थीं। जनपदीय आधार पर लोक भाषाओं की संख्या निर्धारित करना कठिन है। अतएव जितनी लोकभाषाएँ रही होगी उतनी ही प्राकृतें भी माननी चाहिए, किन्तु अन्य प्राकृतों को जानने का कोई साधन नहीं है। प्राकृत के विविध रूपों का दिग्दर्शन संस्कृत नाटकों में ही प्राप्त होता है।Page Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 98