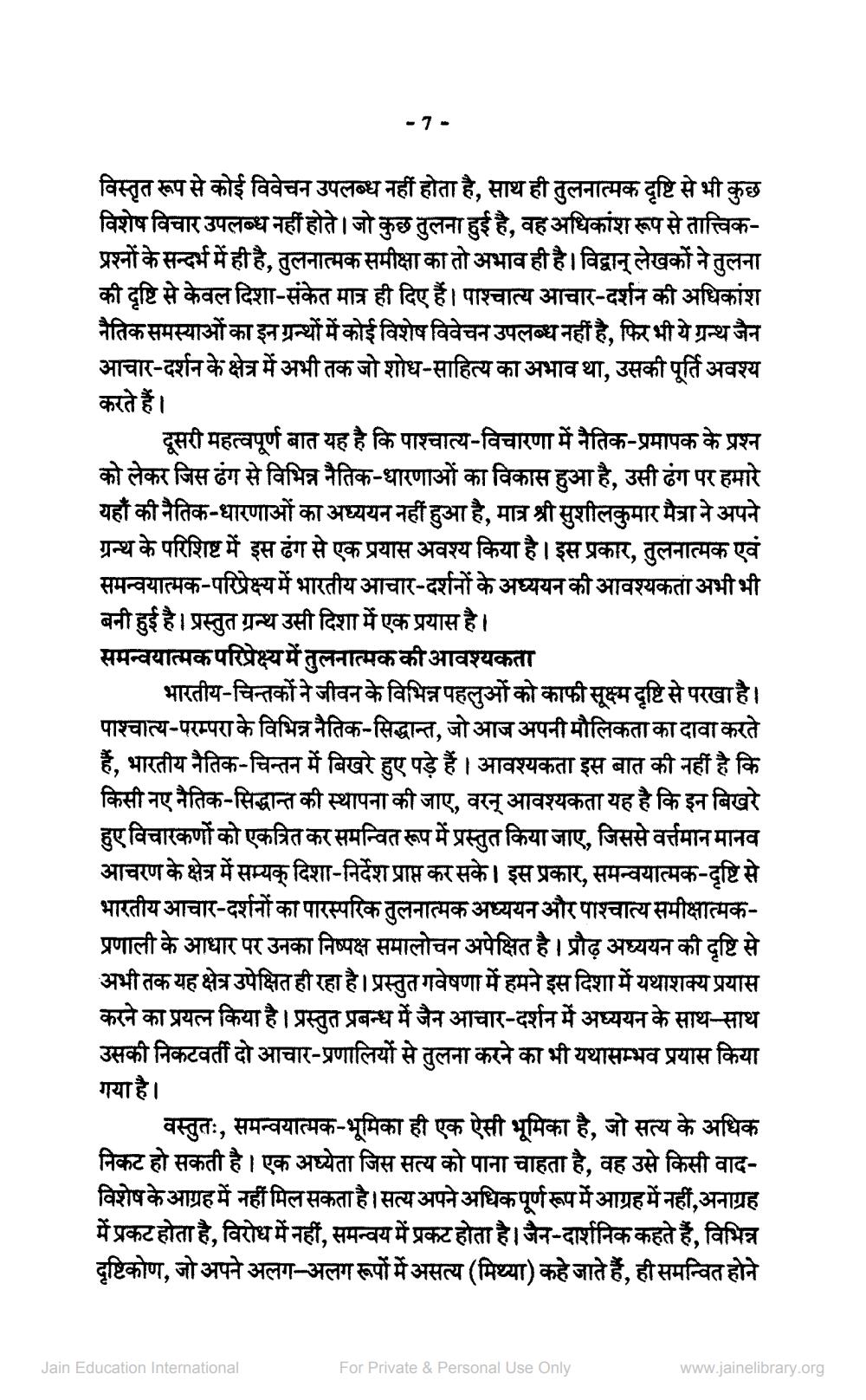Book Title: Bharatiya Achar Darshan Part 02 Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Prachya Vidyapith Shajapur View full book textPage 9
________________ -7. विस्तृत रूप से कोई विवेचन उपलब्ध नहीं होता है, साथ ही तुलनात्मक दृष्टि से भी कुछ विशेष विचार उपलब्ध नहीं होते। जो कुछ तुलना हुई है, वह अधिकांश रूप से तात्त्विकप्रश्नों के सन्दर्भ में ही है, तुलनात्मक समीक्षा का तो अभावही है। विद्वान् लेखकों ने तुलना की दृष्टि से केवल दिशा-संकेत मात्र ही दिए हैं। पाश्चात्य आचार-दर्शन की अधिकांश नैतिक समस्याओं का इन ग्रन्थों में कोई विशेष विवेचन उपलब्ध नहीं है, फिर भी ये ग्रन्थ जैन आचार-दर्शन के क्षेत्र में अभी तक जो शोध-साहित्य का अभाव था, उसकी पूर्ति अवश्य करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाश्चात्य-विचारणा में नैतिक-प्रमापक के प्रश्न को लेकर जिस ढंग से विभिन्न नैतिक-धारणाओं का विकास हुआ है, उसी ढंग पर हमारे यहाँ की नैतिक-धारणाओं का अध्ययन नहीं हुआ है, मात्र श्री सुशीलकुमार मैत्रा ने अपने ग्रन्थ के परिशिष्ट में इस ढंग से एक प्रयास अवश्य किया है। इस प्रकार, तुलनात्मक एवं समन्वयात्मक-परिप्रेक्ष्य में भारतीय आचार-दर्शनों के अध्ययन की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। प्रस्तुत ग्रन्थ उसी दिशा में एक प्रयास है। समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मककी आवश्यकता ___ भारतीय-चिन्तकों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को काफी सूक्ष्म दृष्टि से परखा है। पाश्चात्य-परम्परा के विभिन्न नैतिक-सिद्धान्त, जो आज अपनी मौलिकता का दावा करते हैं, भारतीय नैतिक-चिन्तन में बिखरे हुए पड़े हैं। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि किसी नए नैतिक-सिद्धान्त की स्थापना की जाए, वरन् आवश्यकता यह है कि इन बिखरे हुए विचारकणों को एकत्रित कर समन्वित रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे वर्तमान मानव आचरण के क्षेत्र में सम्यक् दिशा-निर्देश प्राप्त कर सके। इस प्रकार, समन्वयात्मक-दृष्टि से भारतीय आचार-दर्शनों का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन और पाश्चात्य समीक्षात्मकप्रणाली के आधार पर उनका निष्पक्ष समालोचन अपेक्षित है। प्रौढ़ अध्ययन की दृष्टि से अभी तक यह क्षेत्र उपेक्षित ही रहा है। प्रस्तुत गवेषणा में हमने इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करने का प्रयत्न किया है। प्रस्तुत प्रबन्ध में जैन आचार-दर्शन में अध्ययन के साथ-साथ उसकी निकटवर्ती दो आचार-प्रणालियों से तुलना करने का भी यथासम्भव प्रयास किया गया है। वस्तुतः, समन्वयात्मक भूमिका ही एक ऐसी भूमिका है, जो सत्य के अधिक निकट हो सकती है। एक अध्येता जिस सत्य को पाना चाहता है, वह उसे किसी वादविशेष के आग्रह में नहीं मिलसकता है।सत्य अपने अधिक पूर्णरूप में आग्रहमें नहीं,अनाग्रह में प्रकट होता है, विरोध में नहीं, समन्वय में प्रकट होता है। जैन-दार्शनिक कहते हैं, विभिन्न दृष्टिकोण, जो अपने अलग-अलग रूपों में असत्य (मिथ्या) कहे जाते हैं, ही समन्वित होने Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 568