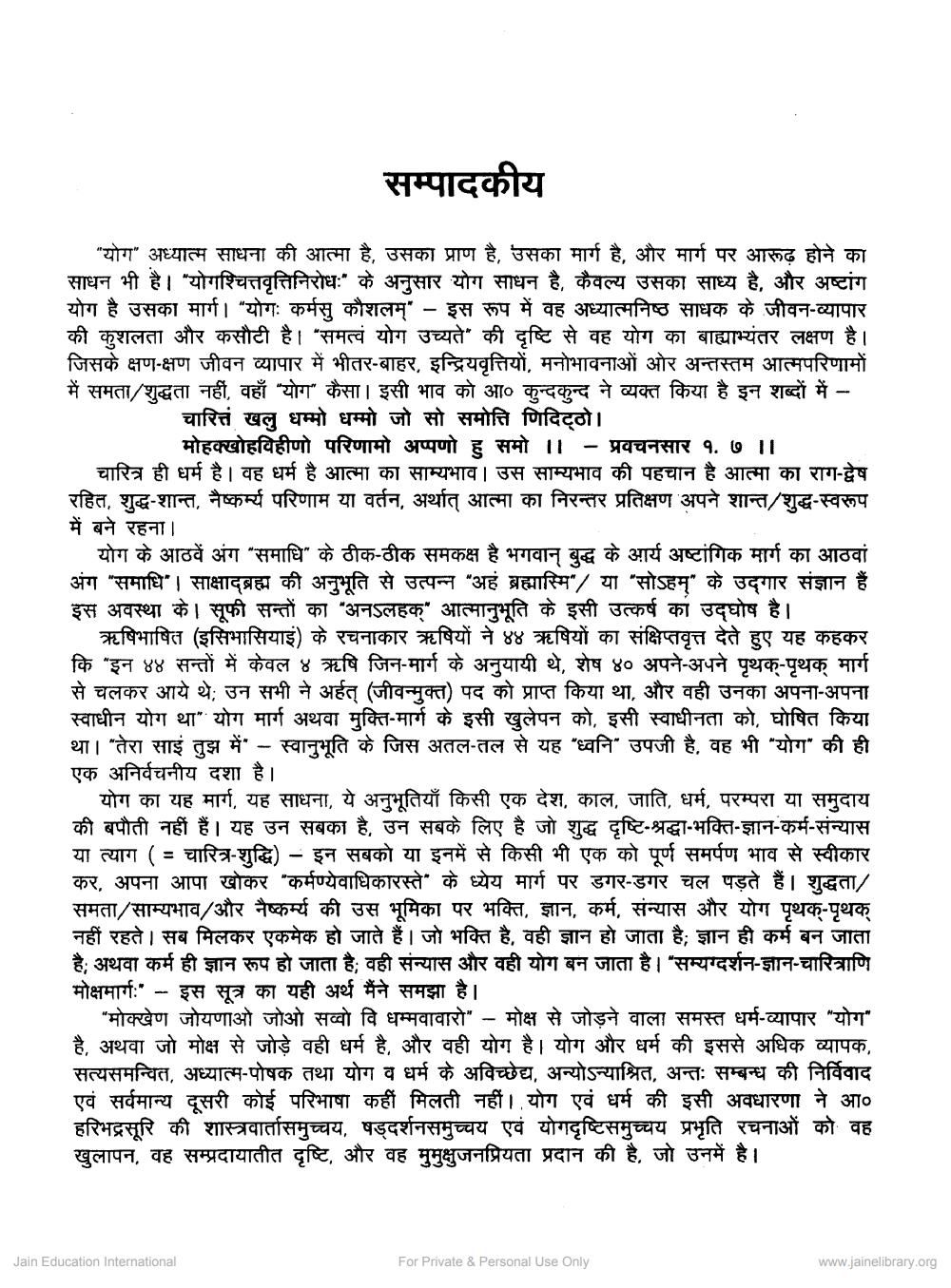Book Title: Patanjalyoga evam Jainyoga ka Tulnatmak Adhyayana Author(s): Aruna Anand Publisher: B L Institute of Indology View full book textPage 9
________________ सम्पादकीय चा "योग" अध्यात्म साधना की आत्मा है, उसका प्राण है, उसका मार्ग है, और मार्ग पर आरूढ होने का साधन भी है। “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः के अनुसार योग साधन है, कैवल्य उसका साध्य है, और अष्टांग योग है उसका मार्ग। “योगः कर्मसु कौशलम् - इस रूप में वह अध्यात्मनिष्ठ साधक के जीवन-व्यापार की कुशलता और कसौटी है। “समत्वं योग उच्यते” की दृष्टि से वह योग का बाह्याभ्यंतर लक्षण है। जिसके क्षण-क्षण जीवन व्यापार में भीतर-बाहर, इन्द्रियवृत्तियों, मनोभावनाओं ओर अन्तस्तम आत्मपरिणामों में समता/शुद्धता नहीं, वहाँ “योग” कैसा। इसी भाव को आo कुन्दकुन्द ने व्यक्त किया है इन शब्दों में - चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिदिट्ठो। मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो || - प्रवचनसार १. ७ ।। __ चारित्र ही धर्म है। वह धर्म है आत्मा का साम्यभाव । उस साम्यभाव की पहचान है आत्मा का राग-द्वेष रहित, शुद्ध-शान्त, नैष्कर्म्य परिणाम या वर्तन, अर्थात् आत्मा का निरन्तर प्रतिक्षण अपने शान्त/शुद्ध-स्वरूप में बने रहना। योग के आठवें अंग "समाधि के ठीक-ठीक समकक्ष है भगवान बद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग का आठवां अंग "समाधि। साक्षादब्रह्म की अनुभूति से उत्पन्न “अहं ब्रह्मास्मि / या “सोऽहम् के उद्गार संज्ञान हैं इस अवस्था के। सूफी सन्तों का "अनऽलहक आत्मानुभूति के इसी उत्कर्ष का उदघोष है। __ ऋषिभाषित (इसिभासियाई) के रचनाकार ऋषियों ने ४४ ऋषियों का संक्षिप्तवृत्त देते हुए यह कहकर कि “इन ४४ सन्तों में केवल ४ ऋषि जिन-मार्ग के अनुयायी थे, शेष ४० अपने-अपने पृथक्-पृथक् मार्ग से चलकर आये थे; उन सभी ने अर्हत् (जीवन्मुक्त) पद को प्राप्त किया था, और वही उनका अपना-अपना स्वाधीन योग था” योग मार्ग अथवा मुक्ति-मार्ग के इसी खुलेपन को, इसी स्वाधीनता को, घोषित किया था। “तेरा साइं तुझ में" - स्वानुभूति के जिस अतल-तल से यह "ध्वनि उपजी है, वह भी “योग' की ही एक अनिर्वचनीय दशा है। योग का यह मार्ग, यह साधना, ये अनुभूतियाँ किसी एक देश, काल, जाति, धर्म, परम्परा या समुदाय की बपौती नहीं हैं। यह उन सबका है, उन सबके लिए है जो शुद्ध दृष्टि-श्रद्धा-भक्ति-ज्ञान-कर्म-संन्यास या त्याग ( = चारित्र-शुद्धि)- इन सबको या इनमें से किसी भी एक को पूर्ण समर्पण भाव से स्वीकार कर, अपना आपा खोकर "कर्मण्येवाधिकारस्ते के ध्येय मार्ग पर डगर-डगर चल पड़ते हैं। शुद्धता/ समता/साम्यभाव/और नैष्कर्म्य की उस भूमिका पर भक्ति, ज्ञान, कर्म, संन्यास और योग पृथक-पृथक नहीं रहते। सब मिलकर एकमेक हो जाते हैं। जो भक्ति है, वही ज्ञान हो जाता है; ज्ञान ही कर्म बन जाता है; अथवा कर्म ही ज्ञान रूप हो जाता है; वही संन्यास और वही योग बन जाता है। “सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः - इस सूत्र का यही अर्थ मैंने समझा है। ___ “मोक्खेण जोयणाओ जोओ सव्वो वि धम्मवावारो” – मोक्ष से जोड़ने वाला समस्त धर्म-व्यापार "योग" है, अथवा जो मोक्ष से जोड़े वही धर्म है, और वही योग है। योग और धर्म की इससे अधिक व्यापक, सत्यसमन्वित, अध्यात्म-पोषक तथा योग व धर्म के अविच्छेद्य, अन्योऽन्याश्रित, अन्तः सम्बन्ध की निर्विवाद एवं सर्वमान्य दूसरी कोई परिभाषा कहीं मिलती नहीं। योग एवं धर्म की इसी अवधारणा ने आ० हरिभद्रसूरि की शास्त्रवार्तासमुच्चय, षड्दर्शनसमुच्चय एवं योगदृष्टिसमुच्चय प्रभृति रचनाओं को वह खुलापन, वह सम्प्रदायातीत दृष्टि, और वह मुमुक्षुजनप्रियता प्रदान की है, जो उनमें है। ताहा Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 350