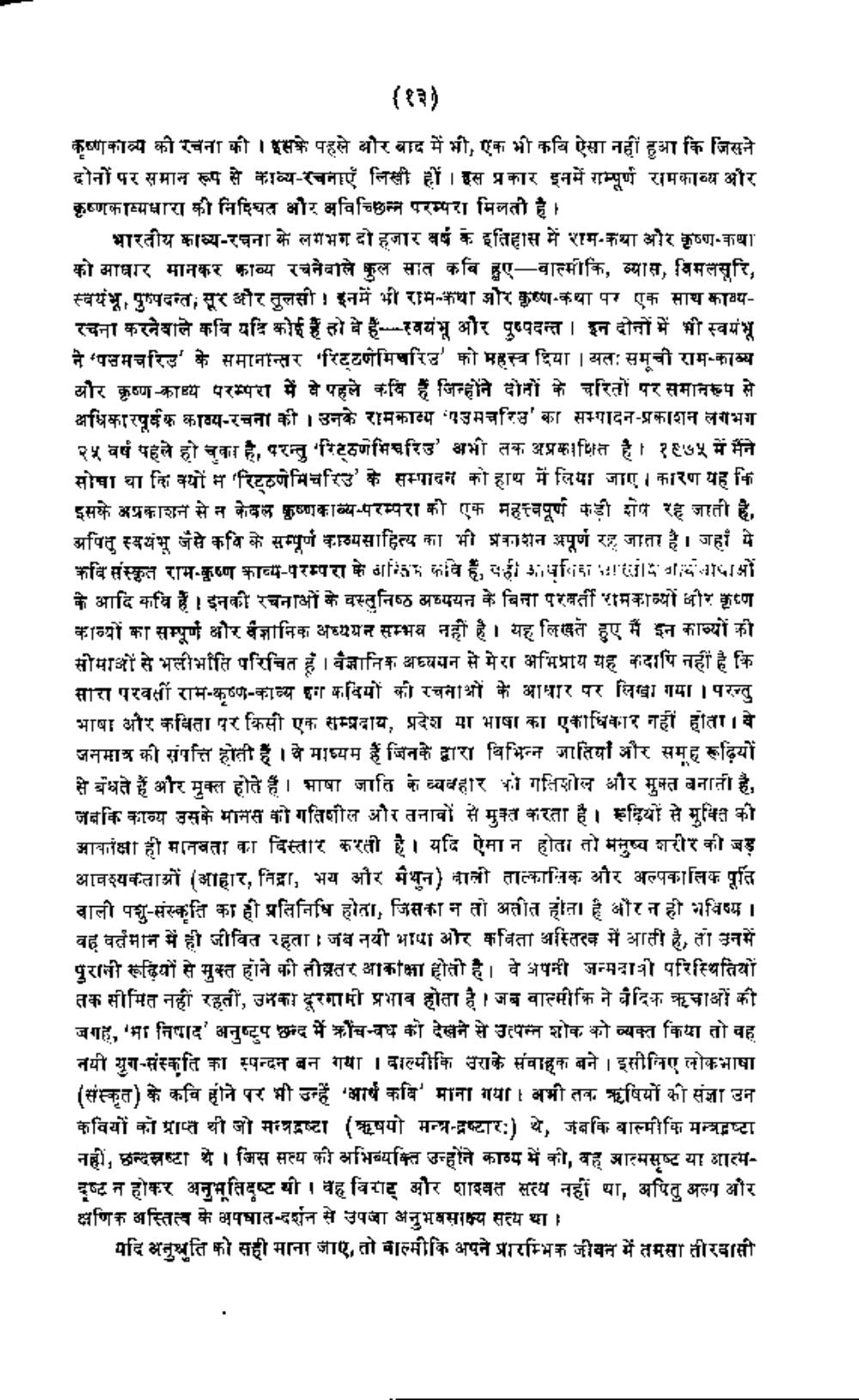Book Title: Ritthnemichariu Author(s): Sayambhu, Devendra Kumar Jain Publisher: Bharatiya Gyanpith View full book textPage 8
________________ {१३) कृष्णकाव्य की रचना की । इसके पहले और बाद में भी, एक भी कवि ऐसा नहीं हुआ कि जिसने दोनों पर समान रूप से काव्य-रचनाएँ लिखी हौं । इस प्रकार इनमें सम्पूर्ण रामकाव्य और कृष्णकाव्यधारा की निश्चित और अविच्छिन्न परम्परा मिलती है। भारतीय काव्य-रचना के लगभग दो हजार वर्ष के इतिहास में राम-कथा और कृष्ण-कथा को आधार मानकर काव्य रचनेवाले कुल सात कवि हुए-वाल्मीकि, व्यास, विमलसूरि, स्वयंभू, पुष्पदन्त; सूर और तुलसी। इनमें भी राम कथा और कृष्ण कथा पर एक साथ काव्यरचना करनेवाले कवि यदि कोई है तो वे हैं- स्वयंभू और पुष्पदन्त । इन दोनों में भी स्वयंभू ने 'पसमचरिउ' के समानान्सर 'रिटणेमिपरिट' को महस्व दिया । यतः समूची राम-काव्य और कृष्ण-काध्य परम्परा में वे पहले कवि हैं जिन्होंने दोनों के चरितों पर समानरूप से अधिकारपूर्वक काव्य-रचना की। उनके रामकाव्य उमचरित' का सम्पादन-प्रकाशन लगभग २५ वर्ष पहले हो चुका है, परन्तु 'रिटवणेमिचरिउ' अभी तक अप्रकाशित है। १६७५ में मैंने सोचा था कि क्यों न 'रिट्ठणेमिचरिउ' के सम्पादन को हाथ में लिया जाए । कारण यह कि इसके अप्रकाशन से न केवल कृष्णकाव्य-परम्परा की एक महत्वपूर्ण कड़ी शेष रह जाती है, अपितु स्वयंभु जैसे कवि के सम्पूर्ण काव्यसाहित्य का भी प्रकाशन अपूर्ण रह जाता है। जहाँ ये कदि संस्कृत राम-कृष्ण काव्य-परम्परा के अति कवि है, यही अपलिका वादाओं के आदि कवि हैं। इनकी रचनाओं के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के बिना परवर्ती रामकाव्यों और कृष्ण काव्यों का सम्पूर्ण और वैज्ञानिक अध्ययन सम्भव नहीं है। यह लिखते हुए मैं इन काव्यों की सोमाओं से भलीभांति परिचित हूँ । वैज्ञानिक अध्ययन से मेरा अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि सारा परवीं राम-कृष्ण-काव्य इन कवियों की रचनाओं के आधार पर लिखा गया । परन्तु भाषा और कविता पर किसी एक सम्प्रदाय, प्रदेश या भाषा का एकाधिकार नहीं होता। वे जनमात्र की संपत्ति होती हैं । ये माध्यम हैं जिनके द्वारा विभिन्न जातियों और समुह रूढ़ियों से बंधते हैं और मुक्त होते हैं। भाषा जाति के व्यवहार को गतिशील और मुक्त बनाती है, जबकि कान्य उसके मानस को गतिशील और तनावों से मुक्त करता है। सदियों से मुक्ति की गावांक्षा ही मानवता का विस्तार करती है। यदि ऐमा न होता तो मनुष्य शरीर की जड़ आवश्यकताओं (आहार, निद्रा, भय और मैथुन) बाली तात्कालिक और अल्पकालिक पूर्ति वाली पशु-संस्कृति का ही प्रतिनिधि होता, जिसका न तो अतीत होता है और न ही भविष्य । वह वर्तमान में ही जीवित रहता। जब नयी भाषा और कविता अस्तित्व में आती है, तो उनमें पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होने की तीव्रतर आकाक्षा होती है। वे अपनी जन्मदात्री परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहतीं, उनका दूरगामी प्रभाव होता है। जब वाल्मीकि ने वैदिक ऋचाओं की जगहें, 'भा निष्पाद' अनुष्टुप छन्द में क्रौंच-वध को देखने से उत्पन्न शोक को व्यक्त किया तो वह नयी युग-संस्कृति का स्पन्दन बन गया । वाल्मीकि उसके संवाहक बने । इसीलिए लोकभाषा (संस्कृत) के कवि होने पर भी उन्हें 'आर्ष कवि' माना गया । अभी तक ऋषियों की संज्ञा उन कवियों को प्राप्त थी जो मन्त्रद्रष्टा (ऋषयो मन्त्र-द्रष्टारः) थे, जबकि वाल्मीकि मन्त्रद्रष्टा नहीं, छन्दस्रष्टा थे। जिस सत्य की अभिव्यक्ति उन्होंने काव्य में को, वह आत्मसृष्ट या आत्मदृष्ट न होकर अनुभूतिदृष्ट यी । वह विराट् और शाश्वत सत्य नहीं था, अपितु अल्प और क्षणिक अस्तित्व के अपघात-दर्शन से उपजा अनुभवसाक्ष्य सत्य था। यदि अनुश्रुति को सही माना जाए, तो वाल्मीकि अपने प्रारम्भिक जीवन में तमसा तीरवासीPage Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 204