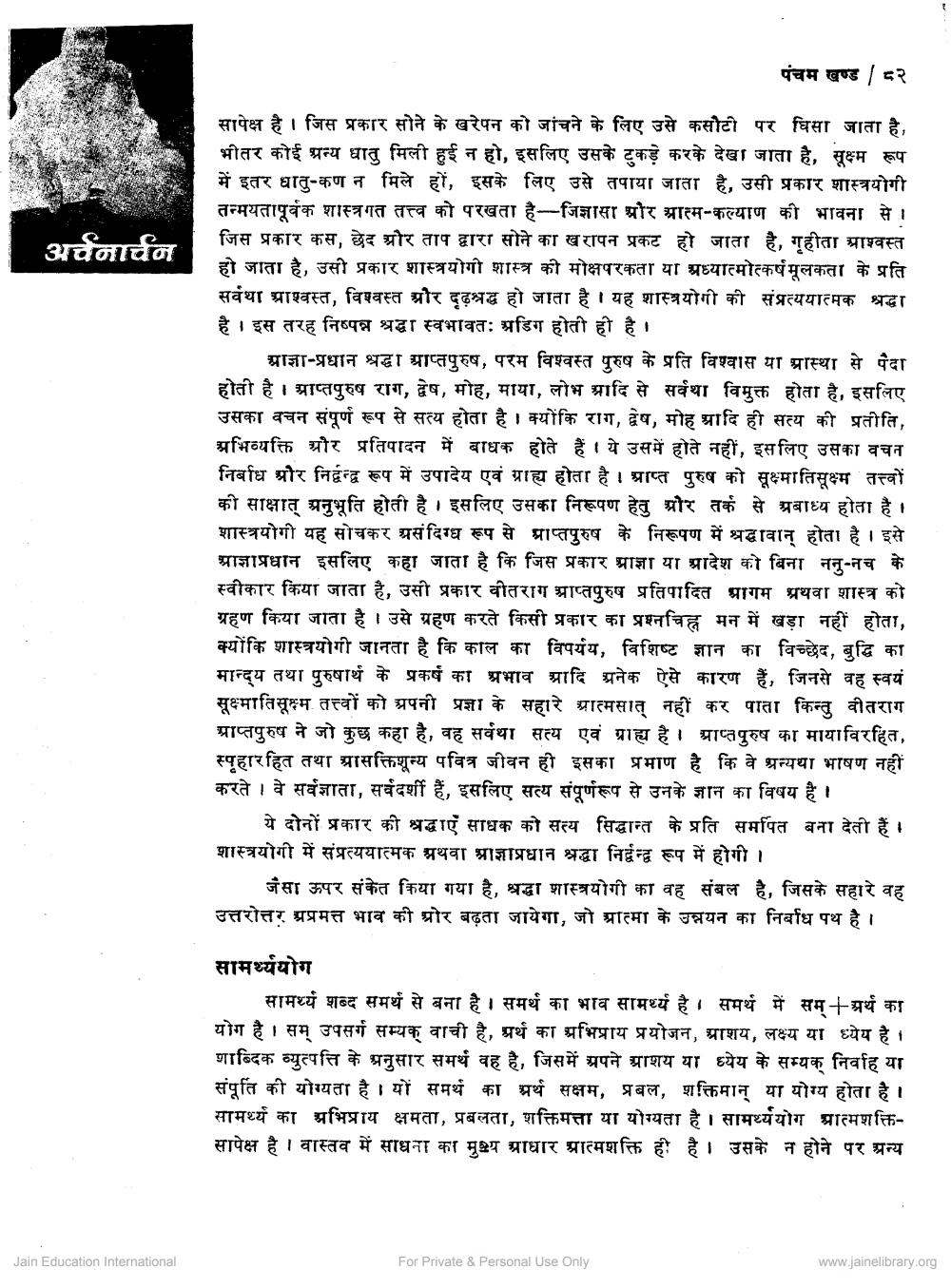Book Title: Yoga drushtti samucchay ek Vishleshan Author(s): C L Shastri Publisher: Z_Umravkunvarji_Diksha_Swarna_Jayanti_Smruti_Granth_012035.pdf View full book textPage 9
________________ अर्चनार्चन Jain Education International पंचम खण्ड / ८२ सापेक्ष है । जिस प्रकार सोने के खरेपन को जांचने के लिए उसे कसौटी पर घिसा जाता है, भीतर कोई अन्य धातु मिली हुई न हो, इसलिए उसके टुकड़े करके देखा जाता है, सूक्ष्म रूप में इतर धातु कण न मिले हों, इसके लिए उसे तपाया जाता है, उसी प्रकार शास्त्रयोगी तन्मयतापूर्वक शास्त्रगत तत्त्व को परखता है- जिज्ञासा और भ्रात्म-कल्याण की भावना से जिस प्रकार कस, छेद और ताप द्वारा सोने का खरापन प्रकट हो जाता है, गृहीता भाश्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार शास्त्रयोगी शास्त्र की मोक्षपरकता या अध्यात्मोत्कर्षमूलकता के प्रति सर्वथा प्राश्वस्त, विश्वस्त और दृढ़श्रद्ध हो जाता है । यह शास्त्रयोगी की संप्रत्ययात्मक श्रद्धा है। इस तरह निष्पन्न श्रद्धा स्वभावतः अडिग होती ही है। आज्ञा-प्रधान श्रद्धा श्राप्तपुरुष, परम विश्वस्त पुरुष के प्रति विश्वास या श्रास्था से पैदा होती है । प्राप्तपुरुष राग, द्वेष, मोह, माया, लोभ आदि से सर्वथा विमुक्त होता है, इसलिए उसका वचन संपूर्ण रूप से सत्य होता है क्योंकि राग, द्वेष, मोह आदि ही सत्य की प्रतीति, अभिव्यक्ति पर प्रतिपादन में बाधक होते हैं। ये उसमें होते नहीं, इसलिए उसका वचन निर्वाध और निर्द्वन्द्र रूप में उपादेय एवं प्राह्य होता है। प्राप्त पुरुष को सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्वों की साक्षात् मनुभूति होती है। इसलिए उसका निरूपण हेतु और तर्क से प्रवाध्य होता है । शास्त्रयोगी यह सोचकर संदिग्ध रूप से प्राप्तपुरुष के निरूपण में श्रद्धावान् होता है। इसे श्राज्ञाप्रधान इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार श्राज्ञा या प्रदेश को बिना ननु नच के स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार वीतराग प्राप्तपुरुष प्रतिपादित श्रागम श्रथवा शास्त्र को ग्रहण किया जाता है। उसे ग्रहण करते किसी प्रकार का प्रश्नचिह्न मन में खड़ा नहीं होता, क्योंकि शास्त्रयोगी जानता है कि काल का विपर्यय, विशिष्ट ज्ञान का विच्छेद, बुद्धि का मान्य तथा पुरुषार्थ के प्रकर्ष का प्रभाव आदि अनेक ऐसे कारण हैं, जिनसे वह स्वयं सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्वों को अपनी प्रशा के सहारे ग्रात्मसात् नहीं कर पाता किन्तु वीतराग प्राप्तपुरुष ने जो कुछ कहा है, वह सर्वथा सत्य एवं प्राह्य है प्राप्तपुरुष का मायाविरहित, स्पृहारहित तथा प्रासक्तिशून्य पवित्र जीवन ही इसका प्रमाण है कि वे श्रन्यथा भाषण नहीं करते। वे सर्वज्ञाता सर्वदर्शी हैं, इसलिए सत्य संपूर्णरूप से उनके ज्ञान का विषय है। ये दोनों प्रकार की श्रद्धाएँ साधक को सत्य सिद्धान्त के प्रति समर्पित बना देती है । शास्त्रयोगी में संप्रत्ययात्मक अथवा प्राज्ञाप्रधान श्रद्धा निर्द्वन्द्र रूप में होगी । जैसा ऊपर संकेत किया गया है, बडा शास्त्रयोगी का वह संबल है, जिसके सहारे वह उत्तरोत्तर प्रप्रमत्त भाव की घोर बढ़ता जायेगा, जो म्रात्मा के उन्नयन का निर्वाध पथ है। सामर्थ्ययोग सामर्थ्य शब्द समर्थ से बना है। समर्थ का भाव सामर्थ्य है। समर्थ में सम् + अर्थ का योग है। सम् उपसर्ग सम्यक् वाची है, अर्थ का अभिप्राय प्रयोजन, आशय, लक्ष्य या ध्येय है । शाब्दिक व्युत्पत्ति के अनुसार समर्थ वह है, जिसमें अपने आशय या ध्येय के सम्यक् निर्वाह या संपूति की योग्यता है। यों समर्थ का अर्थ सक्षम, प्रबल, शक्तिमान् या योग्य होता है। सामर्थ्य का अभिप्राय क्षमता, प्रबलता, शक्तिमत्ता या योग्यता है। सामर्थ्ययोग प्रात्मशक्तिसापेक्ष है। वास्तव में साधना का मुख्य आधार श्रात्मशक्ति ही है। उसके न होने पर अन्य For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25