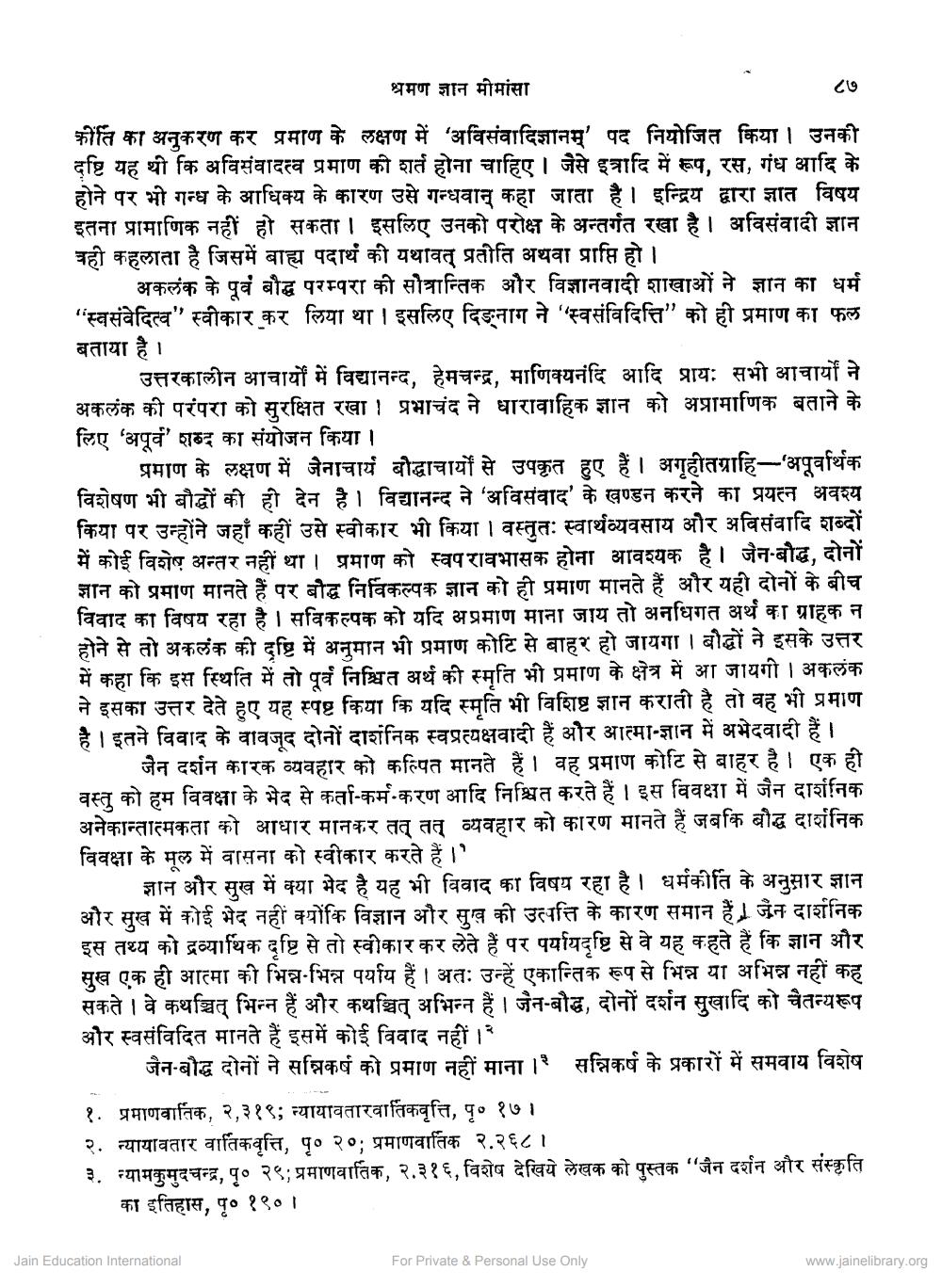Book Title: Shraman Gyan Mimansa Author(s): Bhagchandra Jain Publisher: Z_Aspect_of_Jainology_Part_3_Pundit_Dalsukh_Malvaniya_012017.pdf View full book textPage 2
________________ श्रमण ज्ञान मीमांसा ८७ ८७ कीति का अनुकरण कर प्रमाण के लक्षण में 'अविसंवादिज्ञानम्' पद नियोजित किया। उनकी दष्टि यह थी कि अविसंवादत्व प्रमाण की शर्त होना चाहिए। जैसे इत्रादि में रूप, रस, गंध आदि के होने पर भी गन्ध के आधिक्य के कारण उसे गन्धवान् कहा जाता है। इन्द्रिय द्वारा ज्ञात विषय इतना प्रामाणिक नहीं हो सकता। इसलिए उनको परोक्ष के अन्तर्गत रखा है। अविसंवादी ज्ञान वही कहलाता है जिसमें बाह्य पदार्थ की यथावत् प्रतीति अथवा प्राप्ति हो। अकलंक के पूर्व बौद्ध परम्परा की सौत्रान्तिक और विज्ञानवादी शाखाओं ने ज्ञान का धर्म "स्वसंवेदित्व" स्वीकार कर लिया था । इसलिए दिङ्नाग ने 'स्वसंविदित्ति" को ही प्रमाण का फल बताया है। उत्तरकालीन आचार्यों में विद्यानन्द, हेमचन्द्र, माणिक्यनंदि आदि प्रायः सभी आचार्यों ने अकलंक की परंपरा को सुरक्षित रखा। प्रभाचंद ने धारावाहिक ज्ञान को अप्रामाणिक बताने के लिए 'अपूर्व' शब्द का संयोजन किया। ___ प्रमाण के लक्षण में जैनाचार्य बौद्धाचार्यों से उपकृत हुए हैं। अगृहीतग्राहि-'अपूर्वार्थक विशेषण भी बौद्धों की ही देन है। विद्यानन्द ने 'अविसंवाद' के खण्डन करने का प्रयत्न अवश्य किया पर उन्होंने जहाँ कहीं उसे स्वीकार भी किया । वस्तुतः स्वार्थव्यवसाय और अविसंवादि शब्दों में कोई विशेष अन्तर नहीं था। प्रमाण को स्वपरावभासक होना आवश्यक है। जैन-बौद्ध, दोनों ज्ञान को प्रमाण मानते हैं पर बौद्ध निर्विकल्पक ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं और यही दोनों के बीच विवाद का विषय रहा है । सविकल्पक को यदि अप्रमाण माना जाय तो अनधिगत अर्थ का ग्राहक न होने से तो अकलंक की दृष्टि में अनुमान भी प्रमाण कोटि से बाहर हो जायगा । बौद्धों ने इसके उत्तर में कहा कि इस स्थिति में तो पूर्व निश्चित अर्थ की स्मृति भी प्रमाण के क्षेत्र में आ जायगी । अकलंक ने इसका उत्तर देते हुए यह स्पष्ट किया कि यदि स्मृति भी विशिष्ट ज्ञान कराती है तो वह भी प्रमाण है । इतने विवाद के वावजूद दोनों दार्शनिक स्वप्रत्यक्षवादी हैं और आत्मा-ज्ञान में अभेदवादी हैं। जैन दर्शन कारक व्यवहार को कल्पित मानते हैं। वह प्रमाण कोटि से बाहर है। एक ही वस्तु को हम विवक्षा के भेद से कर्ता-कर्म-करण आदि निश्चित करते हैं । इस विवक्षा में जैन दार्शनिक अनेकान्तात्मकता को आधार मानकर तत् तत् व्यवहार को कारण मानते हैं जबकि बौद्ध दार्शनिक विवक्षा के मूल में वासना को स्वीकार करते हैं।' ज्ञान और सुख में क्या भेद है यह भी विवाद का विषय रहा है। धर्मकीर्ति के अनुसार ज्ञान और सुख में कोई भेद नहीं क्योंकि विज्ञान और सुख की उत्पत्ति के कारण समान हैं। जैन दार्शनिक इस तथ्य को द्रव्यार्थिक दृष्टि से तो स्वीकार कर लेते हैं पर पर्यायदृष्टि से वे यह कहते हैं कि ज्ञान और सुख एक ही आत्मा की भिन्न-भिन्न पर्याय हैं । अतः उन्हें एकान्तिक रूप से भिन्न या अभिन्न नहीं कह सकते । वे कथञ्चित् भिन्न हैं और कथञ्चित् अभिन्न हैं । जैन-बौद्ध, दोनों दर्शन सुखादि को चैतन्यरूप और स्वसंविदित मानते हैं इसमें कोई विवाद नहीं। जैन-बौद्ध दोनों ने सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं माना ।३ सन्निकर्ष के प्रकारों में समवाय विशेष १. प्रमाणवार्तिक, २,३१९; न्यायावतारवातिकवृत्ति, पृ० १७ । २. न्यायावतार वार्तिकवृत्ति, पृ० २०; प्रमाणवार्तिक २.२६८ । ३. न्यामकुमुदचन्द्र, पृ० २९; प्रमाणवार्तिक, २.३१६, विशेष देखिये लेखक को पुस्तक "जैन दर्शन और संस्कृति का इतिहास, पृ० १९०। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19