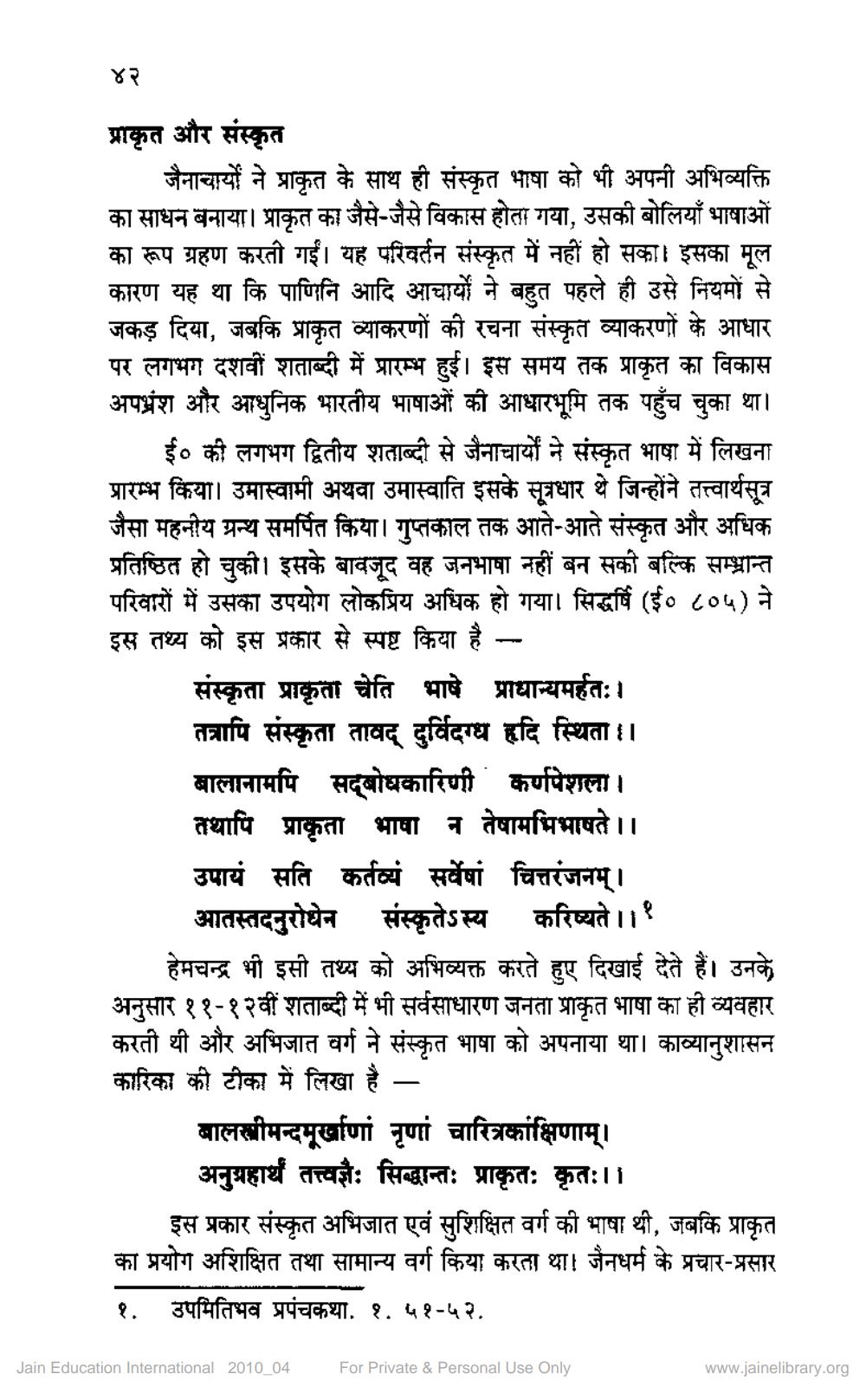Book Title: Sahityik Avdan Author(s): Bhagchandra Jain Publisher: Z_Bharatiya_Sanskruti_me_Jain_Dharma_ka_Aavdan_002591.pdf View full book textPage 8
________________ ४२ प्राकृत और संस्कृत जैनाचार्यों ने प्राकृत के साथ ही संस्कृत भाषा को भी अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनाया। प्राकृत का जैसे-जैसे विकास होता गया, उसकी बोलियाँ भाषाओं का रूप ग्रहण करती गईं। यह परिवर्तन संस्कृत में नहीं हो सका। इसका मूल कारण यह था कि पाणिनि आदि आचार्यों ने बहुत पहले ही उसे नियमों से जकड़ दिया, जबकि प्राकृत व्याकरणों की रचना संस्कृत व्याकरणों के आधार पर लगभग दशवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुई। इस समय तक प्राकृत का विकास अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं की आधारभूमि तक पहुंच चुका था। ई० की लगभग द्वितीय शताब्दी से जैनाचार्यों ने संस्कृत भाषा में लिखना प्रारम्भ किया। उमास्वामी अथवा उमास्वाति इसके सूत्रधार थे जिन्होंने तत्त्वार्थसूत्र जैसा महनीय ग्रन्थ समर्पित किया। गुप्तकाल तक आते-आते संस्कृत और अधिक प्रतिष्ठित हो चुकी। इसके बावजूद वह जनभाषा नहीं बन सकी बल्कि सम्भ्रान्त परिवारों में उसका उपयोग लोकप्रिय अधिक हो गया। सिद्धर्षि (ई० ८०५) ने इस तथ्य को इस प्रकार से स्पष्ट किया है - संस्कृता प्राकृता चेति भाषे प्राधान्यमर्हतः। तत्रापि संस्कृता तावद् दुर्विदग्ध हृदि स्थिता ।। बालानामपि सद्बोधकारिणी कर्णपेशला। तथापि प्राकृता भाषा न तेषामभिभाषते ।। उपायं सति कर्तव्यं सर्वेषां चित्तरंजनम्। आतस्तदनुरोधेन संस्कृतेऽस्य करिष्यते ।।१ हेमचन्द्र भी इसी तथ्य को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। उनके अनुसार ११-१२वीं शताब्दी में भी सर्वसाधारण जनता प्राकृत भाषा का ही व्यवहार करती थी और अभिजात वर्ग ने संस्कृत भाषा को अपनाया था। काव्यानुशासन कारिका की टीका में लिखा है - बालखीमन्दमूर्खाणां नृणां चारित्रकांक्षिणाम्। अनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञैः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः।। इस प्रकार संस्कृत अभिजात एवं सुशिक्षित वर्ग की भाषा थी, जबकि प्राकृत का प्रयोग अशिक्षित तथा सामान्य वर्ग किया करता था। जैनधर्म के प्रचार-प्रसार १. उपमितिभव प्रपंचकथा. १. ५१-५२. ____ Jain Education International 2010_04 For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57