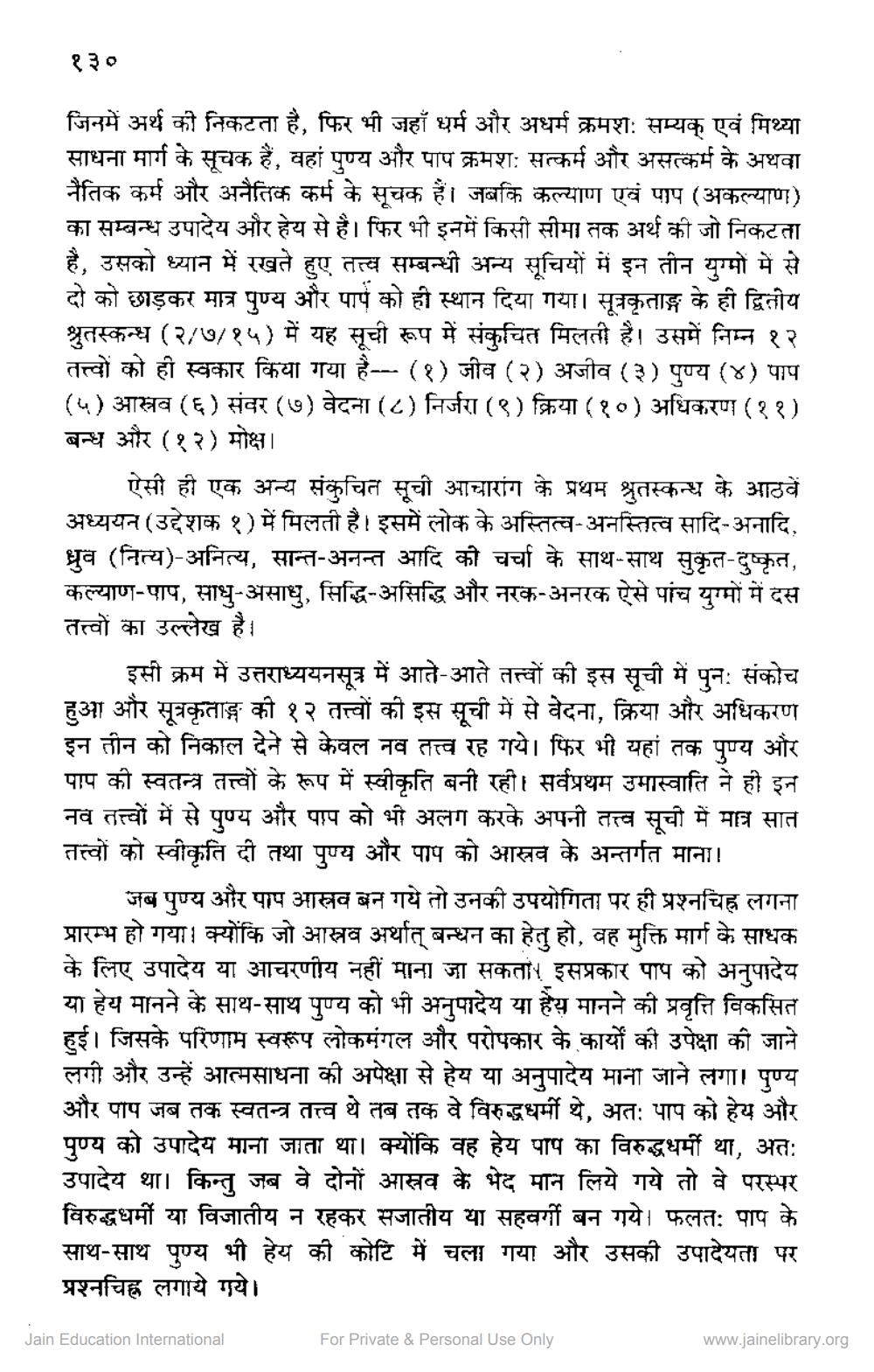Book Title: Punya ki Upadeytaka Prashna Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Sagar_Jain_Vidya_Bharti_Part_4_001687.pdf View full book textPage 4
________________ १३० जिनमें अर्थ की निकटता है, फिर भी जहाँ धर्म और अधर्म क्रमश: सम्यक एवं मिथ्या साधना मार्ग के सूचक हैं, वहां पुण्य और पाप क्रमश: सत्कर्म और असत्कर्म के अथवा नैतिक कर्म और अनैतिक कर्म के सूचक हैं। जबकि कल्याण एवं पाप (अकल्याण) का सम्बन्ध उपादेय और हेय से है। फिर भी इनमें किसी सीमा तक अर्थ की जो निकटता है, उसको ध्यान में रखते हुए तत्त्व सम्बन्धी अन्य सूचियों में इन तीन युग्मों में से दो को छाड़कर मात्र पुण्य और पापं को ही स्थान दिया गया। सूत्रकृताङ्ग के ही द्वितीय श्रुतस्कन्ध (२/७/१५) में यह सूची रूप में संकुचित मिलती है। उसमें निम्न १२ तत्त्वों को ही स्वकार किया गया है--- (१) जीव (२) अजीव (३) पुण्य (४) पाप (५) आस्रव (६) संदर (७) वेदना (८) निर्जरा (९) क्रिया (१०) अधिकरण (११) बन्ध और (१२) मोक्ष। ऐसी ही एक अन्य संकुचित सूची आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के आठवें अध्ययन (उद्देशक १) में मिलती है। इसमें लोक के अस्तित्व-अनस्तित्व सादि-अनादि, ध्रुव (नित्य)-अनित्य, सान्त-अनन्त आदि की चर्चा के साथ-साथ सुकृत-दुष्कृत, कल्याण-पाप, साधु-असाधु, सिद्धि-असिद्धि और नरक-अनरक ऐसे पांच युग्मों में दस तत्त्वों का उल्लेख है। इसी क्रम में उत्तराध्ययनसूत्र में आते-आते तत्त्वों की इस सूची में पुनः संकोच हुआ और सूत्रकृताङ्ग की १२ तत्त्वों की इस सूची में से वेदना, क्रिया और अधिकरण इन तीन को निकाल देने से केवल नव तत्त्व रह गये। फिर भी यहां तक पुण्य और पाप की स्वतन्त्र तत्त्वों के रूप में स्वीकृति बनी रही। सर्वप्रथम उमास्वाति ने ही इन नव तत्त्वों में से पुण्य और पाप को भी अलग करके अपनी तत्त्व सूची में मात्र सात तत्त्वों को स्वीकृति दी तथा पुण्य और पाप को आस्रव के अन्तर्गत माना। जब पुण्य और पाप आस्रव बन गये तो उनकी उपयोगिता पर ही प्रश्नचिह्न लगना प्रारम्भ हो गया। क्योंकि जो आस्रव अर्थात् बन्धन का हेतु हो, वह मुक्ति मार्ग के साधक के लिए उपादेय या आचरणीय नहीं माना जा सकता। इसप्रकार पाप को अनुपादेय या हेय मानने के साथ-साथ पुण्य को भी अनुपादेय या हेय मानने की प्रवृत्ति विकसित हुई। जिसके परिणाम स्वरूप लोकमंगल और परोपकार के कार्यों की उपेक्षा की जाने लगी और उन्हें आत्मसाधना की अपेक्षा से हेय या अनुपादेय माना जाने लगा। पुण्य और पाप जब तक स्वतन्त्र तत्त्व थे तब तक वे विरुद्धधर्मी थे, अतः पाप को हेय और पुण्य को उपादेय माना जाता था। क्योंकि वह हेय पाप का विरुद्धधर्मी था, अत: उपादेय था। किन्तु जब वे दोनों आस्रव के भेद मान लिये गये तो वे परस्पर विरुद्धधर्मी या विजातीय न रहकर सजातीय या सहवर्गी बन गये। फलतः पाप के साथ-साथ पूण्य भी हेय की कोटि में चला गया और उसकी उपादेयता पर प्रश्नचिह्न लगाये गये। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19