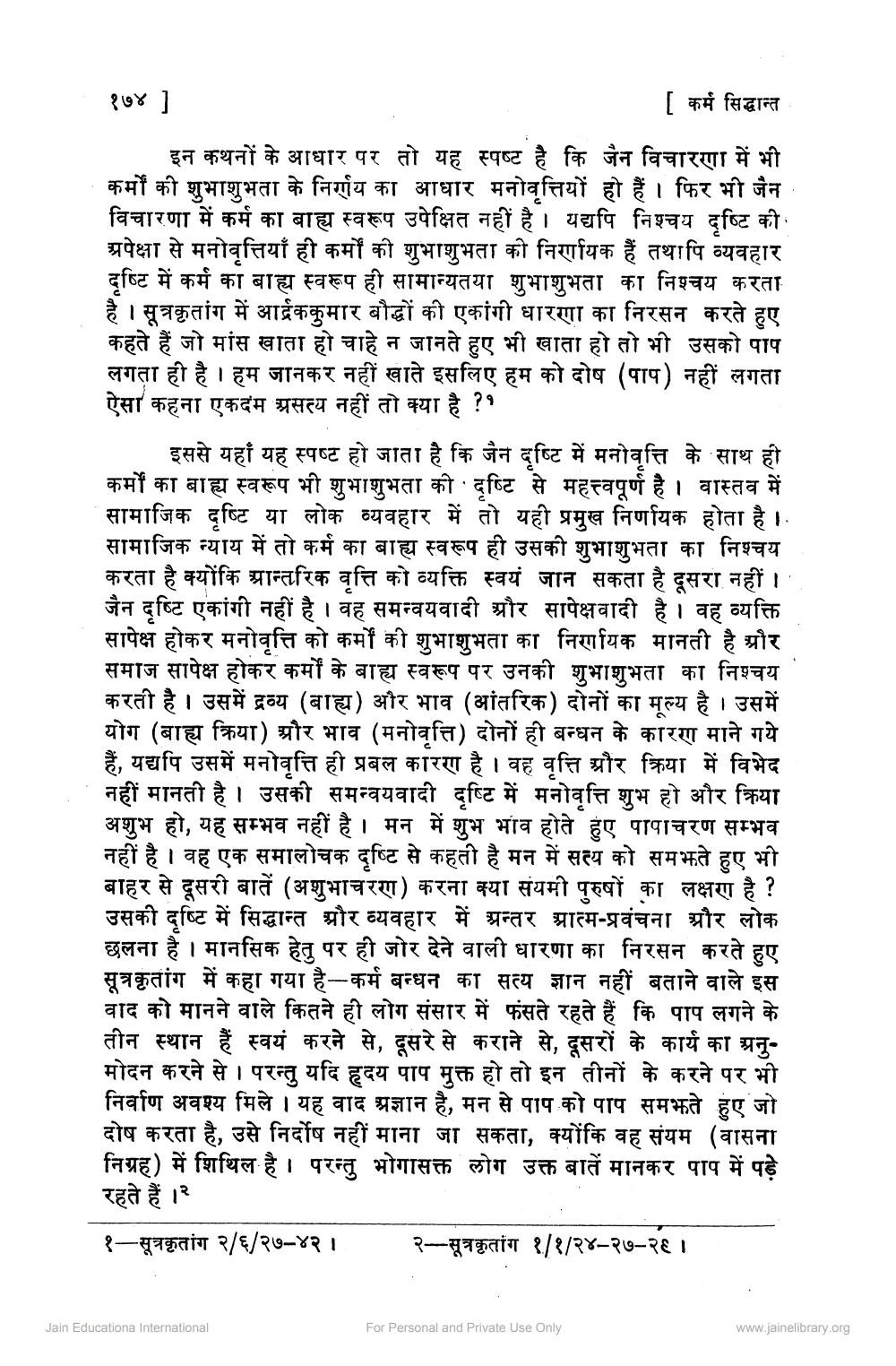Book Title: Jain Bauddh aur Gita ke Darshan me Karm ka Swarup Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Jinvani_Karmsiddhant_Visheshank_003842.pdf View full book textPage 7
________________ १७४ ] [ कर्म सिद्धान्त इन कथनों के आधार पर तो यह स्पष्ट है कि जैन विचारणा में भी कर्मों की शुभाशुभता के निर्णय का आधार मनोवृत्तियों हो हैं। फिर भी जैन विचारणा में कर्म का बाह्य स्वरूप उपेक्षित नहीं है। यद्यपि निश्चय दष्टि की अपेक्षा से मनोवृत्तियाँ ही कर्मों की शुभाशुभता को निर्णायक हैं तथापि व्यवहार दृष्टि में कर्म का बाह्य स्वरूप ही सामान्यतया शुभाशुभता का निश्चय करता है । सूत्रकृतांग में आर्द्रककुमार बौद्धों की एकांगी धारणा का निरसन करते हुए कहते हैं जो मांस खाता हो चाहे न जानते हुए भी खाता हो तो भी उसको पाप लगता ही है । हम जानकर नहीं खाते इसलिए हम को दोष (पाप) नहीं लगता ऐसा कहना एकदम असत्य नहीं तो क्या है ?' __ इससे यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन दृष्टि में मनोवृत्ति के साथ ही कर्मों का बाह्य स्वरूप भी शुभाशुभता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में सामाजिक दृष्टि या लोक व्यवहार में तो यही प्रमुख निर्णायक होता है । सामाजिक न्याय में तो कर्म का बाह्य स्वरूप ही उसकी शुभाशुभता का निश्चय करता है क्योंकि आन्तरिक वृत्ति को व्यक्ति स्वयं जान सकता है दूसरा नहीं। जैन दृष्टि एकांगी नहीं है । वह समन्वयवादी और सापेक्षवादी है। वह व्यक्ति सापेक्ष होकर मनोवृत्ति को कर्मों की शुभाशुभता का निर्णायक मानती है और समाज सापेक्ष होकर कर्मों के बाह्य स्वरूप पर उनकी शुभाशुभता का निश्चय करती है। उसमें द्रव्य (बाह्य) और भाव (आंतरिक) दोनों का मूल्य है । उसमें योग (बाह्य क्रिया) और भाव (मनोवृत्ति) दोनों ही बन्धन के कारण माने गये हैं, यद्यपि उसमें मनोवृत्ति ही प्रबल कारण है । वह वृत्ति और क्रिया में विभेद नहीं मानती है। उसकी समन्वयवादी दृष्टि में मनोवृत्ति शुभ हो और क्रिया अशुभ हो, यह सम्भव नहीं है। मन में शुभ भाव होते हुए पापाचरण सम्भव नहीं है । वह एक समालोचक दृष्टि से कहती है मन में सत्य को समझते हुए भी बाहर से दूसरी बातें (अशुभाचरण) करना क्या संयमी पुरुषों का लक्षण है ? उसकी दृष्टि में सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर आत्म-प्रवंचना और लोक छलना है । मानसिक हेतु पर ही जोर देने वाली धारणा का निरसन करते हुए सूत्रकृतांग में कहा गया है-कर्म बन्धन का सत्य ज्ञान नहीं बताने वाले इस वाद को मानने वाले कितने ही लोग संसार में फंसते रहते हैं कि पाप लगने के तीन स्थान हैं स्वयं करने से, दूसरे से कराने से, दूसरों के कार्य का अनुमोदन करने से । परन्तु यदि हृदय पाप मुक्त हो तो इन तीनों के करने पर भी निर्वाण अवश्य मिले । यह वाद अज्ञान है, मन से पाप को पाप समझते हुए जो दोष करता है, उसे निर्दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह संयम (वासना निग्रह) में शिथिल है। परन्तु भोगासक्त लोग उक्त बातें मानकर पाप में पड़े रहते हैं । १–सूत्रकृतांग २/६/२७-४२ । २-सूत्रकृतांग १/१/२४-२७-२६ । Jain Educationa International For Personal and Private Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23