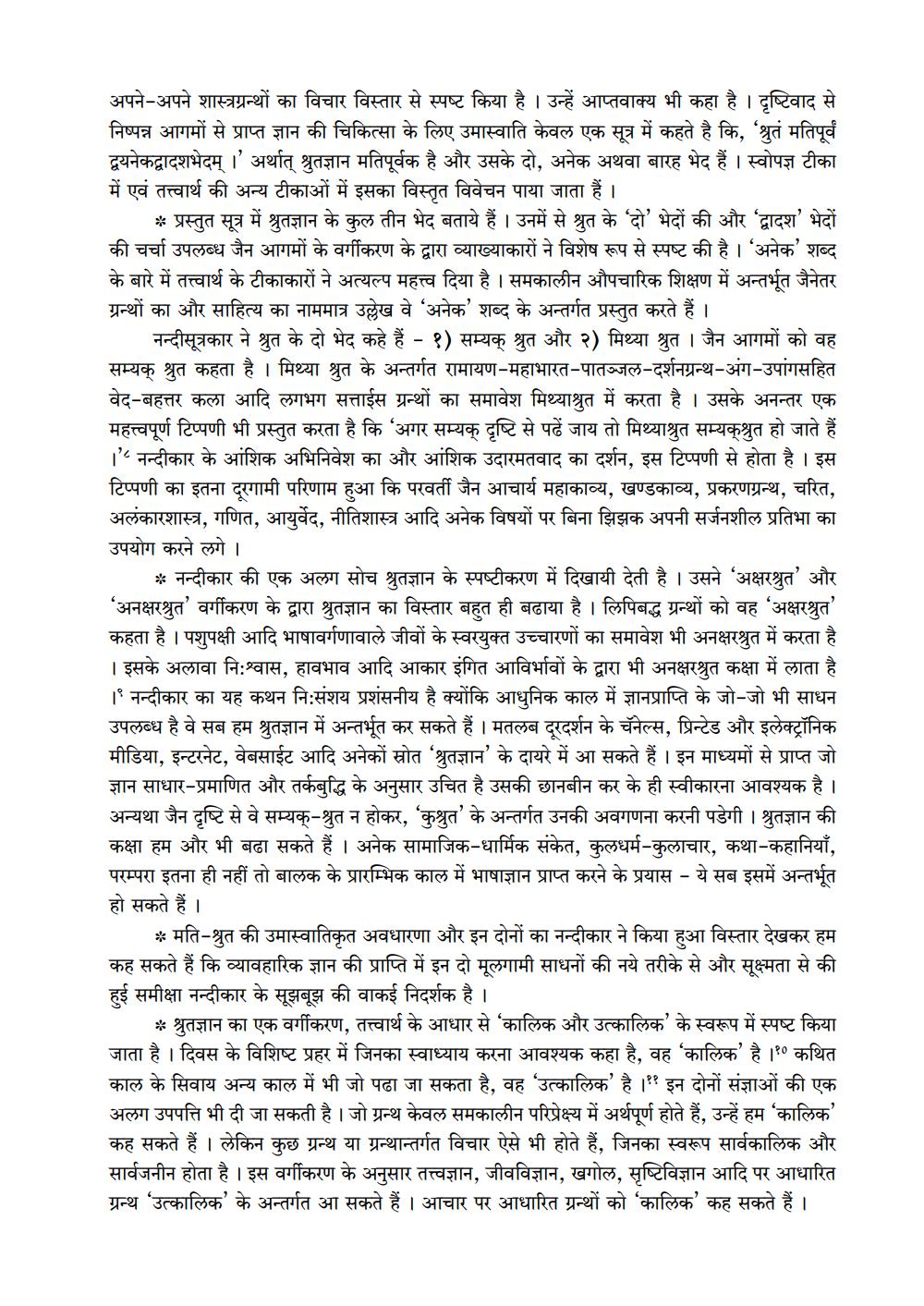Book Title: Tattvartha Sutra me Nihit Gyan Charcha Ek Nirikshan Author(s): Kaumudi Baldota Publisher: Kaumudi Baldota View full book textPage 5
________________ अपने-अपने शास्त्रग्रन्थों का विचार विस्तार से स्पष्ट किया है । उन्हें आप्तवाक्य भी कहा है । दृष्टिवाद से निष्पन्न आगमों से प्राप्त ज्ञान की चिकित्सा के लिए उमास्वाति केवल एक सूत्र में कहते है कि, 'श्रुतं मतिपूर्व द्वयनेकद्वादशभेदम् ।' अर्थात् श्रुतज्ञान मतिपूर्वक है और उसके दो, अनेक अथवा बारह भेद हैं । स्वोपज्ञ टीका में एवं तत्त्वार्थ की अन्य टीकाओं में इसका विस्तृत विवेचन पाया जाता हैं। * प्रस्तुत सूत्र में श्रुतज्ञान के कुल तीन भेद बताये हैं । उनमें से श्रुत के 'दो' भेदों की और 'द्वादश' भेदों की चर्चा उपलब्ध जैन आगमों के वर्गीकरण के द्वारा व्याख्याकारों ने विशेष रूप से स्पष्ट की है । 'अनेक' शब्द के बारे में तत्त्वार्थ के टीकाकारों ने अत्यल्प महत्त्व दिया है । समकालीन औपचारिक शिक्षण में अन्तर्भूत जैनेतर ग्रन्थों का और साहित्य का नाममात्र उल्लेख वे ‘अनेक' शब्द के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हैं। नन्दीसूत्रकार ने श्रुत के दो भेद कहे हैं - १) सम्यक् श्रुत और २) मिथ्या श्रुत । जैन आगमों को वह सम्यक् श्रुत कहता है । मिथ्या श्रुत के अन्तर्गत रामायण-महाभारत-पातञ्जल-दर्शनग्रन्थ-अंग-उपांगसहित वेद-बहत्तर कला आदि लगभग सत्ताईस ग्रन्थों का समावेश मिथ्याश्रुत में करता है । उसके अनन्तर एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी भी प्रस्तुत करता है कि अगर सम्यक् दृष्टि से पढ़ें जाय तो मिथ्याश्रुत सम्यक्श्रुत हो जाते हैं ।' नन्दीकार के आंशिक अभिनिवेश का और आंशिक उदारमतवाद का दर्शन, इस टिप्पणी से होता है । इस टिप्पणी का इतना दूरगामी परिणाम हुआ कि परवर्ती जैन आचार्य महाकाव्य, खण्डकाव्य, प्रकरणग्रन्थ, चरित, अलंकारशास्त्र, गणित, आयुर्वेद, नीतिशास्त्र आदि अनेक विषयों पर बिना झिझक अपनी सर्जनशील प्रतिभा का उपयोग करने लगे। * नन्दीकार की एक अलग सोच श्रुतज्ञान के स्पष्टीकरण में दिखायी देती है । उसने ‘अक्षरश्रुत' और 'अनक्षरश्रुत' वर्गीकरण के द्वारा श्रुतज्ञान का विस्तार बहुत ही बढाया है । लिपिबद्ध ग्रन्थों को वह 'अक्षरश्रुत' कहता है । पशुपक्षी आदि भाषावर्गणावाले जीवों के स्वरयुक्त उच्चारणों का समावेश भी अनक्षरश्रुत में करता है । इसके अलावा नि:श्वास, हावभाव आदि आकार इंगित आविर्भावों के द्वारा भी अनक्षरश्रुत कक्षा में लाता है । नन्दीकार का यह कथन नि:संशय प्रशंसनीय है क्योंकि आधुनिक काल में ज्ञानप्राप्ति के जो-जो भी साधन उपलब्ध है वे सब हम श्रुतज्ञान में अन्तर्भूत कर सकते हैं । मतलब दूरदर्शन के चॅनेल्स, प्रिन्टेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन्टरनेट, वेबसाईट आदि अनेकों स्रोत 'श्रुतज्ञान' के दायरे में आ सकते हैं । इन माध्यमों से प्राप्त जो ज्ञान साधार-प्रमाणित और तर्कबुद्धि के अनुसार उचित है उसकी छानबीन कर के ही स्वीकारना आवश्यक है । अन्यथा जैन दृष्टि से वे सम्यक्-श्रुत न होकर, 'कुश्रुत' के अन्तर्गत उनकी अवगणना करनी पडेगी । श्रुतज्ञान की कक्षा हम और भी बढा सकते हैं । अनेक सामाजिक-धार्मिक संकेत, कुलधर्म-कुलाचार, कथा-कहानियाँ, परम्परा इतना ही नहीं तो बालक के प्रारम्भिक काल में भाषाज्ञान प्राप्त करने के प्रयास - ये सब इसमें अन्तर्भूत हो सकते हैं। ___* मति-श्रुत की उमास्वातिकृत अवधारणा और इन दोनों का नन्दीकार ने किया हुआ विस्तार देखकर हम कह सकते हैं कि व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति में इन दो मूलगामी साधनों की नये तरीके से और सूक्ष्मता से की हुई समीक्षा नन्दीकार के सूझबूझ की वाकई निदर्शक है। * श्रुतज्ञान का एक वर्गीकरण, तत्त्वार्थ के आधार से 'कालिक और उत्कालिक' के स्वरूप में स्पष्ट किया जाता है । दिवस के विशिष्ट प्रहर में जिनका स्वाध्याय करना आवश्यक कहा है, वह कालिक है ।१० कथित काल के सिवाय अन्य काल में भी जो पढा जा सकता है, वह 'उत्कालिक' है ।११ इन दोनों संज्ञाओं की एक अलग उपपत्ति भी दी जा सकती है। जो ग्रन्थ केवल समकालीन परिप्रेक्ष्य में अर्थपूर्ण होते हैं, उन्हें हम 'कालिक' कह सकते हैं । लेकिन कुछ ग्रन्थ या ग्रन्थान्तर्गत विचार ऐसे भी होते हैं, जिनका स्वरूप सार्वकालिक और सार्वजनीन होता है। इस वर्गीकरण के अनुसार तत्त्वज्ञान, जीवविज्ञान, खगोल, सृष्टिविज्ञान आदि पर आधारित ग्रन्थ 'उत्कालिक' के अन्तर्गत आ सकते हैं। आचार पर आधारित ग्रन्थों को 'कालिक' कह सकते हैं।Page Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14